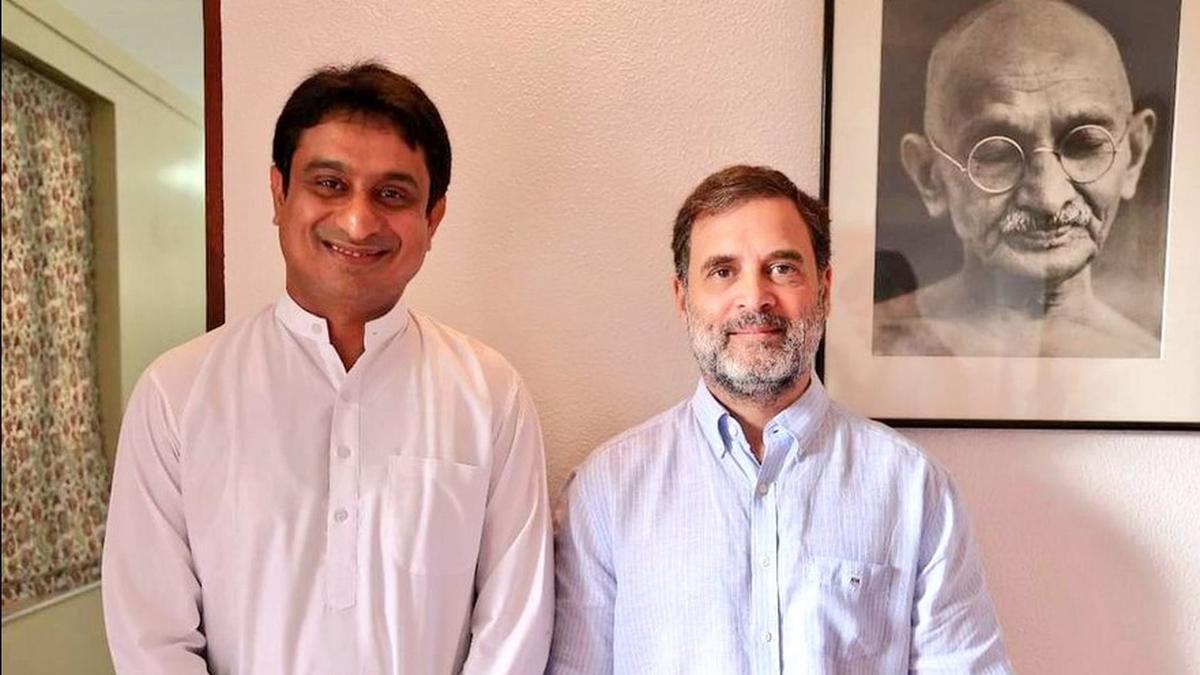नेपाल की क्रांति ने बता दिया है कि युवाओं की अनसुनी, सत्ता पर भारी पड़ सकती है, संवादहीनता की खाई कम करना ही उपाय
नेपाल में हुए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों ने न सिर्फ राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि संचार के क्षेत्र में भी नई बहस शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए संगठित किए गए, जो साबित करता है कि आज का युवा पुराने तौर-तरीके छोड़कर डिजिटल मंचों का सहारा ले रहा है। मैंने इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। मेरा मानना है कि यह सिर्फ संचार की नाकामी नहीं, बल्कि बड़ा पीढ़ीगत बदलाव है। नेताओं और युवाओं के बीच संचार की खाई गहरी हो गई है।
नेता, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो सत्ता के केंद्र में थे, पूरी तरह समाचार चैनलों, अखबारों, फेसबुक और एक्स पर निर्भर थे। वे युवाओं के असंतोष को भांप नहीं पाए, क्योंकि वे डिस्कॉर्ड जैसे मंचों से अनजान थे। डिस्कॉर्ड, युवाओं में कम से कम दो साल से लोकप्रिय था। जिस पर क्रांतिकारी युवा नए प्रधानमंत्री का चयन कर रहे थे और राष्ट्रपति के साथ बातचीत के लिए मुद्दे तय कर रहे थे। वहीं सत्ताधारी वर्ग इससे बेखबर था।
संचार का मतलब दो पक्षों के बीच सूचना का आदान-प्रदान है, लेकिन जब संचार के माध्यम अलग हों, तो रुकावटें आती हैं। नेता युवाओं को अपना श्रोता ही नहीं मानते थे। देश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के विदेश पलायन से जूझ रहा था, लेकिन नेता सत्ता के खेल में उलझे थे। नतीजा? युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और डिजिटल मंचों ने इसे आवाज दी।
पुराने संचार माध्यमों में समाचार चैनल और अखबार एकतरफा थे, वहां जवाब देने का मौका कम था। नेपाल के ज्यादातर लोग पहली बार सोशल मीडिया पर एकजुट हुए, तो यह नई संचार क्रांति का प्रतीक था। सोशल मीडिया ने सूचनाओं को तुरंत और सभी के लिए सुलभ बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, एक पोस्ट, एक वीडियो या एक मजेदार मीम से हजारों लोग जुड़ सकते हैं। यह लोकतंत्र का नया रूप है, क्योंकि यह समय, मेहनत और संसाधन बचाता है।
नेपाल में, युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से को व्यक्त किया, जहां छह महीने पहले से ही 200 से ज्यादा समूह बने थे। ये समूह भ्रष्टाचार और सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ थे। जब प्रधानमंत्री ने इन मंचों पर रोक लगाने की कोशिश की, तो यह आग में घी डालने जैसा हुआ।
पुराने विरोध, जैसे जनआंदोलन या मधेस आंदोलन में संचार धीमा था। तब समाचार चैनलों या मुंह-जुबानी प्रचार पर निर्भरता थी, जिसमें हफ्तों लग जाते थे। इस बार, 24 घंटे में ही विरोध चरम पर पहुंच गया क्योंकि सोशल मीडिया ने तुरंत सूचनाएं दीं। सरकार ने युवाओं पर जुल्म किए, तो खबर फौरन फैली और प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई। काठमांडू से लेकर छोटे कस्बों तक गुस्सा फैल गया। एक नया दृष्टिकोण जोड़ते हुए कहूं तो, विरोध अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ‘रील्स क्रांति’ बन गया है। सोचिए, जहां पहले दीवारों पर नारे लिखे जाते थे, वहां अब हैशटैग और मीम ने जगह ले ली है।
एक मीम, जो भ्रष्ट नेताओं का मजाक उड़ाता है, वायरल होकर लाखों को जोड़ देता है। यह बदलाव ताकतवर है। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विद्रोह है। युवा अपनी भाषा और शैली में बदलाव ला रहे हैं। रील्स में नारे और हैशटैग में मुद्दे, यह नई पीढ़ी की रचनात्मकता है। डिजिटल सहायता के बिना छोटे कस्बों तक पहुंचना नामुमकिन था।
जेन जेड पर पुरानी पीढ़ी का इल्जाम है कि वे रील्स देखने और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में डूबे रहते हैं और राजनीति से दूर हैं। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और भारत के उदाहरण इसके उलट हैं। युवा राजनैतिक बातचीत में सक्रिय हैं, लेकिन अपने तरीके से। वे पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि अपनी बात और अपने मंचों से जुड़ते हैं।
वैश्विक नजरिए से देखें तो भारत का किसान आंदोलन, ब्लैक लाइव्स मैटर या ब्रिटेन में हाल का आप्रवासन विरोध, सभी में तकनीक-प्रेमी युवा डिजिटल मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये युवा शोध में कुशल और अपनी बात कहने में माहिर हैं। इससे दक्षिण एशियाई सरकारें क्या सीखेंगी? अगर वे चाहें, तो सीख सकती हैं। राजनैतिक संचार में कुछ रुझान हैं, कारणों का विश्लेषण कर तैयारी की जा सकती है। लेकिन सीखने का मतलब सख्त नियंत्रण नहीं, बल्कि लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का मौका देना है। अगर गुस्से को दबाया गया, तो हिंसा बढ़ेगी। सरकारों को नई पीढ़ी की उम्मीदों का जवाब देना होगा। ये उम्मीदें पुरानी नहीं, बल्कि डिजिटल युग की हैं। पुराने ढर्रे की बातों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर नेता युवाओं को अपना श्रोता मानें और उनके मंचों पर उतरें, तो संचार की नाकामी टाली जा सकती है। वरना, यह पीढ़ीगत बदलाव और तेज होगा।

(लेखक काठमांडू यूनिवर्सिटी में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं। विचार निजी हैं।)