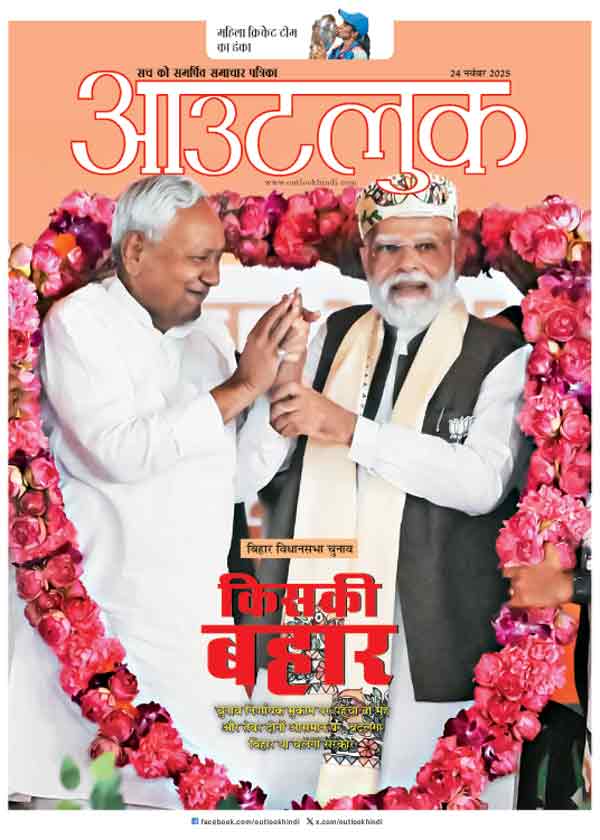यह सिर्फ दिल बहलाने का ख्याल कतई नहीं है। जरा सोचिए, अगर जाति न होती तो देश में चुनाव कैसे होते? विकास के मुद्दे सर्वोपरि होते, उम्मीदवारों का चयन काबिलियत के आधार पर होता और मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने में सहूलियत होती। लेकिन पिछले सात दशकों से देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जाति रूढ़ियों से जकड़े हिंदी पट्टी के प्रदेशों में, जिस आधार पर चुनाव लड़े गए हैं, ऐसी स्थिति तो किसी यूटोपिया जैसे आदर्श लोक में ही संभव दिखती है। यहां चुनावों में हमेशा से जाति मुख्य मुद्दा रहा है। भले ही हर पार्टी समाज के हित में जातिगत बेड़ियां तोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराती रही है, लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, वे अपने समर्थन में जातियों या समुदायों को गोलबंद करने में जुट जाती हैं। जाहिर है, उन्हें चुनाव जीतने की यही सबसे अच्छी और कारगर रणनीति लगती है।
यह अकारण नहीं है। समाज में जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया से उसे अलग कर नहीं देखा जा सकता है। देश के कई हिस्सों में जातिवाद के मुखर प्रणेता आज भी ‘बेटी और वोट स्वजातीय को ही’ जैसे नारे ईजाद कर लेते हैं। लेकिन क्या हर जाति के मतदाता अभी भी किसी खास दल या उम्मीदवार को ही अपना एकमुश्त वोट देते हैं? क्या दूसरे उम्मीदवार की सारी योग्यताएं सिर्फ इस वजह से निरर्थक हो जाती हैं कि वह किसी अन्य जाति का है? यह कटु सत्य है कि अधिकतर राजनीतिक दल कम से कम ऐसा ही समझते हैं। इसलिए जहां किसी खास जाति के लोगों की बहुतायत होती है, वहां उसी जाति के उम्मीदवार को चुनावों में उतारा जाता है, भले ही किसी दूसरी जाति का उम्मीदवार ज्यादा प्रतिभाशाली हो। दरअसल, चुनाव क्षेत्रों को मतदाताओं की जाति की बहुलता के आधार पर चिन्हित किया जाता है और उसी के आधार पर उम्मीदवारों के टिकट के फैसले किए जाते हैं। मसलन, अगर बिहार के मधेपुरा में यादवों की, बक्सर में ब्राह्मणों की और पटना में कायस्थ मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो अधिकतर पार्टियां इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। देश भर में ऐसे कई चुनाव क्षेत्र हैं जहां एक ही जाति के उम्मीदवार दशकों से स्वजातीय मतदाताओं की संख्या बल पर जीतते आए हैं।
आज भले ही कई पार्टियां जाति जनगणना कराने की मांग उठा रही हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर के पास हर चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के जातिगत आंकड़े बूथ स्तर तक उपलब्ध हैं। जिनके पास नहीं हैं, वे सामाजिक आर्थिक-संगठनों की रिपोर्ट या चुनावी रणनीतिकारों की मदद से लेती हैं। विडंबना यह है कि इसमें वे पार्टियां भी शामिल हैं जो समावेशी विकास की लकीर को समाज के अंतिम आदमी तक खींचने की बात करती रही हैं। यही बात उन क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जहां किसी समुदाय विशेष के वोटरों का बोलबाला है। इसी कारण जाति या वर्ग विशेष के मतदाताओं को रिझाने के लिए गोलबंदी या ध्रुवीकरण करने के तमाम हथकंडे चुनाव के दौरान अपनाए जाते हैं। चुनाव-दर-चुनाव ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है मानो विकास के सारे मुद्दे ऐसे हथकंडों के सामने पंगु हो गए हैं।
क्या पांच राज्यों में अभी हो रहे विधानसभा चुनावों में कुछ अलग होगा या फिर वही जातिगीरी की पुरानी, कर्कश राग अलापी जाएगी? क्या इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाता योगी आदित्यनाथ सरकार का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कामकाज के आधार पर करेंगे या किसी दूसरी कसौटी पर? क्या अखिलेश और मायावती की पार्टियां जातिवाद के पैमाने से इतर उत्तर प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के वादों के आधार पर चुनी जाएंगी? क्या सर्वांगीण विकास, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, नारी सुरक्षा व कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे की इन चुनावों में कोई भूमिका होगी या ये चुनाव भी जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाएंगे?
हर चुनाव की तरह इस बार भी वही पुराने सवाल सामने हैं, जिन्हें लेकर हम इस अंक की आवरण कथा के साथ हाजिर हैं। नई सदी के दो दशक बीतने के बाद ऐसे सवाल बेमानी हो जाने चाहिए थे। आज जब देश के अधिकांश मतदाता मिलेनियल पीढ़ी के युवा हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे किसी भी चुनावी समर में अप्रासंगिक हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा ही हो रहा है।
इसमें शक नहीं कि आज के अधिकतर युवा सामाजिक-आर्थिक जैसे कई क्षेत्रों की परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे निकल चुके हैं। इसलिए उनसे उम्मीद करना वाजिब है कि चुनाव के माध्यम से वे जनप्रतिनिधियों को चुनने में भी योग्यता को तरजीह देंगे, न कि उनकी जाति या कौम को। यह भी कि वे लोकतंत्र की बेहतरी के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार का ही चयन करेंगे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। नए भारत की नई पीढ़ी के मतदाताओं से ऐसी उम्मीद रखना न ही यूटोपिया बनाने जैसा दिवास्वप्न देखना है, न चांद तोड़कर जमीन पर लाने की ख्वाहिश रखना। अभी हो रहे चुनावों में ये सपने साकार हो न हों, इन्हें हकीकत में आज नहीं तो कल बदलना ही होगा।