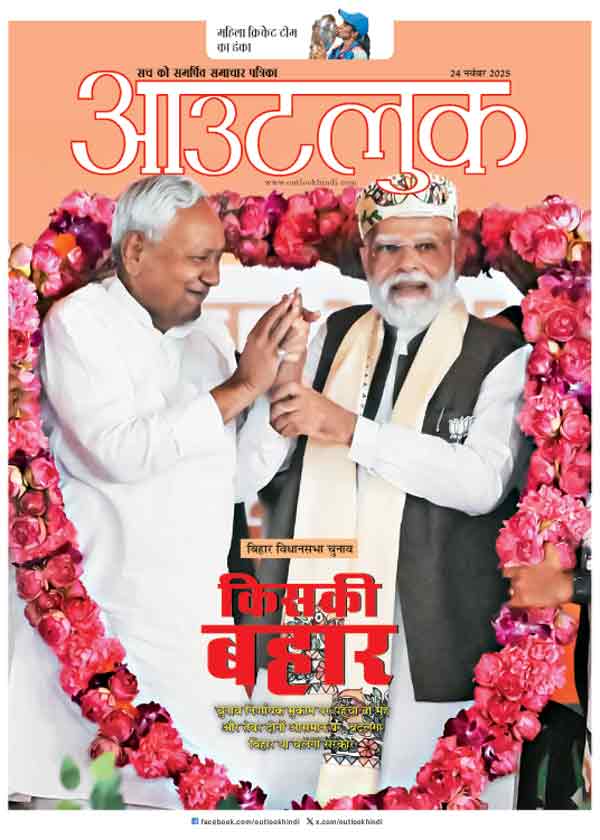बड़े नेताओं को छोड़कर सब नए विधायक संसदीय सचिव ही बनाए जाते थे। मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता था कि वह नेता सदन की हैसियत से अपनी पार्टी से किसे संसदीय सचिव बनाने की संस्तुति राज्यपाल को करे। यह समझा जाता था नए लोगों के लिए कार्यपालिका में प्रवेश करने का द्वार यही पद है। दूसरे प्रदेशों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो संभवतः यह पद वहां भी पहली सीढ़ी की तरह था। संसदीय सचिव हो कर आगे बढ़ा जा सकता था। वह राजनीति में नए विधायक के लिए इंटर्नशिप थी। उस काल के राजनीतिज्ञ जो इस प्रक्रिया से गुजर कर आए उनमें से अधिकतर सफल राजनीतिज्ञ हुए। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं, लालबहादुर शास्त्री को भी इंटर्नशिप से गुजरना पड़ा था।
यह प्रक्रिया क्यों समाप्त हुई? यह सवाल वाजिब है। दरअसल पार्टी में गुटबंदी बढ़ने के साथ मंत्रीपद महत्त्वपूर्ण होता गया। जातिगत विभाजन भी इसका मुख्य कारण हो गया। हर गुट पहले अपने गुट के लिए मंत्री पद मांग लेता है। सब यही समझते थे कि चुनाव जीतकर सदन में पहुंचना मंत्री बनने का प्रमाण पत्र है। अब तो यह स्थिति है कि अगर किसी विधायक के साथ चार विधायक हैं तो उसकी मांग मंत्री पद की होती है। यह प्रशिक्षण की परंपरा अब लगभग समाप्त हो गई है। नतीजा यह हुआ कि अब मंत्रियों में न बोलने का प्रशिक्षण है और न लिखने की क्षमता। सदन में प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से देना कठिन होता है। संसदीय सचिव मंत्रियों के साथ संबद्ध होते थे, मंत्री के सदन संबंधी पत्र व्यवहार अधिकतर संसदीय सचिव ही देखते थे। मंत्री को ब्रीफिंग भी करते थे। उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे नीतिगत वक्तव्य दें। आज मंत्री भी यह नहीं समझ पाते कि कौन सी बात कही जानी चाहिए कौन सी नहीं। कांग्रेस के जमाने में मंत्रियों में वाचा का अनुशासन बहुत था। अब तो मंत्री ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जो पार्टी और सत्तासीन सरकार की नीति से मेल नहीं खाते।
फिर थ्री टायर मंत्रिमंडल बनने लगे । उसमें संसदीय सचिव होता था, फिर उप मंत्री और फिर मंत्री। फिर उप मंत्री , राज्य मंत्री और मंत्री होने लगे। अब राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्यमंत्री और मंत्री। उनको सब सुविधाएं मिलने लगीं। प्रशिक्षण तत्व लगभग समाप्त हो गया। अब संसद सचिव जहां होते हैं उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है कुछ सदस्यों को सरकार में जगह देना। हालांकि यह भी सुनने में आता है कि कई मंत्री अपने राज्य मंत्री को भी काम नहीं देते। लालबत्ती उन्हें संतुष्ट रखती है। उत्तर प्रदेश में उपमंत्रियों तक को वाहन नहीं मिलता था। केवल सरकार व्यक्तिगत कार खरीदने के कर्ज देती थी। सरकारी काम के लिए पूल से वाहन मंगाना पड़ता था। आज संसद सचिव का मुद्दा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक कारण अधिक हैं। 18 जून के द हिंदू में लिखा था कांग्रेस और भाजपा अपने संसदीय सचिव को मासिक भत्ता देती थी।
क्यों यह इतना गंभीर मुद्दा बनना चाहिए?
शायद चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में यह है कि वह अपनी सरकार को कैसे गठित करता है। लगभग साल भर से दिल्ली सरकार में 21 संसद सचिव कार्यरत थे। पता नहीं उनको उप राज्यपाल ने गोपनीयता की शपथ दिलाई थी या नहीं। बताया जाता है उन्हें सिवा विधायक के वेतन और भत्ते के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। कानूनी पेंच तब बना जब दिल्ली सरकार ने संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार के हाथ अवसर लग गया। अगर ऐसा न होता तो संभवतः यथास्थिति बनी रहती। ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से सचिवों को हटाने के लिए कहती। दरअसल मंत्रिमंडल की सीमित संख्या का अतिक्रमण एक अहम मुद्दा है। मुद्दा संभवतः संसद सचिव का नहीं, वे तो दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, बल्कि संख्या का है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के नाम से दिल्ली सरकार का बिल रिजेक्ट कर दिया था तो ज्यादा से ज्यादा सचिवों को हटाने का मामला बनता है। जनता द्वारा चुने गए 21 विधायकों को अवैध घोषित करने में कई और भी पक्ष सामने आएंगे। उनकी गलती कितनी है। क्या उन्होंने किसी ऐसी सूचना को कमीशन से छुपाया जो देना अनिवार्य था। या उन्होंने अतिरिक्त पद लाभ लिया जिसके लिए अधिकृत नहीं थे। सचिवों का कोई मिस कंडेक्ट था वगैरह वगैरह। कैबिनेट के निर्णय के तहत या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं या नहीं? यह कुछ सवाल हैं जो चुनाव आयोग के सामने होंगे। दिल्ली की विधानसभा में भाजपा के तीन विधायकों के अतिरिक्त किसी पार्टी का विधायक नहीं है। अगर 21 विधायक अवैध घोषित कर दिए गए और उन रिक्त स्थान पर दूसरी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी आदि को सीटें मिल गई तो शायद उनकी स्थिति सम्मानजनक हो जाएगी।