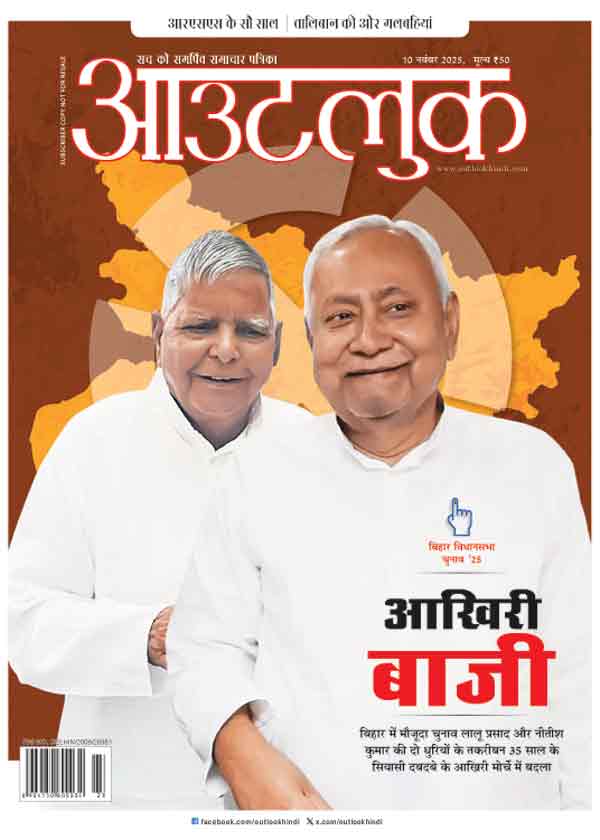यूरोप में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक चेतना का उदय और विकास एक लंबी संघर्ष-प्रक्रिया के दौरान हुआ लेकिन भारत में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र की राजनीतिक प्रणाली को ऐसे समाज पर थोप दिया गया, जो अभी तक मध्यकालीन मूल्य-व्यवस्था और सामंती चेतना से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई परिवार है और हमारे देश में वह पूरी तरह से पितृसत्तात्मक मूल्यों के आधार पर गठित और संचालित होता था। आज स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं। इस चेतना का एक बुनियादी अवयव यह है कि हर व्यक्ति अपने आपको खास यानी दूसरों से श्रेष्ठ और भिन्न समझना चाहता है। भारतीय समाज में रची-बसी जाति-व्यवस्था भी इस चेतना को मजबूत करती है क्योंकि वह जन्माधारित ऊंच-नीच के सिद्धांत पर टिकी है। ऐसे में विशेषाधिकार ही किसी की सामाजिक-राजनीतिक हैसियत का पैमाना बन जाते हैं। यह लोकतंत्र का विलोम है।
हमने पश्चिमी देशों से लोकतंत्र का ‘तंत्र’ तो ले लिया लेकिन उसे ‘लोक’ से दूर कर दिया। लोकतंत्र का बुनियादी मूल्य सभी नागरिकों की समानता है। लेकिन भारत में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। जॉर्ज ऑरवेल के शब्दों में कहें तो कुछ नागरिक दूसरों से अधिक ‘समान’ हैं क्योंकि उन्हें उनकी हैसियत के कारण विशेषाधिकार मिले हुए हैं। याद कीजिए स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। वे अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने गए थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी सामान्य नागरिक जाता है। न कोई पायलट कार, न सुरक्षा गार्ड। फिल्म देखकर बाहर निकले तो उन पर गोली चल गई और उनकी मृत्यु हो गई। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हांस-डीट्रिश गेंशर के साथ हुआ एक वाकया भी याद आ रहा है। गेंशर अपने देश के अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानित राजनीतिक नेता थे। एक बार वे कुछ खरीदारी करने गए और कार गलत जगह खड़ी कर दी। उनका तत्काल चालान हुआ, जिसकी रकम उन्होंने वहीं अदा कर दी। देश के अखबारों में उनकी कड़ी आलोचना हुई कि जो व्यक्ति कार सही जगह पार्क नहीं कर सकता, वह विदेश नीति को सही ढंग से कैसे संचालित करेगा? इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक सीरियल देखा जा सकता है जिसका शीर्षक है ‘बोरियन’। यह एक महिला राजनीतिज्ञ पर केंद्रित है जो अप्रत्याशित रूप से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन जाती है। लेकिन उसका मध्यवर्गीय जीवन नहीं बदलता, न ही उसका मकान बदलता है। पति के साथ उसके संबंधों में तनाव आने लगता है क्योंकि वह अपनी बारी आने पर बच्चों को स्कूल छोड़ने या वहां से लाने नहीं पहुंच पाती। पति को एक बहुत बढि़या नौकरी मिलती है लेकिन वह उसे नहीं करने देती क्योंकि वह प्रधानमंत्री है और उस पर अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पति को नौकरी दिलाने का आरोप लग सकता है। क्या हम अपने देश में कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी सिनेमा हॉल में सामान्य नागरिक की तरह फिल्म देखने जाएगा, और वह भी बिना किसी तामझाम के? या कोई प्रधानमंत्री उन्हीं आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए अपना पहले जैसा जीवन बिताएगा, जैसा वह पद पर आने से पहले बिताता था?
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए चुनावों के कारण विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे राजनीतिक नेता विशिष्ट और अति विशिष्ट बन जाते हैं। दूसरे भी इस वीआइपी संस्कृति की नकल करते हैं। न जाने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं जब टोल प्लाजा पर टोल मांगे जाने पर पंचायत प्रधानों या विधायकों ने हंगामा खड़ा किया, और कई बार तो गोलियां तक चल गईं। पहचान-पत्र दिखाने को कहने पर अनेक सुरक्षाकर्मी विशिष्ट व्यक्तियों से थप्पड़ खा चुके हैं।
कुछ ही दिन पहले कानपुर में एक पचास-वर्षीय महिला की अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही मृत्यु हो गई क्योंकि राष्ट्रपति वहां से गुजर रहे थे और रास्ता बंद था। अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही के समय सड़कों को घंटों-घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है और सुरक्षाकर्मी इस बात का भी लिहाज नहीं करते कि कोई रोगी गंभीर हालत में अस्पताल जा रहा है और वे एंबुलेंस को तो कम-से-कम जाने दें। वह महिला भारतीय उद्योग एसोसिएशन की कानपुर शाखा के महिला संगठन की अध्यक्ष थीं, इसलिए अब कानपुर के पुलिस आयुक्त का कार्यालय माफी मांग रहा है और राष्ट्रपति भी शोक प्रकट कर रहे हैं। कोई मामूली व्यक्ति होता तो किसी को कोई परवाह न होती। ऐसी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश के विभिन्न स्थानों में पहले भी होती रही हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह वीआइपी संस्कृति पूरे राजनीतिक वर्ग में फैल चुकी है और इससे अछूते रहने वाले इक्का-दुक्का अपवाद ही नजर आते हैं। शासक दल हो या विपक्षी दल, सभी ने विशेषाधिकार की इस संस्कृति को अपना लिया है। वह जमाना गया जब समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू से संसद में प्रधानमंत्री के खर्च का हिसाब पूछा करते थे। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए आठ हजार चार सौ करोड़ रुपये के विशेष विमान खरीदे जाते हैं और कहीं कोई चूं तक नहीं करता। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को लगातार सीमित किया जा रहा है और सत्ता-प्राप्त व्यक्तियों के अधिकारों को और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है, चाहे वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, नौकरशाह हों या पुलिसकर्मी हों। ‘लोक’ और ‘तंत्र’ यानी व्यवस्था के बीच की खाई लगातार और चौड़ी होती जा रही है। जब तक इस वीआइपी संस्कृति पर अंकुश नहीं लगेगा, लोकतंत्र केवल एक औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहेगी, जिसमें शासक और शासित के अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह अलग होंगे।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं)