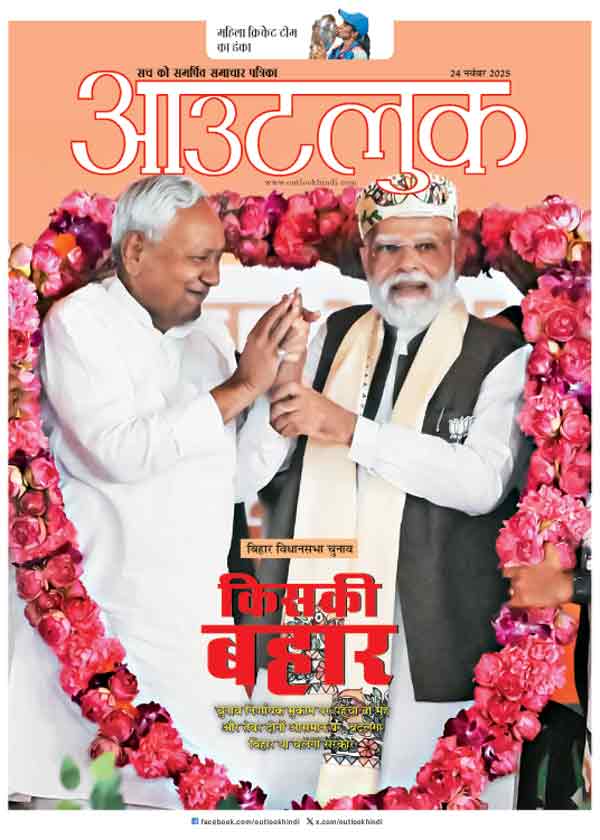एक तरफ विधानसभा चुनावों के सियासी शोर-शराबे और दूसरी तरफ महामारी की दूसरी लहर की दर्दनाक तबाही के बीच 5 अप्रैल को देश के हालिया इतिहास में मील का पत्थर समान एक घटना पूरी तरह भुला दी गई। करीब एक दशक पहले उस दिन महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि गांव के एक स्वयंभू गांधीवादी दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे।
उस वक्त मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर था। वरिष्ठ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के खिलाफ रक्षा सौदों, राष्ट्रमंडल खेल, कोयला ब्लॉक और स्पेक्ट्रम आवंटन वगैरह में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्टों से निकल रहे थे। जांच एजेंसियां खासकर सीबीआइ पर सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के आरोप लग रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी पर विपक्ष हमलावर था। उन पर यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कठपुतली की तरह काम करने के आरोप लगाए जा रहे थे। उधर, बढ़ती महंगाई और आसमान छूती बेरोजगारी ने आम लोगों में निराशा और गुस्से को बढ़ा दिया। सत्ता में बैठे लोग कथित रूप से काले धन के जरिए करोड़ों-अरबों में खेल रहे थे।
अगले दो वर्षों में जब भी रालेगण सिद्धि का वह शख्स धोती-कुर्ता और गांधी टोपी में दिल्ली में आकर अनशन पर बैठा, सरकार हिल जाती थी। उसके इर्दगिर्द कुछ एक्टिविस्ट, वकील, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, एक योग कारोबारी का घेरा था और अनशन का समाचार टीवी चैनलों पर चौबीसों घंटे लाइव प्रसारित होता था। इस तरह जंतर-मंतर पर उस बुजुर्ग और उसकी टोली ने लोकपाल के रूप में सभी संस्थाओं को बचाने और राजनीति में बदलाव लाने का रामबाण नुस्खा पेश किया। इंकलाब के नारे उठ रहे थे और उस शख्स के सिपहसालार दावा कर रहे थे कि वे तथाकथित स्वायत्त संस्थाओं को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कराएंगे।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से मंत्रमुग्ध अनेक देशवासियों के लिए यह आंदोलन कुछ खास महत्व का था। उन उथल-पुथल भरे दिनों में लोकपाल आंदोलन के हिस्सा रहे एक्टिविस्ट मयंक गांधी आउटलुक से कहते हैं, ‘‘आंदोलन ने नब्ज पर हाथ रख दिया था....हम संवैधानिक निकायों और तथाकथित स्वायत्त संस्थाओं की सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत देखते-देखते थक गए थे।’’ मयंक कहते हैं कि पब्लिक चार्टर और नेताओं, अधिकारियों तथा न्यायपालिका को लोकपाल के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रस्ताव इस विश्वास से निकला था कि ऐसी संस्था की जरूरत है जो सही मायने में स्वायत्त हो, कामकाज में स्वतंत्र हो और लोगों के प्रति, न कि सत्ताधीशों के प्रति जवाबदेह हो।’’
लोकपाल को 1 जनवरी 2014 को विधायी मंजूरी मिल गई, अलबत्ता मूल अवधारणा से काफी कम शक्तियां मिलीं। पांच महीने बाद ही यूपीए सरकार सत्ता गंवा बैठी। कांग्रेस लोकसभा में सबसे कम संख्या में पहुंच गई और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के हाथ सत्ता आ गई। जंतर-मंतर का शख्स लौट गया, उसके कई सिपहसालार उसी व्यवस्था में जा बैठे, जिसे बदलने की कौल उठा चुके थे। कुछ राजनीतिक सत्ता का प्रसाद चख रहे हैं, जिससे वे कभी नफरत-सा करते थे।
आखिर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की कई बार हिदायतों के बाद लोकपाल मूर्त रूप ले सका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी.सी. घोष देश के पहले लोकपाल बने। लेकिन सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने का लोकपाल का मूल उद्देश्य भ्रामक साबित हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लोकपाल को 2020-2021 में सिर्फ 95 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 66 प्रारंभिक जांच के विभिन्न चरणों में बंद हो गईं। 2019-2020 के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। मसलन, लोकपाल को कुल 1427 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1218 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। कार्रवाई के निर्देश केवल 34 शिकायतों में दिए गए। इसके विपरीत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआइ) में भारत की स्थिति कुछ और तस्वीर बयान करती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दो वर्षों में सीपीआइ रेटिंग में मामूली सुधार के बाद, भारत 2017 के बाद से लगातार इस सूचकांक में फिसल रहा है, फिलहाल 180 देशों में वह 86वें स्थान पर है।
लेकिन संस्थाओं की सच्ची स्वतंत्रता संबंधी लोकपाल आंदोलन का बड़ा सपना जल्दी ही भुला दिया गया। अब तो ये संस्थान पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक लाचार नजर आ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड, 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान घटाने पर काफी आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग ‘‘स्वतंत्र’’ देश से ‘‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’’ देश कर दी गई, लेकिन चिंता की और भी कई वजहें हैं।
उस रैंकिंग में भारत कई पैमाने पर कमतर आंका गया। मसलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शिक्षा प्रणाली में व्यापक राजनीतिक दखल, भ्रष्टाचार के खिलाफ संरक्षा और दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उचित प्रक्रिया को बरकरार रखने में नाकामी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक विशेष हवाला काफी परेशान करने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘अंक 3 से गिरकर 2 हो गया, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की असामान्य नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले सरकार के हक में होना, सरकार के राजनैतिक हितों के विरुद्ध फैसला सुनाने पर जज के ताबादले का हाई प्रोफाइल मामला, सभी से यही जाहिर होता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच कहीं ज्यादा ही करीबी संबंध बन गए हैं।’’
ऐसी बहस छिड़ गई है कि न्यायपालिका, खासकर उसके शिखर की प्रतिबद्धता न्याय से ज्यादा सरकार के प्रति हो गई है। इस साल की शुरुआत में आउटलुक को दिए एक साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, ‘‘यह महसूस होता है, ऐसी धारणा बनने लगी है कि अदालत सरकार के पक्ष में ज्यादा झुकी है, बनिस्बत देश के आम लोगों के।’’ जनवरी 2017 में न्यायाधीशों की चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बने प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के फैसलों ने राजनीतिक स्तर पर संदेह और बढ़ा दिया है। कोविड महामारी प्रबंधन और टीकाकरण से संबंधित मामलों में हाल के हफ्तों में न्यायपालिका के समय पर किए गए हस्तक्षेप और निर्णायक फैसले अपवाद के रूप में हैं, जिनकी सराहना भी की जा रही है।
न्यायपालिका को दोहरा झटका इस धारणा से भी लगता है कि शिखर के जजों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक पसंद-नापसंद के आधार पर हो रही है। न्यायमूर्ति गुप्ता कहते हैं, ‘‘आप हाइकोर्ट में स्वतंत्र दिमाग के न्यायाधीश हैं और सरकार के प्रति नरम नहीं हैं, तो सरकार आपको मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति में अड़ंगा डाल सकती है।’’ हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं। मसलन, त्रिपुरा हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकिल कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने का सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की पीठ स्वीकृत है मगर सात जगहें खाली पड़ी हैं।
मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार तीखे हमले करते जा रहे हैं कि, ‘‘सरकार मीडिया और न्यायपालिका सहित उन सभी संस्थाओं के ढांचे को नष्ट कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।’’ यह आलोचना कुछ हेरफेर के साथ कांग्रेस के पिछले शासन काल में समान रूप से लागू होती रही है। उस दौरान कांग्रेस सरकारें लगातर मीडिया और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश करने की दोषी बताई जाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यूपीए सरकार के दौरान सीबीआइ को ‘‘पिंजरे का तोता’’ कह दिया था। यह आरोप भी लगे कि यूपीए सरकार अपनी विचारधारा के लोगों को विभिन्न आयोगों और अकादमियों में नियुक्त कर रही है।
फिर भी संस्थाओं पर कब्जे, या कुछ लोगों की राय में संस्थाओं के पतन, के दाग मोदी सरकार पर ज्यादा गहरे चिपक रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ पूछते हैं, ‘‘क्या आप किसी संवैधानिक निकाय या स्वायत्त संस्था का नाम ले सकते हैं जो आज सरकार के ही अंग की तरह काम नहीं कर रही है?’’ एनआइए, सीबीआइ, ईडी और डीआरआइ जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साख में गिरावट के पुराने आरोप कोविड की जानलेवा दूसरी लहर की तरह लौट आए हैं। भाजपा की राजनीति और विचारधारा से अलग नजरिया रखने वालों पर फटाफट निशाने, गिरफ्तारी और नजरबंदी से आरोप सही जान पड़ने लगे हैं। भीमा कोरेगांव मामले में बुद्धिजीवियों; जेएनयू, अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया के छात्रों; सीएए के विरोध में छात्र-कार्यकर्ता; पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों और पी. चिदंबरम तथा डी.के. शिवकुमार जैसे प्रमुख नेताओं के मामले, ऐसे ढेरों सबूत हैं। इन जांच एजेंसियों में सबसे बदनाम सीबीआइ में अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच भारी उठा-पटक दिखी थी, जब कथित तौर पर राफेल जेट सौदे की जांच करने की तैयारी कर रहे उसके निदेशक आलोक वर्मा को पहले केंद्र ने छुट्टी पर भेजा, और फिर बर्खास्त कर दिया।
तत्कालीन कैग का नाम हर घर में चर्चा का विषय था, उनकी रिपोर्टों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। आज किसी को भी पता नहीं कि कैग कौन है
इस बीच कैग, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) जैसी अन्य संस्थाओं का अब पता-ठिकाना भी नहीं लगता, जो यूपीए शासन के दौरान नियमित नकारात्मक खबरों के लिए चर्चा में होती थीं। पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली कहते हैं, ‘‘लोगों के बीच यूपीए की साख गिरने का एक प्रमुख कारण कैग, सीवीसी जैसे संस्थाओं से आईं परेशान करने वाली रिपोर्टें थीं। तत्कालीन कैग (विनोद राय) का नाम हर घर में चर्चा का विषय था, उनकी रिपोर्टों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। आज किसी को भी पता नहीं है कि कैग कौन है या वह क्या कर रहा है।’’ पिछली बार जब कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक हलचल का कारण बनी तो वह विवादास्पद राफेल जेट सौदे के ऑडिट से संबंधित थी, लेकिन उसकी चर्चा खुलासे के लिए नहीं, बल्कि तथ्य छुपाने के लिए हुई। पूर्व कानून मंत्री पूछते हैं, ‘‘कीमतों में बदलाव के बाद कैग की राफेल ऑडिट रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था, क्या आपने कभी ऐसी ऑडिट रिपोर्ट देखी-सुनी है जिसमें कीमतों के बारे में कुछ न कहा गया हो?’’
जेएनयू और जामिया जैसी शीर्ष शिक्षण संस्थाओं पर भी लगाम कसने की कोशिशें जारी हैं, जिन्हें बदनाम करने के लिए भाजपा सदस्यों ने शातिर अभियान चलाया। एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र सोहेल हाशमी कहते हैं, ‘‘देश भर के कैंपस में अशांति की घटनाओं की पुनरावृत्ति, भाजपा के गुंडों द्वारा छात्रों पर हमले, छात्रों के खिलाफ राजद्रोह के मामले और विभिन्न विश्वविद्यालयों में बिना रीढ़ वाले कुलपतियों की नियुक्तियां इन आरोपों को साबित करती हैं।’’
जाहिर है, एक दशक पहले जंतर-मंतर पर एकत्र हुए लोगों की उम्मीदें बेमानी साबित हो चुकी हैं। उनके असंतोष और गुस्से से आए सात साल पहले ऐतिहासिक चुनावी नतीजे, और दो साल पहले आए उसका जोरदार दोहराव भी देश की संस्थागत सड़ांध को दूर करने में नाकाम रहे। यकीनन आज संस्थाएं कहीं बदतर हालात में हैं। बदले में देश को लोकपाल के रूप में एक और संस्था जरूर मिली, लेकिन आज कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रही है। इस बीच जंतर-मंतर पर सन्नाटा है और 10 साल पहले मंच से 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लगाने वाला शख्स भी चुप है।