फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेमा बनाने और देखने वालों के लिए दशकों से दिलचस्पी का सबब रहा है। पर पिछले कुछ वक्त से हिंदी फिल्मों का हश्र देखते हुए यह अब उत्सुकता से ज्यादा दहशत की वजह बनता जा रहा है। करोड़ों रुपये के बजट और सैकड़ों लोगों की मेहनत से बनी फिल्मों का पहला ही शो बुरी तरह पिट जाने की दहशत इस वक्त तारी है। किसने सोचा था कि चार साल बाद परदे पर एक चर्चित फिल्म के रीमेक के साथ उतरे आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा पहले ही दिन दर्शकों को तरस जाएगी और थियेटर खाली रह जाएंगे। रिलीज से जुड़ी तमाम दिक्कतें झेलने के बाद करीब दस हजार शो के साथ 11 अगस्त को परदे पर आई इस फिल्म के दूसरे ही दिन तेरह सौ शो कम कर दिए गए क्योंकि दर्शक नदारद रहे। यहां तक कि नए भारत कुमार बनने को बेताब अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी बुरी तरह लड़खड़ा गई। अनुराग कश्यप का प्रयोग और आत्मविश्वास भी उनकी फिल्म दोबारा को डूबने से नहीं बचा सका। हाल में धराशायी होने वाली इन तीनों फिल्मों के खिलाफ सोशल मीडिया पर चले बायकॉट अभियान को इस असफलता की बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि हालिया महीनों में फ्लॉप रही हिंदी फिल्मों के पीछे सिर्फ बायकॉट की ही भूमिका हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछले कुछ वक्त में सबसे ज्यादा ठोकर खाने वाले निर्माताओं में यशराज बैनर है। भरपूर प्रचार के बावजूद रणबीर कपूर के अभिनय वाली शमशेरा जिस बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज नौवें दिन दर्शकों को तरसी उसमें इन फिल्मों के त्रुटिपूर्ण कथ्य और बेजान प्रस्तुति का रोल ज्यादा रहा। इससे ठीक पहले कंगना रनौत की धाकड़ भी अपनी रिलीज के आठवें दिन पूरे देश में बीस टिकट बिकने की शर्म झेल चुकी है। अप्रैल-मई में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की झड़ी बताती है कि कारण सिर्फ बायकॉट तक सीमित नहीं है। लंबे समय से रिलीज तलाश रही शाहिद कपूर की जर्सी अप्रैल में आई लेकिन केजीएफ 2 के तूफान में टिक नहीं पाई। अप्रैल में ही अजय देवगन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 को दर्शकों ने नकार दिया। मई में आई रणवीर सिंह की जयेशभाई जोरदार के खस्ता प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि दर्शकों की नब्ज पर हिंदी फिल्मकारों का हाथ नहीं है। हर फिल्म के फ्लॉप होने की अलग वजह ढूंढी जा सकती है पर बुनियादी बात यही है कि बॉलीवुड की फिल्में अब बड़े बजट, बड़े सितारे या हिट फॉर्मूले को भुनाकर दर्शक नहीं जुटा सकेंगी। द कश्मीर फाइल्स की बात करना यहां बेमानी है क्योंकि इस फिल्म की सफलता के कारणों पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस फिल्म की सफलता का सोशल मीडिया में उठे तूफान से संबंध रहा है।

कोरियन और दक्षिण की फिल्मों के आगे फीका बॉलीवुड
बायकॉट, बॉलीवुड और मनोरंजन
सोशल मीडिया ने आम आदमी के हाथ में भस्मासुर जैसी जो ताकत दी है, उसकी एक बानगी है ‘बायकॉट बॉलीवुड’ का ताजा उन्माद। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहिष्कार की इस मुहिम का हिंदी फिल्मों को लेकर बने नकारात्मक माहौल से रिश्ता है। कलाकारों के पुराने बयानों को नई बहस में घसीटकर जनता के रुख को प्रभावित करना ऐसा हथियार बनता जा रहा है जिससे पार पाने का रास्ता फिलहाल किसी के पास नहीं है। बहिष्कार की यह मुहिम ‘कैंसिल कल्चर’ का एक रूप है, जिसने पूरी दुनिया में कला, कलाकारों और नामचीन लोगों के वजूद को चुनौती दी है। अनुराग कश्यप इसका ताजा उदाहरण हैं, जिन्होंने शायद मजाक में दोबारा के प्रचार के दौरान लोगों से अपील की थी कि उनकी भी फिल्म को बायकॉट करके ट्रेंड करवाएं। नतीजा क्या हुआ वह सबके सामने है। इसी तरह 2015 में भारत के मौजूदा सांप्रदायिक माहौल पर आमिर खान के बयान को आधार बनाकर लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से ठीक पहले उठी बायकॉट की आवाजों ने फिल्म के प्रदर्शन पर असर डाला।
2011 के ‘अरब स्प्रिंग’ से लेकर ‘मी टू’ मुहिम का असर, 2012 में निर्भया कांड के बाद देशव्यापी प्रदर्शन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पनपा उन्माद ऐसे सशक्त उदाहरण हैं, जो साफ बताते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ आभासी दुनिया का बेमानी शोर नहीं है। एक फिल्म की किस्मत तय करने में निर्देशक, कहानी, कलाकार और प्रचार-तंत्र से आगे इसकी कितनी भूमिका है यह शोध का विषय है। कलाकार अब इसके असर को स्वीकार करने लगे हैं। पिछले दो दशक से इंडस्ट्री में काम कर रही करीना कपूर को दर्शकों से अपनी फिल्म का बायकॉट न करने की अपील करनी पड़ी। यहां तक कि नेटफ्लिक्स पर आई डॉर्लिंग्स फिल्म से ताजा सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता विजय वर्मा ने भी एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा था कि “यह माहौल आपको डरा सकता है। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपने दस साल पहले कोई बात कही वो अब नागवार हो सकती है।” दशकों पहले किसी खास संदर्भ में कही गई बात के आधार पर भी किसी के पूरे कला-कर्म को नकार देने की ताकत रखने वाले ‘कैंसिल कल्चर’ ने सोशल मीडिया के जरिये ऐसी ताकत दर्शकों को दी है जिसने सिनेमा और दर्शक के बीच ताकत के रिश्ते में तब्दीली के संकेत दिए हैं। कहानियां, उन्हें कहने के तरीके और मनोरंजन फिल्मों की सफलता-असफलता तय करते आए हैं लेकिन इस मुहिम ने जरूर दिखा दिया है कि भारत में फिल्म उद्योग का सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। हिंदी फिल्मों की बदहाली के इस दौर का छिद्रान्वेषण बेहद जरूरी है जिससे सारे पहलुओं पर नजर डाली जा सके।
भारतीय सिनेमा का लेबल लगाए बॉलीवुड का संकट देश के भीतर और बाहर दोनों जगह बराबर दिखाई दे रहा है। इसी साल मई में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक कान फिल्मोत्सव में भारत ने कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की। भारत के सरकारी दल-बल की तस्वीरें मीडिया में तैरती रहीं। भारतीय सिनेमा का ग्लैमरस प्रतिनिधित्व करती हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के महत्वाकांक्षी बयान और कपड़ों की चर्चा-आलोचना हुई। समारोह में छह भारतीय फिल्में भी दिखाई गईं लेकिन मजाल है कि एक भी हिंदी फिल्म मुख्य प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाई हो। जख्म पर नमक ये कि छोटे से देश दक्षिण कोरिया की फिल्में न सिर्फ सीधे मुकाबले में रहीं बल्कि पार्क चान-वूक को मिले सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार समेत दो पुरस्कारों के साथ उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। वूक की फिल्म डिसीजन टू लीव एक जासूसी रोमांस कथा है, जो एक आदमी की हत्या और उसकी पत्नी पर संदेह के इर्द-गिर्द बुनी गई है। यह तर्क फिजूल है कि फिल्म समारोहों में खास तरह की यथार्थवादी फिल्मों को ही जगह मिलती है इसलिए बॉलीवुड पीछे रह जाता है। यह स्थिति इन फिल्मोत्सवों/समारोहों के सीमित नजरिये पर बहस करके निपटायी जा सकती हैं। इन बातों को यह कहकर भी टाला जा सकता है कि हिंदी सिनेमा को किसी विदेशी समारोह में तालियों की दरकार नहीं, लेकिन जब देसी दर्शकों की ही तालियां न मिल रही हों और दक्षिण कोरियाई फिल्मों, धारावाहिकों और पॉप संगीत की सुनामी में बॉलीवुड की नैया डूबती नजर आए तो सवाल उठाना स्वाभाविक है।
दूसरे, जब मामला अंतरराष्ट्रीय साख और वैश्विक पहुंच का हो तो इन समारोहों का मंच क्या अहमियत रखता है इस पर सवाल उठाना बेमानी है। वरना टॉम क्रूज जैसे हॉलीवुड के दिग्गज नाम को अपनी बहुचर्चित फिल्म टॉपगन: मैवरिक लेकर कान जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉलीवुड की रंगीली दुनिया में संकट के संकेत इतने साफ हैं कि इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह करवट लेते वक्त की आहट है जिसकी जड़ में कई देसी-विदेशी कारण हैं।
दक्षिण कोरियाई सिनेमा की लहर में डूबता बॉलीवुड?
कोई सिनेमाई-संस्कृति किसी खास वक्त पर अपनी पहचान कायम करती है या चूकती है तो इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों का पूरा संदर्भ होता है जो अहम भूमिका निभाता है। नब्बे के दशक में जब बॉलीवुड की कहानी परवान चढ़ी तब देश में आर्थिक उदारवाद की बयार बहनी शुरू हुई थी। नया आर्थिक परिवेश, विदेशी कंपनियों की आमद, नई नौकरियां और देश की सीमाएं लांघकर बाहर निकलने के नए मौके। भौगौलिक दायरे से बाहर एक वैश्विक ‘भारतीय’ की नई सांस्कृतिक श्रेणी इसी दौर में पैदा हुई जिसमें चमचमाते बॉलीवुड ने गरीब भारत को किनारे कर अपना दर्शक-वर्ग खोज लिया। उस खास लम्हे में शुरू हुई कहानी शायद अब इस मोड़ पर आ गई है जहां से घर लौटकर देसी दर्शकों का दिल जीतने के सिवाय अब हिंदी सिनेमा के पास कोई चारा नहीं बचा है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नितांत देसी परिवेश वाली कहानियों की जोरदार स्वीकार्यता हो या फिर पैरासाइट जैसी दक्षिण कोरियाई फिल्मों की वैश्विक सफलता, इन सब में समान बात यही है कि ये कहानियां स्थानीय जिंदगी और आम अनुभवों के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं, जो रोमांस-रोमांच में भी पीछे नहीं रहतीं। फिलहाल ‘हालयुवुड’ यानी दक्षिण कोरियाई फिल्मों की लहर की चर्चा जोरों पर है लेकिन इसके पीछे उस देश का जबरदस्त उतार-चढ़ाव वाला सफर रहा है, जिसने सिनेमा को नित नए राजनैतिक और सामाजिक संदर्भ दिए। देश के भीतर ऐसे तमाम बदलाव हुए जिन्होंने कोरियाई सिनेमा को लोकप्रियता के वर्तमान दौर तक पहुंचाने में मदद की है।
विविधतापूर्ण, मनोरंजक और कलात्मक फिल्में परोसने वाले दक्षिण कोरियाई उद्योग ने यह रफ्तार नब्बे के दशक में पकड़ी जब बॉलीवुड ने प्रवासी भारतीयों के साथ अपना रोमांस शुरू किया था। कोरियाई फिल्म उद्योग में बदलावों का अहम दौर जुलाई 1987 से शुरू हुआ जब एक समझौते के तहत हॉलीवुड फिल्मों को दक्षिण कोरिया में वितरित करने की इजाजत मिली। आयातित फिल्मों से कोटा व्यवस्था हटने और किसी भी कंपनी को बिना कोई धनराशि जमा किए फिल्म निर्माण में शामिल होने की इजाजत, जैसे कदमों ने एक नया रास्ता खोला। हॉलीवुड फिल्मों के आयात से पहले तो खूब कमाई हुई लेकिन धीरे-धीरे इसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी। फिल्म कंपनियों को बिना किसी कोटा के फिल्में आयात करने की इजाजत तो थी लेकिन सालाना एक देसी फिल्म बनाने का नियम भी था। लिहाजा कुछ कंपनियों ने देश के भीतर फिल्में बनाने पर ध्यान लगाना शुरू किया। 1984 में दक्षिण कोरिया में 20 फिल्म निर्माण कंपनियां थीं जिनकी संख्या 1991 में 121 तक पहुंच चुकी थी। साथ ही थियेटरों में साल में 100 दिनों से ऊपर का कोटा कोरियाई फिल्मों के लिए नियत था।
इसी दौर में कला और वीडियो की दुनिया से युवा निर्देशकों ने फिल्मों में कदम रखा और फिल्म उद्योग को नए नजरिये, कहानियों और ऊर्जा से भर दिया। 1988 से 1997 के बीच ऐसे नाम उभरे जिनका जोर फिल्मों में यथार्थवाद और गंभीर संवाद पर रहा। इसे कोरियन न्यू-वेव सिनेमा कहा जाता है। निर्देशक जांग सन-वुन और ली म्यांग-से कुछ मुख्य नाम हैं, जिन्होंने फिल्मी भाषा और फिल्म निर्माण को सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों और आम जिंदगी के मसलों से जोड़ना जरूरी माना। न्यू-वेव फिल्मों ने दक्षिण-कोरिया में राजनैतिक दमन, शहरी जिंदगी, श्रमिक-जीवन और छात्र-आंदोलनों जैसे सामाजिक विषयों को केंद्र में रखा। अ रूस्टर (1990) और द डे अ पिग फेल इंटू द वेल (1996) जैसी फिल्मों ने देश के सबसे बड़े शहर सोल को खोखले रिश्तों, अकेलेपन और मानसिक समस्याओं से जूझते लोगों की कहानियों के जरिये रेखांकित किया। इस दौर की फिल्मों में कोरिया के राजनैतिक इतिहास और महिलाओं की सामाजिक स्थिति का चित्रण भी देखने को मिलता है। कोरियन न्यू-वेव का देसी फिल्म उद्योग पर दूरगामी असर पड़ा। इसने निर्देशकों को अपना खास स्टाइल विकसित करने का मौका दिया और नई प्रतिभाओं की फिल्में दर्शकों तक पहुंचती रहीं। कुल मिलाकर इंडस्ट्री का विस्तार करने में यह दौर खासा अहम माना जाता है, हालांकि देसी फिल्मों के लिए थियेटर तक पहुंचना आसान नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर विदेशी फिल्मों का कब्जा रहता था पर देसी फिल्मों के लिए स्क्रीन कोटा होने का मतलब था कि विदेशी फिल्मों की छाया में भी कोरियाई फिल्में पलती-बढ़ती रहीं।
1980 के दौर में देसी फिल्में निजी निवेश से बनती रहीं यानी कंपनियों के पास निर्माण पूंजी जुटाने का कोई संस्थागत साधन नहीं था। यह स्थिति 1993 में बदली जब सरकार ने फिल्म उद्योग को सेवा क्षेत्र से निकाल कर निर्माण क्षेत्र का हिस्सा बनाया और फिल्म कंपनियों के लिए बैंकों से लोन लेना संभव हुआ। इसके साथ ही निर्देशकों ने उन बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से पैसा जुटाना भी शुरू किया जिनके पास पहले से वीडियो प्रभाग थे। इनमें सैमसंग, डेवू और ह्यूंडै शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर 1992 से 1996 के बीच कम से कम बीस फिल्मों के निर्माण में सैमसंग किसी न किसी रूप में भागीदार रही है। फिल्मों को कॉरपोरेट का साथ मिलना शुरू हुआ तो फिल्मों के बाजार में प्रतियोगिता का दौर भी शुरू हुआ। इस संदर्भ में 1996 खास तौर से निर्णायक रहा क्योंकि इस साल सेंसरशिप को खत्म किया गया, जिसका सीधा संबंध सिनेमा में नई और धारदार आवाजों के उदय से था जिन्हें बाद में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में बढ़ावा मिला। इसी साल बुसान फिल्म महोत्सव की भी नींव रखी गई, जो फिल्म और मीडिया उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार खोजने में अहम साबित हुआ। इसकी शुरुआत कोरियाई संगीत के पॉप और ड्रामा सीरीज के अंतरराष्ट्रीय वितरण के साथ हुई जिसने धीरे-धीरे मजबूत हुई देसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जगह बनाई।
दक्षिण कोरियाई फिल्म उद्योग के पास दुनिया को देने के लिए हर जॉनर की फिल्में मौजूद हैं- चाहे वह बॉलीवुड स्टाइल रोमांस हो, साइंस-फिक्शन और हॉरर हो या फिर यथार्थवादी मनोरंजन। फिल्मों की कहानियां और किरदार देसी परिवेश और अनुभवों को बुनकर लाती हैं, जिन पर वास्तविकता की छाप है। इसके विपरीत बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों से भारतीय जिंदगी के विविध रूपों को बाहर धकेल कर एक अलग ही दुनिया बनाई जिसमें शहरी और ग्लोबल दिखने वाले किरदारों के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं थी। दक्षिण कोरियाई सिनेमा की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता की जड़ में जबरदस्त घरेलू इंडस्ट्री और उसके दर्शक हैं जबकि बॉलीवुड फिल्मों के हाथ से घरेलू दर्शक छिटकते जा रहे हैं।

दुनिया भर की वेबसीरीज के आगे बॉलीवुड को करनी होगी कड़ी मेहनत
हालयुवुड और बॉलीवुड की स्थितियों में आज अंतर दिख रहा है, लेकिन कई समानताएं भी मिलेंगी। मसलन, 2010 में दिबाकर बनर्जी की लव, सेक्स और धोखा के साथ ही भारत में भी एक नए किस्म के इंडिपेंडेंट और यथार्थवादी सिनेमा की धारा पैदा हुई जिसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा कहते हैं। विक्रमादित्य मोटवाने, अनुराग कश्यप, रितेश बत्रा, नीरज घायवान जैसे युवा निर्देशकों ने देसी जिंदगी को परदे पर लाने का सिलसिला शुरू किया। ये फिल्में अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों में लगातार पहुंचती भी रही हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के मुकाबले भारत में इस तरह की फिल्मों की संख्या अब भी कम है। इसकी वजह सरकारी रवैये के साथ-साथ फिल्म उद्योग की अपनी कार्य-प्रणाली में भी देखनी होगी, कि वह नई प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए क्या करता है। भाई-भतीजावाद की बहस ने फिल्मी सितारों के बच्चों की फिल्में नकारे जाने में एक मुख्य भूमिका अदा की है। हकीकत भी यही है कि फिल्मी परिवारों के अलावा इक्का-दुक्का नए चेहरे ही इंडस्ट्री में कदम रख पाते हैं। ऐसे में कहानियों और सरोकारों में विविधता की उम्मीद कैसे की जाए?
दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम की बेशुमार सफलता पर बात करते हुए सीरीज निर्देशक ह्वांग डौंग ह्योक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दक्षिण कोरियाई समाज देश और दुनिया में हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनशील है और कोरियाई कंटेंट बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को आत्मसात करने में कामयाब रहा है। अब इस नजरिये से अगर बॉलीवुड को देखा जाए तो फ्लॉप हुई सारी फिल्मों को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि एक भी ऐसी कहानी नहीं थी जो सितारों की ताकत या नॉस्टेल्जिया के कंधे पर सवार होकर सफल होने की कोशिश न कर रही हो। खासकर कोविड के दौर में दर्शकों ने दुनिया भर से आने वाली इतनी फिल्में और सीरीज देख ली हैं कि उनकी जेब से टिकट के पैसे निकलवाने के लिए बॉलीवुड को ग्लैमर और रूमानी जज्बात से आगे जाकर सोचना होगा।
दक्षिण भारतीय सिनेमा का बवंडर
बॉलीवुड की धराशायी होती फिल्मों के बीच आरआरआर, पुष्पा और केजीएफ ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की धाक जमा दी और इनकी सफलता का कारवां चल निकला। सफलता मिली है तो चर्चा भी लाजमी है। वैसे तो एक-एक फिल्म की कहानी को खोलकर देखा जाए तो तारीफ करने की वजहें शायद कम होती जाएंगी पर बात केवल बॉक्स ऑफिस की नहीं है। बात यह भी है कि हिंदी फिल्में ऐसा बहुत कुछ करने से चूकती रहीं जिसकी पूर्ति दक्षिण भारतीय फिल्मों ने की। इसमें गुस्से से भरे आम और गरीब किरदारों की अपील ही नहीं, कई और वजहें भी शामिल हैं।
कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया में सिनेमा उद्योग को जैसा जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, उससे उबरने में लंबा वक्त लगना तय है। हिंदी सिनेमा को संजय लीला भंसाली निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रदर्शन से थोड़ी उम्मीदें बंधी थीं, हालांकि यहां यह भी देखना होगा कि आलिया भट्ट की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के साथ ही पवन कल्याण और राणा डुग्गूबती की तेलुगु फिल्म भीमला नायक भी रिलीज हुई थी। एक हिट मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियम के इस बेहद सफल रीमेक का हिंदी डब संस्करण रिलीज नहीं किया गया। यह हिंदी सिनेमा के भीतर की खदबदाहट नहीं तो और क्या है कि पिछड़ जाने के डर से मुकाबले में खड़ी हो रही फिल्मों को ही रोकना पड़े। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जबरदस्त प्रदर्शन और बॉलीवुड को उससे मिल रही टक्कर अब कोई नया मुद्दा नहीं है पर इसमें कई बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा।
लॉकडाउन के चलते सिनेमाहॉल बंद रहने से जो आर्थिक झटका लगा वह इस परिदृश्य का एक पहलू है, लेकिन महामारी का सिर्फ आर्थिक संदर्भ नहीं है। इस वैश्विक संकट ने सिनेमा को ऐसा असाधारण विषय भी दिया जिसे केंद्र में रखकर इंसानी अनुभवों की कहानियां कहने में हिंदी सिनेमा चूक गया। सितारों के दम पर फिल्में बेचने की परंपरा इस माहौल में काम न आई। इस बेहद जटिल और कठिन अनुभव से खुद को अछूता रखने का नतीजा उस दर्शक वर्ग की लिस्ट में पिछड़ना था, जिसे ओटीटी पर भारतीय भाषाओं समेत पूरी दुनिया से विविधतापूर्ण सामग्री परोसी जा रही है। पुष्पा के तेवर, शोमैन राजामौलि का जलवा और केजीएफ में यश की डायलॉगबाजी ने अगर यह याद दिलाया कि थियेटर में सिनेमा देखने का उन्माद क्या होता है, तो डिजिटल माध्यम या ओटीटी ने एक ऐसी जगह पैदा की जो निजी अनुभवों और संवेदनशील कहानियों के लिए मुफीद माध्यम बन गया।
सिनेमाई मनोरंजन के विकल्प के तौर पर उभरे ओटीटी माध्यमों पर इस जगह को खास तौर से भरा मलयाली फिल्मों ने, जहां निर्देशकों ने कोविड से गुजर रही जिंदगी को कहानियों में पिरोया। महामारी के माहौल में भी मलयाली सिनेमा में नए निर्देशक ओटीटी के जरिये कदम रखते रहे और बिना बड़े सितारों का सहारा लिए आम लोगों की कहानियों पर फिल्में बनाते रहे। 2021 में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कोविड की पृष्ठभूमि पर बनी फहद फासिल की थ्रिलर जोजी या फिर पहली बार फिल्म निर्देशित कर रहे सानू जॉन वर्गीज की आरकरियम, जिसमें कहानी कोविड से जूझ रहे किरदारों को दिल्ली से निकाल कर केरल की जमीन पर ले जाती है, जहां छुपा है एक अपराध का अतीत। दक्षिण कोरियाई सिनेमा की तरह मलयाली सिनेमा ने लगातार वक्त की नब्ज पर हाथ रखा है। 2019 में अभिनेता और फिल्मकार आशिक अबू ने वायरस नाम की थ्रिलर बनाई जिसके केंद्र में था 2018 में केरल में फैला नीपा वायरस। क्या हिंदी सिनेमा को फीकी प्रेम कहानियों और ठीक से हिंदी में संवाद भी न बोल पाने वाले फिल्मी सितारों के बच्चों को दर्शकों पर लादने के अलावा ऐसे किसी मसले की सुध आई है? दक्षिण भारत के मसलों को अगर छोड़ भी दें तो क्या उत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं घटा जिस पर कुछ कहने की जरूरत बॉलीवुड को महसूस हो? वक्त का हाथ थामकर आगे बढ़ने में नाकाम बॉलीवुड अब मनोरंजक के तौर पर कतार में पीछे खड़ा है और मुकाबले में हैं आर्ट सिनेमा से लेकर विशुद्ध मनोरंजन परोसने वाली दुनिया भर के छोटे-बड़े देशों से आ रही फिल्में और धारावाहिक। दर्शकों को छोटे स्क्रीन पर मौजूद बेशुमार सामग्री को छोड़कर थियेटर तक बुलाने के लिए बॉलीवुड को ईमानदार कहानियां और सिनेमाई करिश्मा बुनकर लाना होगा।
पुष्पा की नकल नहीं, जिद चाहिए
देश के भीतर और बाहर जो कुछ घटित हो रहा है, मीडिया-परिवेश ने जिस तरह की करवट ली है, उस सबको नजरअंदाज करके ‘मुख्यधारा’ हिंदी सिनेमा के तौर पर प्रतिष्ठित बॉलीवुड के लिए आगे का रास्ता तय करना संभव नहीं होगा। यह रणनीतिक चुनाव का मौका है कि इस वक्त का इस्तेमाल दक्षिण भारतीय सिनेमा को खदेड़ने और दक्षिण कोरियाई सिनेमा के बगल से बच निकलने की कोशिशों में लगा दिया जाए या फिर ऐसे नए किरदारों और कहानियों को तलाश कर लाया जाए जो देसी दर्शकों का हाल-ए-दिल बयां कर सकें, जिनमें सिनेमाई रोमांच हो तो अपने जैसे लगने वाले किरदार भी। इसके लिए हिंदी सिनेमा को एक और पुष्पा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुष्पा जैसी जिद की जरूरत जरूर है।
2022 का फ्लॉप शो
बच्चन पांडेय (18 मार्च)
साजिद नाडियाडवाला की फिल्म बच्चन पांडेय में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज, कृति सेनन, अरशद वारसी जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म 2014 में आई एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ठीक शुरुआत की, लेकिन बाद में दर्शक नहीं मिले।
अटैक पार्ट 1 (1 अप्रैल)
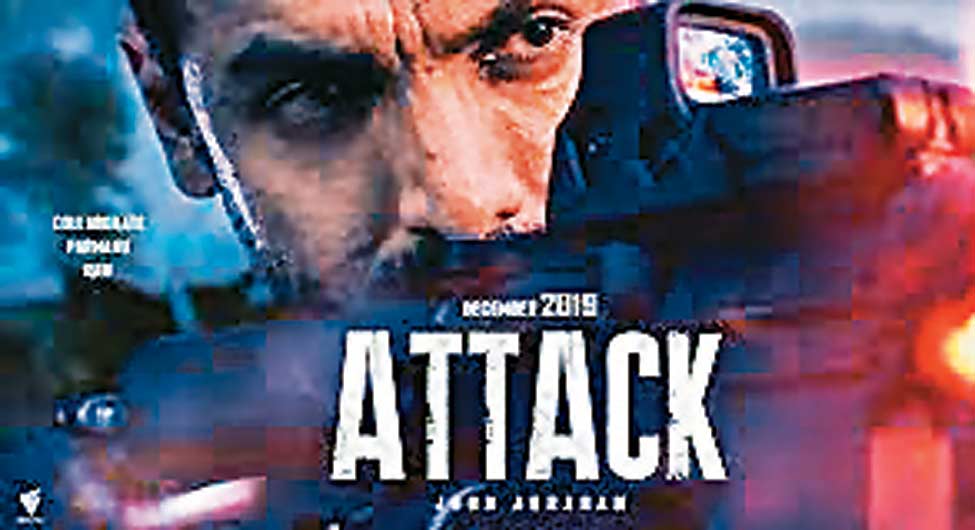
अभिनेता जॉन अब्राहम, जैकलीन फर्नांडीज और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म अटैक पार्ट 1 एक्शन से भरी हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म है। जयंतीलाल गढ़ा, अजय कपूर और जॉन अब्राहम ने फिल्म का प्रोडक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी शुरुआत रही। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों ने फिल्म को नकार दिया।
जयेशभाई जोरदार (13 मई)
यशराज फिल्म्स की फिल्म जयेशभाई जोरदार में मुख्य भूमिका रणवीर सिंह ने निभाई थी। रणवीर सिंह की पिछली फिल्मों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी को इस फिल्म से उम्मीदें थीं। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों को लुभा नहीं सकी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी हालत रही फिल्म की।
जर्सी (22 अप्रैल)
कबीर सिंह की कामयाबी के बाद शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी से सभी को उम्मीदें थीं। 2019 में इसी नाम से आई एक तेलुगु फिल्म की इस रीमेक की कहानी एक क्रिकेटर के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर की मौजूदगी भी फिल्म फ्लॉप होने से नहीं बचा सकी।
हीरोपंती 2 (29 अप्रैल)
निर्देशक अहमद खान की फिल्म। 2014 में आई फिल्म हीरोपंती की सीक्वल हीरोपंती 2 साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस की पेशकश है। मुख्य भूमिका में टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया नजर आए। ए आर रहमान के संगीत से सजी यह एक्शन फिल्म समीक्षकों और दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
रनवे 34 (29 अप्रैल)
महानायक अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी जैसी हस्तियों के अभिनय से सजी फिल्म रनवे 34 जेट एयरवेज के 2015 में हुए एक्सीडेंट से प्रेरित थी। फिल्म समीक्षकों ने फिल्म को यथार्थ से दूर बताया। बुरी बॉक्स ऑफिस शुरुआत के बाद फिल्म फ्लॉप रही।
धाकड़ (20 मई)
धाकड़ में कंगना रनौत एक्शन अवतार में नजर आईं। समीक्षकों और दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर के बाद काफी उम्मीदें थीं मगर फिल्म के रिलीज होने पर इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई और हफ्ते भर में सिनेमाघरों से उतर गई।
अनेक (27 मई)

नॉर्थ ईस्ट भारत के महत्वपूर्ण विषय पर बनाई गई फिल्म। आयुष्मान खुराना और निर्देशक अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 के बाद फिर से सिनेमाई जादू रचने का प्रयास किया लेकिन फिल्म दर्शकों को छूने में नाकाम रही। फिल्म के नैरैटिव पर विवाद हुआ। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन खराब रहा।
सम्राट पृथ्वीराज (3 जून)
यशराज फिल्म्स की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में नजर आए। किरदार में न जंचने के कारण दर्शकों ने फिल्म और अक्षय कुमार को नकार दिया। फिल्म समीक्षकों ने भी अक्षय कुमार की आलोचना की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही।
शाबाश मिठू (15 जुलाई)

भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज के जीवन पर आधारित फिल्म शाबाश मिठू में अभिनेत्री तापसी पन्नू ने मिताली राज का किरदार निभाया। हाल के दिनों में तापसी पन्नू को महिला खिलाड़ियों की बायोपिक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। मगर मिताली राज की भूमिका दर्शकों और समीक्षकों को पसंद नहीं आई।
शमशेरा (22 जुलाई)
चार साल बाद रणवीर कपूर ने फिल्म शमशेरा से वापसी की। यशराज फिल्म्स की इस फिल्म में संजय दत्त और वाणी कपूर जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने उम्मीदें जगाई थीं मगर दर्शकों और समीक्षकों को यह पसंद नहीं आई। फिल्म में रणवीर कपूर के अभिनय की तीखी आलोचना हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औंधे मुंह गिर गई।
रक्षाबंधन (11 अगस्त)
रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हुई आनंद एल राय की फिल्म का जोर शोर से प्रचार हुआ लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी। अक्षय कुमार की इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली लेकिन दर्शक फिल्म देखने के लिए थियेटरों तक नहीं पहुंचे। फिल्म के फ्लॉप होने की मुख्य वजह कमजोर कहानी का होना रहा।
लाल सिंह चड्ढा (11 अगस्त)
अभिनेता आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म अमरीकी फिल्म फॉरेस्ट गंप पर आधारित है। बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का सामना करना पड़ा। तमाम कोशिश के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी।
दोबारा (19 अगस्त)
अनुराग कश्यप की यह साइंस फिक्शन फिल्म है। तापसी पन्नू ने मुख्य भूमिका में हैं। समीक्षकों के अच्छे रिव्यू मिले लेकिन आम दर्शकों को नहीं लुभा पाई। जटिल कहानी के कारण दर्शक भ्रमित हुए। दर्शक न मिलने के कारण शो कैंसल हुए।
लाइगर (25 अगस्त)

इस फिल्म का बिजनेस भी बहुत ठंडा रहा। विजय देवरकोंडा उत्तर भारतीय दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रहे। फिल्म आने से पहले जितनी हाइप थी, उसका एक प्रतिशत भी दर्शकों को देखने को नहीं मिला।
(स्वाति बक्शी वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय, लंदन में हिंदी सिनेमा पर शोध कर रही हैं और समसामयिक मुद्दों पर लिखती हैं)








