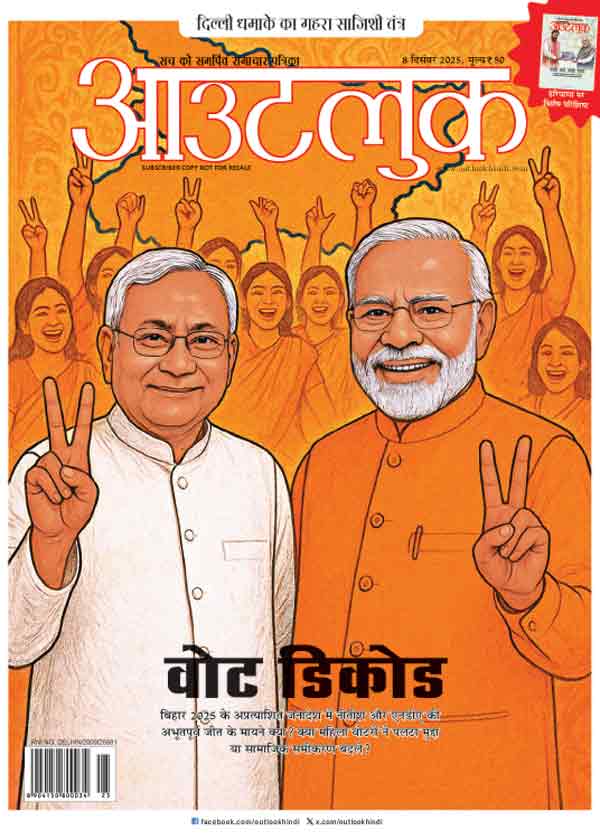बात नब्बे के दशक के आखिरी वर्षों और राजधानी दिल्ली के ऊंचे लोगों के लकदक मार्केट साउथ एक्सटेंशन की है। तब ईबोनी नाम का एक कई मंजिला स्टोर हुआ करता था। उस पूरी इमारत पर ऊपर से नीचे तक एक विशाल फेस्टून सबका ध्यान खींच रहा था। उस पर अंग्रेजी में लिखे लफ्ज हैरान कर रहे थे। उसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा बनता था, ‘ऐ! खुदगर्जो, बेवफा, दगाबाजो, झूठो....आओ सब आओ, अब दौर हमारा है।’ वह मानो आने वाले दौर का एहसास दिला रहा था। मगर तब तक ऐसे दौर पर सहसा भरोसा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। हालांकि जिंदगी के हर हलके में उसका हल्का-हल्का एहसास होने लगा था। तब भी नौजवानों में मानवीय आदर्श की भावनात्मक लहरियां गुम-सी नहीं हुई थीं।
लेकिन देश का खासकर मध्यवर्ग उदारीकरण की फिजा में नई आजादी का एहसास करने लगा था। उसकी लालसाओें के सारे दरवाजे खुल रहे थे। राज्यतंत्र कल्याणकारी योजनाओं, सार्वजनिक उद्यमों और शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भूमिकाएं सिकोड़ रहा था। सब्सिडी सबसे दागदार शब्द बनने लगा था और उसे विकास की सबसे बड़ी अड़चन बताया जाने लगा था। लेकिन, दूसरी ओर निजी उद्योगों और बड़े घरानों के लिए सरकारी थैलियां खोली जा रही थीं।
लिहाजा, नए उद्योग और फिर सूचना क्रांति खासकर शहरी मध्यवर्ग के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही थी। उसकी आमदनी बढ़ रही थी और तमाम विलासिताओं के लिए राह आसान हो रही थी। मध्यवर्ग इस आजादी के स्वाद में अपने को देश के गरीब-गुरबों, सामाजिक न्याय-अन्याय की जिम्मेदारी से भी मुक्त करने लगा। तब प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने लिखा था कि मध्यवर्ग अब अपनी आकांक्षाओं, लालसाओं की पूर्ति के लिए देश की तमाम जिम्मेदारियों और आदर्शों का बोझ अपने कंधे से उतार फेंकना चाहता है।
लेकिन शासक वर्ग नव-पूंजीवाद की इस फिजा में उसे विकास का हरावल दस्ता बता रहा था। उसे नए आकांक्षी वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। इसके नतीजे एक दूसरी दिशा में भारी तनाव भी पैदा कर रहे थे। खेती-किसानी धीरे-धीरे उपेक्षा का शिकार होने लगी, जो देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करती है। पुराने किस्म के छोटे उद्योग-धंधे सिकुड़ने लगे थे। इससे समाज में तरह-तरह के दबावों से अस्मिता और पहचान की राजनीति का सूत्रपात होने लगा। हालांकि नब्बे के दशक की शुरुआत में ही खासकर मंडल और मंदिर आंदोलनों ने एक मायने में इस पहचान की राजनीति को हवा दे दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के ही एक एजेंडे से निकली सामाजिक न्याय की धारा से निकला मंडल और दलित आंदोलन भी कुछ खास जातियों की पहचान की राजनीति में सिमटने लगा और उसका हश्र परिवारवाद के नए रूप में सामने आया।
इसके साथ-साथ मंदिर आंदोलन ने ध्रुवीकरण की उस राजनीति को हवा दी जो एक नए राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ रही थी। इस राष्ट्रवाद में देश के शासक वर्ग (सत्ता, उद्योग घरानों और संसाधनों पर पकड़ रखने वाला वर्ग) पर सवाल उठाना लगातार वर्जित होता गया है। ‘पराया’ और ‘शत्रु’ तलाशने की फितरत जुनून की शक्ल लेने लगी। शायद इसी क्रम में ‘छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों’ की तलाश भी शुरू हुई। ऐसे ही दौर में देसी भाषा में जनमत को सही दिशा में प्ररित करने की अपनी कोशिशों के तहत आउटलुक समूह ने 2002 में जब हिंदी का प्रकाशन शुरू किया तो संस्थापक प्रधान संपादक विनोद मेहता ने अपनी कटिबद्धता इन शब्दों में जाहिर की थीः
“हम आउटलुक को एक खुला, स्वतंत्र, उदार और प्रगतिशील प्रकाशन बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आज के हिसाब से ये शब्द भारी-भरकम लग सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि आज भी शब्दों की प्रासंगिकता बरकरार है। हम भी खुद को देश की उस जमात में शुमार करना चाहते हैं जिसका तमाम राजनेताओं और राजनीतिक दलों से भरोसा उठ गया है। बहरहाल, हम दृढ़ता के साथ निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कुछ लोगों ने मुझ पर छद्म धर्मनिरपेक्ष होने का ठप्पा लगा रखा है अपनी जगह वे एकदम सही हैं। यदि एक बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होना छद्म धर्मनिरपेक्षता है तो मुझे इस पदवी को स्वीकार करते हुए गर्व है।”
तब उस यशस्वी संपादक ने बड़ी उम्मीद से यह भी वादा किया था कि “मुझे आशा है कि आउटलुक हिंदी समाज की संस्कृति, साहित्य और कलाओं से संबंधित मुद्दों पर वाद-विवाद, संवाद और बहस-मुबाहिसे का मंच बनेगा। हमारी कोशिश होगी कि हिंदी में लिखा जा रहा श्रेष्ठ साहित्य इसके पन्नों की शोभा बढ़ाए।”
उसी वादे को साकार करने की एक छोटी-सी कोशिश आपको अगले पन्नों पर दिखेगी। आज समाज, साहित्य, संस्कृति और सबसे बढ़कर राजनीति ऐसी चुनौतियों से रू-ब-रू है, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गईं। समाज निरंतर नए-नए खांचों में बंटता जा रहा है, बल्कि हर खांचा एक-दूसरे के प्रति गहरी शंका की दृष्टि से देखने लगा है। कहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और महापुरुषों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विभाजनकरी मंसूबे को हराने के लिए समूचे देश में एक समरस राष्ट्र की भावना जगाई थी, आज वही राष्ट्रवाद सबसे विदग्ध लगने लगा है। इसका आखिर समाधान क्या है? क्या हैं आज के हालात? यही जानने की कोशिश में हमने देश और खासकर प्रबुद्ध साहित्यकारों, कवियों, लेखकों का रुख किया है। इसमें हर लेखक की अपनी शैली और कुछ मामले में अपनी विधा में टिप्पणियां हैं जो मौजूदा हालात की भयावहता तो दर्शाती ही हैं, हमें एक नई सांस्कृतिक क्रांति की ओर बढ़ने का इशारा करती हैं। यानी आज एक नए रेनेसां की दरकार है।