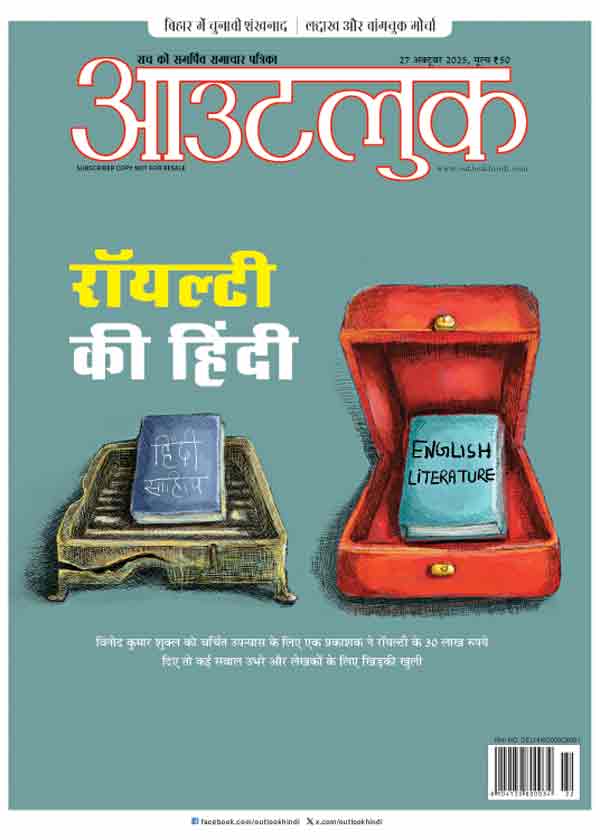मेरी राय में तो अयोध्या केस से जुड़े इस्माइल फारूकी मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास जरूर भेजा जाना चाहिए था। न्यायालय इसके पहले कई छोटे मामले भी बड़ी बेंच को भेज चुका है। अभी हाल ही में वोहरा संप्रदाय में प्रचलित लड़कियों से संबंधित एक कुप्रथा के मामले को पांच सदस्यों वाली पीठ के पास भेजा गया। इसमें तो कोर्ट को फौरन फैसला सुना देना चाहिए था कि यह प्रथा संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन उसे बड़ी बेंच को भेज दिया गया।
ऐसे में अयोध्या मामले को जरूर बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए था। आखिर अयोध्या मामला बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले ही आपस में टकरा रहे है। दूसरे, इस्माइल फारूकी मामले वाले बहुमत के फैसले में एक और समस्या यह है कि इसमें दूसरे धर्मों से तुलना की गई है। अगर यह तय करना है कि इस्लाम धर्म में नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, तो इसके लिए दूसरे धर्मों को देखने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, किसी धर्म के अनिवार्य पहलुओं की पड़ताल ही गलत है क्योंकि धर्म केवल अनिवार्य पहलुओं से नहीं बनता है। उसके किसी पहलू को छोटा या बड़ा बताना सही नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट न धर्मगुरु है, न ही वह धार्मिक प्रक्रियाओं का विशेषज्ञ है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि फारूकी मामले का बाबरी मस्जिद केस पर क्या असर पड़ेगा अहम बात यह है कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अनिवार्यता का सिद्धांत लागू किया जा रहा है। इससे एक गैर-जरूरी अंकुश लग जाता है।
कहने का मतलब यह है कि संविधान में कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनिवार्यता का पहलू या शर्त नहीं जोड़ी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे कई फैसलों में यह साफ-साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अपनी धार्मिक मान्यताएं रखने को स्वतंत्र है। मतलब यह कि कोई भी अपने भगवान या खुदा से जैसा चाहे रिश्ता रख सकता है। यही धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है।
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार, आधार और समलैंगिकता के मामले में व्यक्ति की स्वायत्तता को तरजीह दी है। जिस तरह किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सामाजिक जरूरतों को निजी तौर पर पूरा करने की इजाजत दी है, उसी तरह किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी चुनने की आजादी होनी चाहिए। उसके इस चयन पर अनिवार्यता की शर्त जोड़ना एक गैर-जरूरी प्रतिबंध लगाता है। मैं इस मुद्दे को बार-बार उठाता रहा हूं कि संवैधानिक न्यायालय को धार्मिक मुद्दों की व्याख्या से बचना चाहिए क्योंकि न्यायालय को धर्म के बारे में क्या पता है? मसलन, ईसाई धर्म के बारे में बिशप व्याख्या करेंगे, इस्लाम में मौलाना, तो हिंदू धर्म में उसे जानने वाले ही व्याख्या करेंगे। न्यायालय को तो यह कहना चाहिए कि हम तो संविधान को लागू करेंगे। हम उसके आधार पर तय करेंगे कि किस चीज की अनुमति मिलनी चाहिए या किस चीज की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
अभी हाल ही में सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। अगर महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म का अनिवार्य या अटूट हिस्सा मान लेता, तो ऐसे में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति न्यायालय नहीं दे पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलना महिलाओं के सम्मान और समानता के हक पर चोट है, इसीलिए उसने परंपराओं को न देखते हुए संवैधानिक अधिकार को तरजीह दी है। किसी भी धर्म की कोई मान्यता उसका अटूट हिस्सा है या नहीं, यह बहस न्यायालय को उस रास्ते पर ले जाती है, जिसमें उसकी विशेषज्ञता नहीं है।
तीन तलाक के मामले का ही उदाहरण लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक कुरान में नहीं है, इसलिए वह इस्लाम में नहीं है। कुरान के आधार पर उन्होंने कहा कि यह अवैध है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उसकी अनुमति देनी चाहिए। मैं यह कहता हूं कि संवैधानिक नैतिकता के आधार पर तीन तलाक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो यह कहना चाहिए कि हम यह नहीं देखेंगे कि आपका धर्म क्या कहता है, हम तो केवल यह देखेंगे कि संविधान क्या कहता है। सबरीमाला मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि धर्म की व्याख्या करने में संवैधानिक मूल्यों को देखा जाय। दरअसल, इन मामलों में फैसले का यही आधार होना चाहिए। यानी अगर धर्म का कोई हिस्सा संविधान से टकरा रहा है तो कोर्ट को उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। अदालत को तो संविधान के अनुसार ही फैसले सुनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून का न्यायालय है, आस्था का नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद मामले में नमाज का मसला गया था तो एक सवाल यह भी उठा था कि क्या विवादित जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था, तो न्यायालय ने इसका उत्तर देने से मना कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि न्यायालय के पास ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं थे। ऐसे में न्यायालय जब धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा बहस करेगी तो उसे कहा जाएगा कि यह तो आस्था का न्यायालय बन गया। न्यायालय को कानून और संविधान के तहत फैसले करने चाहिए। न्यायालय यह स्थापित करे कि संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता, समानता के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। यानी समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में टकराव होगा तो समानता के अधिकार को तरजीह मिलेगी। मैं इस बात से चिंतित हूं कि संविधान कहता है कि वह नागरिकों को अपने धर्म की हर बात मानने का अधिकार देता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तय करेंगे। उसके मुताबिक, केवल अनिवार्य पहलुओं को मानने का अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आपस में टकरा रहे हैं, उन पर उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि स्थिति साफ हो।
(लेखक एनएएलएसएआर लॉ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के कुलपति हैं। लेख प्रशांत श्रीवास्तव से बातचीत पर आधारित है)