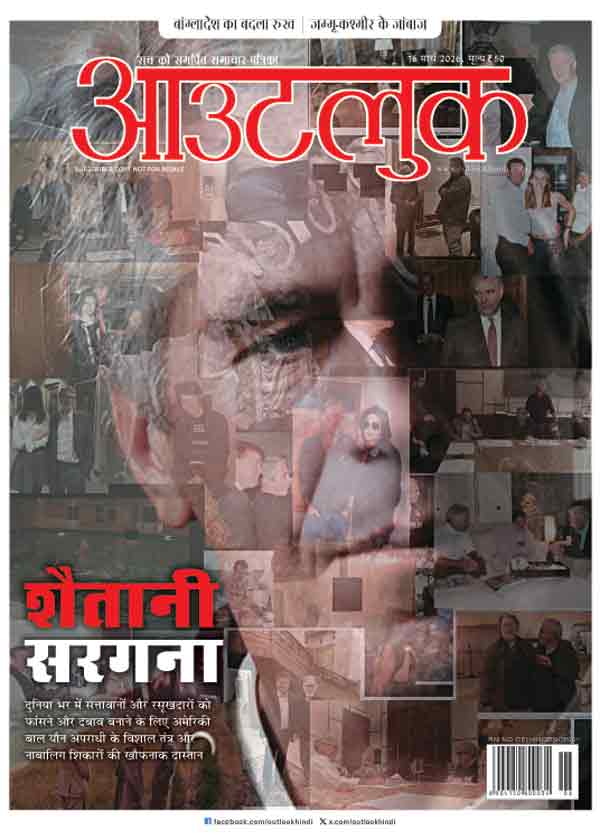छह साल बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर का चीन दौरा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा संकेत है कि ट्रम्प उथल-पुथल से नई दिल्ली की विदेश नीति की दिशा बदल रही है। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 25वीं बैठक कई देशों, रणनीतिक जानकारों और आर्थिक सलाहकारों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। बोहाई खाड़ी स्थित तियानजिन बंदरगाह 1979 के सुधारों के बाद से चीन के आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है। 10 देशों के एससीओ बैठक में चीन, भारत और रूस के बीच व्यापक मुद्दों पर कैसी सहमति बनती है, इसी पर अगली विश्व-व्यवस्था का अंदाजा लगेगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विवादास्पद बयानों से जटिल हो गई है।
टेक्नोलॉजी, खासकर डिजिटल आर्थिकी के इस युग में वैश्विक अर्थव्य्वस्था के आधार पर करवट ले रही नई भू-राजनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विमर्श पर हावी हो रही है। इसलिए रूस, चीन और भारत तीनों के नेता एससीओ में मिलेंगे, तो उनके सामने मुद्दों का भरा-पूरा टोकरा होगा, जिनके दायरे में बर्फीले आर्कटिक से लेकर गर्म हिंद महासागर तक फैला विशाल भौगोलिक क्षेत्र है। उसमें वैकल्पिक व्यवस्थावओं के साथ टैरिफ से लेकर पाबंदियों और बैलिस्टिक धमकियों का सामना करने जैसे तमाम मसले होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा?
सबसे पहले, मेजबान चीन में बहुत कुछ बदल गया है। 1965 में चाऊ एन लाई के ‘चार आधुनिकीकरण’ के अक्स तियानजिन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिलहाल चीन, भारत और रूस को ट्रम्प के लगाए अतार्किक टैरिफ प्रतिबंधों के चलते अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा की रणनीतियों में तालमेल बैठाना होगा। चीन में एक कहावत है झोंग श्यू वेई ती, शी श्यू वेई योंग (यानी पश्चिमी पढ़ाई का इस्तेमाल करो), जिसकी मिसाल 1949 से ही चीन में दिखी है। आज इसे ‘विशेष चीनी समाजवाद’ कहा जा सकता है।
चीन के नेता हमेशा ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था की तलाश में लगे रहे हैं, जो एकदम आधुनिक मगर खांटी चीनी हो। अगर कोई सन यात-सेन के ‘तीन लोक सिद्धांतों’ की व्याख्या समाजवाद की पृष्ठभूमि की तरह करे, तो ऐतिहासिक निरंतरता दिख सकती है। हां, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के मुखिया शी जिनपिंग कुओमिन्तांग के संस्थापक सन यात सेन की कही और लिखी बातों की खिल्ली जरूर उड़ाएंगे, लेकिन उसकी निंदा नहीं करेंगे। पहले जिस निरंतरता का उल्लेख किया गया था, वह तब थी, जब माओ के समय के बाद, देंग शियाओ पिंग ने कहा था, ‘‘आम तौर पर, हमारा मानना था कि हमने, जो रास्ता चुना है, जिसे हम चीनी खासियत का समाजवाद कहते हैं, वह सही है।’’ इस तरह उन्होंने चीन की सदियों पुरानी बहस में अपना एक नया अध्याय जोड़ा कि कैसे आर्थिक गति बनाए रखी जाए और विदेशियों से मिली हार से उबरकर हारी हुई जमीन छीन ली जाए।
चीन के लिए पूंजीवाद का मतलब निजी स्वामित्व, मुक्त बाजार आर्थिक व्यवस्था और अर्जित पूंजी के मुताबिक धन का वितरण है। बतौर राजनेता, शी जिनपिंग को देश को उच्च उत्पादक शक्तियों के निर्माण, सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी दूर करने, ग्रामीण-शहरी अंतर पाटने और लोगों का जीवन सहज-सुलभ बनाने की ओर ले जाना है।
महामारी के वर्षों (2019-2022) ने चीन को आर्थिक संकट में डाल दिया है, जो अभी भी जारी है। शी जिनपिंग के लिए जरूरी है कि तियानजिन में एससीओ के बहुपक्षीय स्वरूप, तार्किक नीतिगत नतीजों का निरंतर प्रवाह हो, न कि एकतरफा फैसले हों।
शंघाई सहयोग संगठन में रूस का जोर पश्चिम के लगाए आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों पर ही रहना है। मास्को के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध के बहाने रूस को अलग-थलग करने की कोशिश में कॉर्पोरेट लालच है, जिसे दुनिया में लोकतंत्र के कथित पहरुए यानी अमेरिका से शह मिल रही है। रूस के मुताबिक, यह कथित स्वतंत्रता, स्वाधीनता और न्याय के नाम पर कॉर्पोरेट लाभ के लिए रूस को तोड़ने की नई साजिश है।
इस तरह एससीओ बैठक में यूक्रेन पर चिंताएं बंद दरवाजों के पीछे व्यक्त की जाएंगी। रूस के लिए यूक्रेन, खासकर कीव उसकी ऐतिहासिक सभ्यतागत निरंतरता के लिए आवश्यक है। 1325 से मास्को में पूर्वी रूढ़िवादी चर्च पहले कीव में था, जो कीवियन रूस का केंद्र था। तीन शताब्दियों से भी अधिक समय बाद, 1686 में, कॉन्स्टेंटिनोपल के अधिपति ने कीव को मास्को के हवाले कर दिया। मास्को के लिए, पश्चिम का पाखंड इस बात में दिखाई देता है कि यूक्रेन उन देशों से रक्षा सामग्री प्राप्त कर रहा है जो हर समय शांति का दावा करते हैं, जबकि अन्य जगहों पर अत्याचारों को अनदेखा कर रहे हैं। मसलन, गाजा, सूडान और म्यांमार। एससीओ की यह बैठक यह दर्शाएगी कि कैसे प्रमुख आर्थिक शक्ति अमेरिका, एक दशक के भीतर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की संभावना का सामना करने से असहज है। पुतिन के लिए, चीन के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों की पुनः पुष्टि यह तय करती है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी।
अमेरिका के भारी टैरिफ निशाने पर इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ में मौजूदगी बहुध्रुवीय दुनिया के रास्ते की ओर बढ़ने का संकेत है। शंघाई सहयोग संगठन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी 2025 में तीन अरब लोगों (चीन और रूस सहित) की आवाज है, जिसके हर देश अपने-अपने आर्थिक एजेंडे पर चलना चाहते हैं। यहां आर्थिक और राजनैतिक-रणनीतिक संबंधों को अलग करना आवश्यक है। नई दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को विविध आर्थिक क्षेत्रों में संबंध स्थापित करके एक-दूसरे के साथ व्यापार करने में अधिक सहज होंगे। अगर यूरेशिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के लिए एक साझा मुद्रा पर बातचीत शुरू करने पर सहमत होती हैं, तो यह अमेरिकी डॉलर के विकल्प के लिए ब्रिक्स के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा, एक ऐसी मुद्रा जिसे ब्रेटन वुड्स ने बाजार मूल्यों के अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक रूपांतरण के लिए आदर्श मुद्रा के रूप में सुझाया था।
दरअसल अमेरिकी डॉलर से जुड़ाव 1971 में ही समाप्त हो गया, हालांकि यह एक संदर्भ बिंदु के रूप में जारी रहा, जिसके लिए अत्यंत आवश्यक सुधार की आवश्यकता थी। ट्रम्प इसका विरोध करते हैं, और उन्होंने कहा है कि वे ब्रिक्स को समाप्त कर देंगे। क्या एससीओ 2025 आर्थिक एजेंडे को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा, जो यूरेशिया क्षेत्र को बेकाबू धमकियों से मुक्त कर सके, जिसमें राजनीतिक-रणनीतिक कारक ही एकमात्र निर्धारक हो? आर्थिक स्थिरता पहली शर्त होनी चाहिए, जिसमें संबंधित घरेलू आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाया जाए, न कि उन्हें निर्देशित किया जाए।
भारत स्वीकृत व्यापार मूल्यों में बराबरी के लिए वित्तीय सेवा प्रदान करने का एक प्रमुख मॉडल हो सकता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार (1875) होने के नाते, मुंबई वह स्थान हो सकता है, जहां व्यापार-संबंधी वित्तीय गतिशीलता, मुद्रीकरण और संसाधन जुटाने में लचीलेपन पर विचार किया जाना चाहिए। भारत को दसों सदस्यों को सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हुए एक बयान जारी करने के लिए चतुराई से राजी करना होगा। इस अंतर-सरकारी मंच के सदस्य के रूप में पाकिस्तान आपत्तियां उठाएगा, लेकिन उससे हमारे आर्थिक एजेंडे को पटरी से नहीं उतारना चाहिए और राजनैतिक मुद्दों को अलग रखना चाहिए, ईरान जैसे सदस्यों के साथ भेदभाव न करके समूह की आर्थिक पहचान को मजबूत करना चाहिए। अभी एक कठिन निर्णय लिया जाना बाकी है, भारत की विदेश नीति को शब्दों से परे, ऐसी आर्थिक ताकत का उदाहरण पेश करके पूरब की ओर चलने की नीति पर काम करना होगा, प्रस्तुत करते हुए, जो ट्रम्प के भड़काऊ बयानों से घिरा न हो। एससीओ बैठक को बहुत ही बारीकी से यह संदेश देना होगा कि यूरेशियाई बाजार में इसकी उपस्थिति और कार्यप्रणाली पहले से दस गुना बड़ी है।

(चीन और ताइवान के संबंधों के जानकार, विचार निजी हैं)