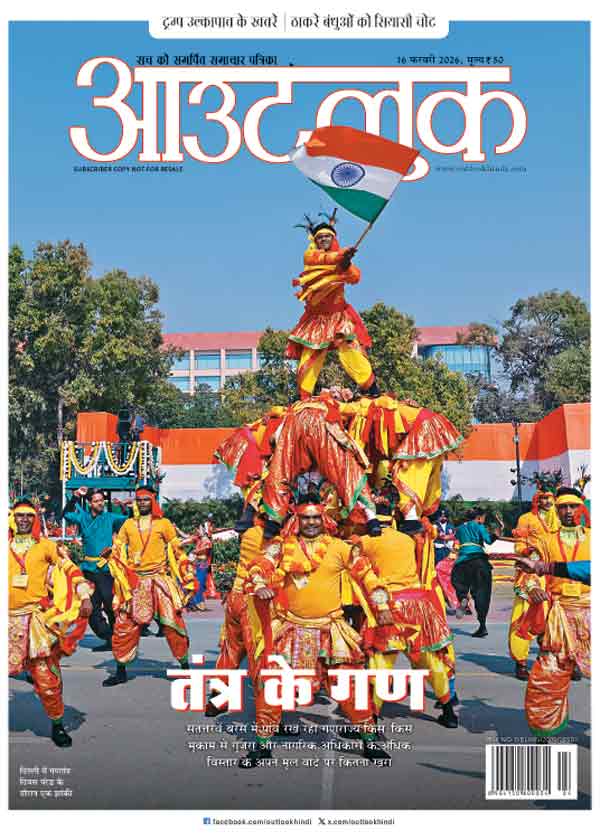हाल ही में 21 नवंबर को उर्दू की मशहूर कवयित्री फहमीदा रियाज़ का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसी के साथ जुल्म का शिकार होने वाले सभी इनसानों, खास तौर पर स्त्रियों के पक्ष में उठने वाली एक जोरदार आवाज खामोश हो गई। कहने को तो वे पाकिस्तान की थीं, लेकिन हकीकत में वे उतनी ही भारत की और शेष विश्व की थीं। मानवीय मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि और दबे-कुचले इनसानों के प्रति हमदर्दी से भरा उनका पूरा जीवन एक विद्रोही का जीवन था जो किसी भी क्षेत्र में अन्याय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, भले ही वह अन्याय सामाजिक-राजनीतिक जीवन में हो या फिर नितांत व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए उनका जीवन बंधनों को तोड़ने के दुर्दम्य साहस की ऐसी प्रेरक गाथा है जिसे लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनकी गाथा को दोहराती रहेंगी।
फहमीदा रियाज़ का परिवार उत्तर प्रदेश के मेरठ का सुशिक्षित और साहित्यिक रुचि से संपन्न परिवार था। लेकिन उनकी परवरिश हैदराबाद (सिंध) में हुई क्योंकि 1930 में उनके पिता ने वहां अध्यापक की नौकरी कर ली थी। मई 2014 में एक बार फहमीदा रियाज़ ने एक बातचीत के दौरान मुझे बताया था कि उनके पिता फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार थे और उनके घर में खूब किताबें थीं। लेकिन जब वे छोटी थीं, शायद पांच साल की, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन के पति संभालते थे, जो सिंधी थे। इसलिए घर में उर्दू और सिंधी दोनों भाषाएं बोली जाती थीं। बचपन में ही फहमीदा ने तुकबंदी करना शुरू कर दिया था। शायद वे तुकें मिला-मिलाकर बोलने लगी थीं, क्योंकि उनकी अम्मी ने काफी बाद में उन्हें उनके पिता की हस्तलिपि में उनकी कुछ तुकबंदियां दिखाईं और बताया कि जब वे इस तरह की काव्यात्मक पंक्तियां बोलती थीं तो उनके अब्बा उन्हें कागज पर उतार लिया करते थे। समय के साथ-साथ उनकी साहित्यिक अभिरुचि परिष्कृत और विकसित होती गई और 1967 में उनका पहला काव्य संग्रह पत्थर की जुबां प्रकाशित हुआ।
वह क्या बात है जो किसी व्यक्ति के भीतर की रचनात्मकता को जगाती है या यूं कहें उसमें कुछ नया रचने की प्रतिभा का ताला खोलती है। फहमीदा का मानना था कि शायरी का ताला प्रेम की कुंजी से ही खुलता है। अपनी बेबाक शायरी के लिए विख्यात फहमीदा रियाज़ ने मुक्त भाव से बताया था, “जब कोई लड़का या लड़की जवान होते हैं, तो उनके अंदर जो क्रेविंग होती है, जो चाहत होती है, दूसरे शख्स के लिए, उसी से क्रिएटिविटी का ताला खुलता है। हालांकि बचपन से ही तुकबंदी करती थी लेकिन जब लड़कों में दिलचस्पी बढ़ी, तब शायरी का भी आगाज (प्रारंभ) हुआ।” 1960 के दशक में उनकी शायरी की विधिवत शुरुआत हुई। यह समय फील्ड मार्शल अयूब खां की तानाशाही हुकूमत का था। राजनीतिक पाबंदियों के अलावा वैचारिक पाबंदियां भी लागू थीं और वामपंथी साहित्य का मिलना बड़ा मुश्किल था। मैक्सिम गोर्की का कालजयी उपन्यास मां और उस जैसी अन्य पुस्तकें दुर्लभ थीं। लेकिन फिर उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की और तब वामपंथी साहित्य भी मिलने लगा। फहमीदा रियाज़ इसी दौर में मार्क्सवादी बनीं। 1967 में उनका पहला काव्य संग्रह आया। इसमें लगभग सभी नज्में प्रेम के अनुभव से संबंधित थीं। यह भी एक विचित्र बात है कि फहमीदा रियाज़ की तबीयत कभी गजल की तरफ नहीं गई और उन्होंने नज्म का ही रियाज किया। इसी साल उनकी शादी कर दी गई। पति ब्रिटेन में काम करते थे, सो शादी के सोलह दिन बाद फहमीदा भी उनके साथ लंदन चली गईं। पाकिस्तान में वे रेडियो में काम करती थीं, इसलिए लंदन में उन्हें बीबीसी में काम करने का अवसर मिला।
फहमीदा ने सिंध में देखा था कि कैसे सिंधी भाषा को उर्दू की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया। इसलिए जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला के साथ यही हुआ और फिर पाकिस्तानी सेना ने वहां व्यापक पैमाने पर नरसंहार करना शुरू किया तो उनका दिल रो दिया। कई बार बीबीसी पर खबरें पढ़ते-पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया और उनके अपने जीवन का हाल, दोनों ही एक समान्तर आख्यान रच रहे थे। दरअसल उनकी शादी बेमेल थी। हालांकि उनकी एक संतान हुई लेकिन वे दिल से कभी अपने पति को न चाह सकीं। बिना चाहत के किसी मर्द को अपना बदन सौंपने की इस यातना की कोख से उनके दूसरे काव्य संग्रह बदन दरीदा (चिथड़ा शरीर) की रचनाओं ने जन्म लिया। इन कविताओं में उन्होंने बहुत साफगोई और बेबाकी के साथ अपने अनुभवों को व्यक्त किया था। इस संग्रह के आने के बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई और उन्हें “फ्रिजिड”, “अश्लील” और “दुश्चरित्र” होने के आरोपों को भी झेलना पड़ा। फहमीदा का कहना था, “मैंने औरत के वक्ष के लिए ‘पिस्तान’ शब्द का प्रयोग किया जिसे लोगों ने अश्लील समझा। कम्युनिस्ट भी मुझे कहते थे कि मैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हूं और मुझे किसी और तरह से लिखना चाहिए। लेकिन मैंने कभी अपना अंदाज नहीं बदला।” इस शादी को टूटना ही था और वह टूट गई। बाद में उनकी एक ट्रेड यूनियन नेता के साथ शादी हुई जो बहुत सफल रही।
इसके बाद तो उनकी साहित्यिक यात्रा ने भी कई मंजिलों को पार किया और धीरे-धीरे वह दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण कवयित्रियों में शुमार की जाने लगीं। यूं उन्होंने उपन्यास भी लिखे लेकिन उनकी छवि मूलतः एक शायरा की ही बनी रही। हिंदी में कराची शीर्षक से उनका उपन्यास वाणी प्रकाशन ने छापा। वाणी प्रकाशन ने ही उनका काव्य संग्रह कतरा-कतरा और उपन्यास जिंदा बहार प्रकाशित किए। कतरा-कतरा में ही उनकी वह नज्म भी शामिल है जिसे उनके निधन के बाद भारत में सबसे अधिक याद और उद्धृत किया गया। इस नज्म का शीर्षक है, नया भारत। फहमीदा ने इस नज्म में व्यंग्यात्मक अंदाज में भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास से कोई सबक न लेते हुए ठीक उस जैसा ही ‘घामड़’, ‘मूर्ख’, ‘धार्मिक कट्टर’ और ‘पीछे की ओर चलने वाला’ बनने की ठान ली है। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दो अलग कौम नहीं हैं। इस तरह व्यंग्य के जरिए फहमीदा ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की भी बुनियाद खोद डाली। यहां कुछ पंक्तियां उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा, “तुम बिलकुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई? वो मूरखता, वो घामड़पन, जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, बहुत बधाई।” पूरी नज्म में पाकिस्तान और पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच बन रहे दृश्यों को दिखा कर फहमीदा रियाज़ ने भारतवासियों को आगाह करने की कोशिश की है कि वे उस रास्ते को न अपनाएं जिस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान ने अपना सत्यानाश किया है। उन्होंने मुझसे कहा था, “लगभग आधी आबादी को वहां गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया है।” इस्लामी राज के हश्र से कोई सबक न लेते हुए अब भारत में हिंदू राज कायम करने की कोशिश हो रही है, जिस पर दुख और चिंता प्रकट करने के लिए फहमीदा ने व्यंग्य का सहारा लिया। लेकिन कट्टर सोच वाले लोगों को व्यंग्य भी समझ में नहीं आता। 1996 में लिखी इस नज्म को जब 29 अप्रैल, 2000 को फहमीदा रियाज़ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित एक हिंद-पाक मुशायरे में पढ़ना शुरू किया तो भारतीय सेना के दो अधिकारियों ने उन पर पिस्तौल तान दी थी।
फहमीदा रियाज़ ने पाकिस्तान में जनरल जिया-उल-हक की सैनिक तानाशाही का विरोध किया था और दिल्ली में आत्म-निर्वासन के कई बरस गुजारे थे। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से प्रेम करती थीं इसलिए उनके यहां ‘मेघदूत’ और ‘भरतनाट्यम’ शीर्षक से भी कविताएं मिल जाती हैं और ‘कार्ल मार्क्स’ जैसी कविताएं भी।
उनका वामपंथी चिंतन उन्हें समाज के वंचित तबकों का साथ देना सिखाता था और जीवन भर उन्होंने इस सीख को नहीं भुलाया। उनका उपन्यास जिंदा बहार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को समेटे हुए है क्योंकि ये तीन देश कभी एक ही थे। इन देशों के समाज और संस्कृति के ताने-बाने एक-दूसरे के साथ इतने संश्लिष्ट ढंग से गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग असंभव है।
आश्चर्य नहीं कि उनकी भाषा हमें मीर तकी ‘मीर’ और ‘फिराक गोरखपुरी’ की परंपरा की याद दिलाती है-
“देखो तो सुहागन के मुखड़े की दमक
अपने प्रीतम की आंख का तारा है
जीवन-खेती को सींचती जाएगी
अमृत की नदी का रस भरी धारा है।”
फहमीदा रियाज़ की कृतियों में भी अमृत की नदी की रस-धार बहती है जो साहित्य प्रेमियों को लंबे समय तक रससिक्त करती रहेगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और कला-संस्कृति पर लिखते हैं)