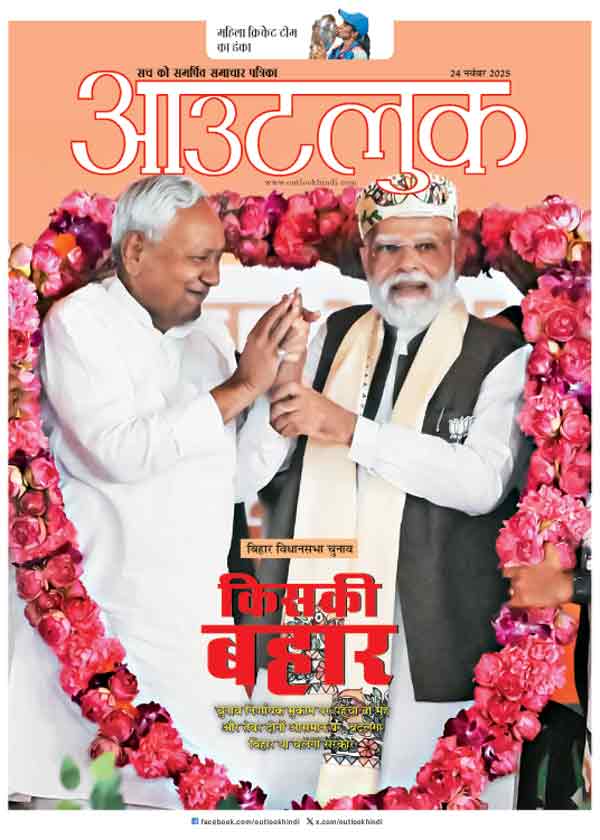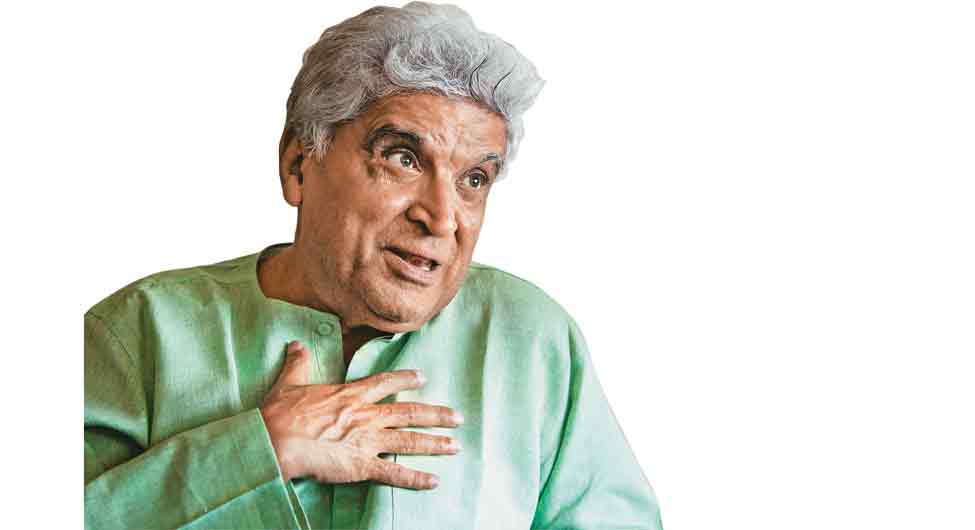एक जमाने में जल-जमाव की समस्या छोटे शहरों की त्रासदी समझी जाती थी। साल दर साल मानसून के दौरान और उसके कई हफ्तों बाद भी उससे जुड़ी समस्याओं से जूझना वहां के बाशिंदों की नियति बन गई थी। अब भी कुछ बदला नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में अंधाधुंध शहरीकरण के कारण आज स्थिति और भयावह हो गई। हालांकि जलजमाव की समस्या अब सिर्फ छोटे शहरों तक नहीं रही। एक वक्त था जब महानगरों में यह समस्या नहीं थी। उस दौर में आम तौर पर समझा जाता था कि बाढ़ और जल-जमाव सिर्फ बिहार और असम जैसे कथित पिछड़े राज्यों को ही हर साल बेहाल करते हैं, बड़े और विकसित प्रदेश के नगर इससे अछूते रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि वहां नागरिक सुविधाओं और शहरी विकास की बेहतर व्यवस्था होती है। हालांकि हाल की तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि कम से कम इस मामले में बड़े और छोटे शहरों की दूरियां मिट गईं हैं।
पिछले कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में जल-जमाव की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। हर साल मानसून से पहले वहां शहरी निकायों के अधिकारी जलनिकासी के पुख्ता इंतजाम करने के दावे करते हैं, जो कुछ मिनटों की बारिश में खोखले साबित होते हैं। आज हर बड़े नगर में जल-जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हाल की बारिश ने जैसा कहर बरपाया, वह अप्रत्याशित था। लंबी कतारों में गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रही।
गौरतलब है कि गुरुग्राम कि ख्याति अति आधुनिक नगर के रूप में है, जिसे ‘मिलेनियम सिटी’ कहा जाता है। वहां तमाम आधुनिक सुख-सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन एक ही तेज बारिश में इसके अति आधुनिक होने की कलई खुल गई। इस महानगर में भले ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुमंजिला दफ्तर हों, महंगे रिहायशी इलाके हों, शानदार शॉपिंग मॉल हों, साइबर सिटी हो लेकिन जल-जमाव के मामले में उसे भी वैसी ही समस्याओं से जूझना पड़ा, जो कभी सिर्फ छोटे शहर में बसे लोगों के किस्मत में बदा था।
अस्सी के दशक में मुंबई के जुहू और विले-पार्ले जैसे रिहायशी इलाकों में जब जल-जमाव हुआ तब पहली बार एहसास हुआ कि वहां के ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक दुरुस्त करने की दरकार है। देश के सबसे संपन्न शहरी निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उसके बाद इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास किए। लेकिन आज भी वहां कई इलाकों में बारिश के बाद लंबे समय तक जल-जमाव रहता है। यही कहानी कमोबेश मैदानी इलाकों के सभी बड़े शहरों की है।
इसके लिए क्या सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या ऐसी समस्याएं मानव निर्मित हैं? पिछले कुछ वर्षों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि या बादल फटने की घटनाओं में दुनिया भर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका मूल कारण प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। शहरीकरण के प्रति दीवानगी में पेड़ बेरहमी से काटे जा रहे हैं और पहाड़ों को काटकर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानियों की यात्रा बेहतर बनाई जा सके। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था किए बगैर नए कस्बे और शहर बेतरतीब तरीके से बसाए जा रहे हैं। इन सबका प्रतिकूल असर पर्यावरण और आम जीवन पर पड़ना लाजिमी है।
जल-जमाव बड़े शहरों की इकलौती बड़ी समस्या नहीं है। वहां उपलब्ध संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का जबरदस्त दवाब है। आजादी के बाद से ही गांवों में जीवनयापन के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से बड़े पैमाने पर महानगरों की ओर लोगों ने कूच करना शुरू किया, जहां बड़े उद्योग लगाए गए। वहां सभी जरूरी सुविधाएं और संसाधन मौजूद थे। वहां से तैयार माल देश के बाकी हिस्सों में भेजना आसान था। इस वजह से उद्योग का विकास महानगरों के इर्दगिर्द ही हुआ। इसी कारण भारी संख्या में कामगारों के आने से वहां की व्यवस्था पर दवाब बढ़ा। आज भी लाखों लोग रोजगार की तलाश में महानगरों का ही रुख करते हैं। बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के कारण नगर निगमों और अन्य शहरी निकायों के लिए यह मुमकिन नहीं दिखता कि बदलते समय की जरूरतों के अनुसार आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाया जाए, ताकि किसी भी समस्या के समाधान की तैयारी रखी जाए। हाल के वर्षों में देश में ‘स्मार्ट सिटी’ बनाए जाने का प्रयास किया गया लेकिन वैसे परिणाम देखने को नहीं मिले जिसकी उम्मीद थी। गुरुग्राम के हालत देख कर तो कम से कम ऐसा ही लगता है।
जाहिर है, इन समस्याओं के स्थायी समाधान के बारे में नीति-निर्माताओं को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर प्रकृति से लंबे समय तक खिलवाड़ होगा तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करने लगेगी, जिसका खमियाजा बड़े और छोटे दोनों शहरों के लोगों को भरना पड़ेगा।