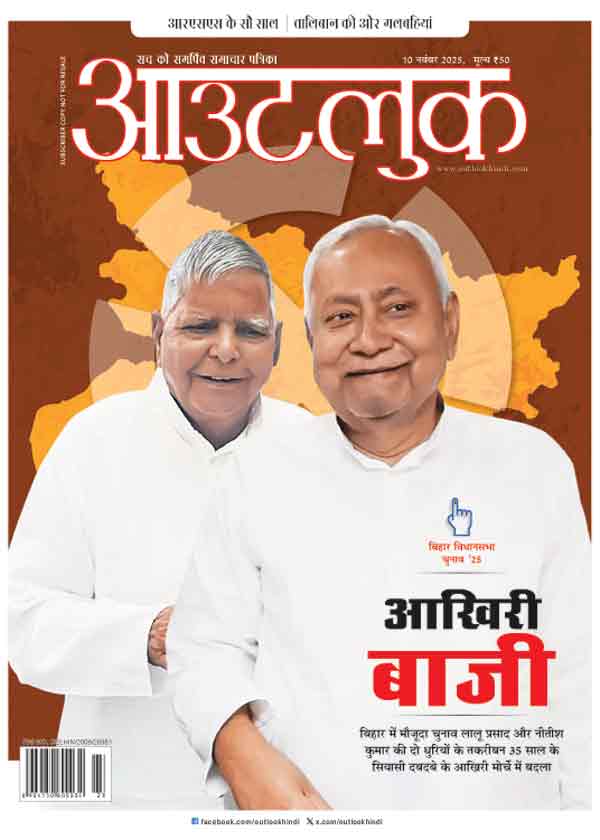किसी जीवित या मृत व्यक्ति की जीवनी या ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनाना दोधारी तलवार पर चलने जैसा है, खासकर उस देश में जहां भावनाएं बेतुकी बातों पर भी आहत हो जाती हैं। न सिर्फ किरदारों के चित्रण या किसी संवाद पर बल्कि फिल्म के नाम पर भी तलवारें म्यान से निकल आती हैं। देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और कभी-कभी उसे बनाने वाले की ‘गुस्ताखी’ पर नाराज लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इसके बावजूद भारतीय फिल्मकार, विशेषकर बॉलीवुड ब्रिगेड बॉयोपिक बनाने से तौबा नहीं करता। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, निर्माताओं को बैठे-बिठाए एक अच्छी कहानी मिल जाती है, जिसमें लोगों की पहले से दिलचस्पी होती है। दूसरा, दर्शकों की उत्सुकता की वजह से फिल्म प्रदर्शन के शुरुआती दिनों में अच्छा व्यवसाय करने की क्षमता रखती है।
लेकिन, बॉलीवुड के बॉयोपिक के प्रति मोह से जुड़ी एक समस्या भी है। यहां किसी शख्सियत या घटनाक्रम का ईमानदार सिनेमाई रूपांतरण बिरले ही होता है। यहां फिल्मों में तथ्यों के साथ खिलवाड़ को रचनात्मक अपराध नहीं समझा जाता। अगर जेम्स बांड को पाश्चात्य फिल्मों में कत्ल करने का लाइसेंस मिला है तो भारतीय फिल्मकारों को किसी भी स्क्रिप्ट में हर उस मसाले का तड़का लगाने का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसकी खुशबू दर्शकों को थिएटर तक खींच सके। मुख्य पात्रों के व्यक्तित्व के स्याह पक्ष की ऐसी लीपापोती की जाती है कि वह सर्वगुणसंपन्न इंसान नजर आए। वह करिश्माई नायकों की तरह परदे पर कोई भी हैरतअंगेज करतब कर सकता है। शेक्सपियर के ट्रैजिक हीरो की तरह उसके चरित्र में कोई बड़ी खामी नजर नहीं आती।
मसाला फिल्मों के लिए तो यह स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन किसी बॉयोपिक या सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में यह अक्षम्य-सा गुनाह लगता है। वैसे बॉलीवुड के अपने कायदे-कानून हैं। यह संभवत: इकलौती इंडस्ट्री है, जहां पोस्टर पर तो ऐसी फिल्मों के ‘सच्ची घटना से प्रेरित’ होने का दावा किया जाता है लेकिन हकीकत में, उसी फिल्म की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि सारे चरित्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका किसी जीवित या मृत से कोई लेना-देना नहीं है। अगर कुछ दृश्य मिलते भी हैं तो उसे संयोग मात्र समझा जाए। यानी चित भी उनकी और पट भी! इसलिए बॉयोपिक का हूटर बजाकर दर्शकों को टिकट खिड़कियों की ओर लुभाने से परहेज नहीं किया जाता और कोई चाहा-अनचाहा विवाद खड़ा होता है तो सब कुछ काल्पनिक बता कर पल्ला झाड़ने में भी देर नहीं की जाती। ऐसी फिल्मों को चुपके से काल्पनिक घोषित करने से बॉयोपिक निर्माताओं को सेंसर बोर्ड की कैंची से बचने का रास्ता भी मिल जाता है।
इन तमाम तरकीबों और चालाकियों के बावजूद अधिकतर बॉयोपिक पर विवाद होते ही रहते हैं, चाहे वह बाजीराव-मस्तानी की ऐतिहासिक प्रेम कहानी हो या आज के दौर की एयर फोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट गुंजन सक्सेना की जीवनी। कभी-कभी तो लगता है कि निर्माता जानबूझकर अपनी ही फिल्मों पर विवाद खड़ा करने का हथकंडा अपनाते हैं। अक्सर विवादों के कारण लचर कथा-पटकथा वाली कमजोर फिल्म भी अच्छा व्यवसाय कर लेती है। विवाद से तिजोरी भरती है तो दाग की तरह विवाद भी अच्छे हैं!
हाल में प्रदर्शित अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पृथ्वीराज (विवादों के कारण अंतिम समय में जिसका शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज किया गया) पर भी आरोप लग रहे हैं कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखने का साहस जुटाया है, उनका कहना है कि उसके कई दृश्य इतिहास में दर्ज विवरणों से मेल नहीं खाते। पूर्व में भी पद्मावत जैसी फिल्मों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। क्या ऐतिहासिक तथ्यों को सिनेमाई स्वतंत्रता की नाम पर बेरहमी से तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है? फिल्मकारों की मानें तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। उनके अनुसार, सिनेमा विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्टबुक का अक्षरश: रूपांतरण नहीं होता और व्यावसायिक या कलात्मक वजहों से कथा-पटकथा में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं। उनका तर्क है कि अगर यशराज फिल्म्स के नए शाहकार में अंधे किए जाने के बाद सम्राट पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी को मारने के बजाय स्वयं एक विदेशी आक्रांता के हाथों शहीद होते तो क्या इस फिल्म को उतने दर्शक भी मिलते, जितना उसे तमाम जतन करने के बाद मिले?
यह सही है कि फीचर फिल्मों का व्याकरण वृत्त-चित्र से भिन्न होता है और सिनेमाई आजादी से किसी फिल्मकार को वंचित नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें यह अधिकार कतई नहीं कि वे सच की आड़ में झूठ का मुलम्मा पेश करें। जैसे हर सिगरेट के पैकेट पर एक वैधानिक चेतावनी होती है, वैसे ही क्या सेंसर बोर्ड को सिनेमा के प्रचार-प्रसार के हर माध्यम में यह प्रमुखता से सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्शक भ्रामक पब्लिसिटी के कारण परदे पर दिखाए गए दृश्यों को सत्य न समझ बैठें और फिल्म को महज फिल्म की तरह ही देखें, इतिहास के आईने के रूप में नहीं? जरा सोचिए!