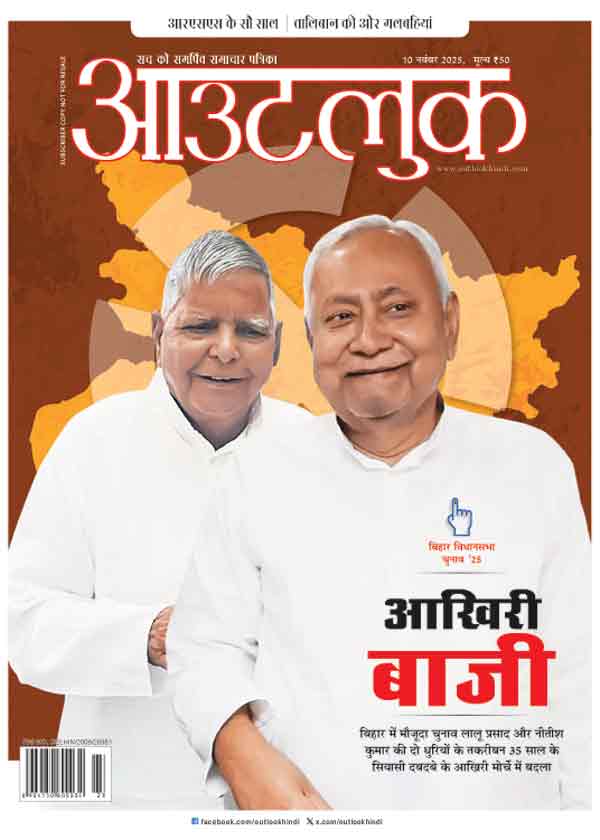अगस्त की हवा और पंद्रह तारीख कई यादें जगाती हैं। इनमें से कुछ यादें बीते हुए वक्त की हैं, पर कई को सपनों के संस्मरण की संज्ञा दी जा सकती है। आजादी सिर्फ एक घटना नहीं थी, जिसे इतिहास में दर्ज कर देना पर्याप्त हो। वह एक लंबी वैचारिक खलबली भी थी। उस खलबली में अनेक नई परिभाषाएं गढ़ी जाने के करीब पहुंचीं। संविधान ने उन्हें सूत्र रूप में व्यक्त किया। लोकतंत्र की साधना का एक बड़ा अर्थ इन सूत्रों को खोलना और फैलाना था। सबसे गहन सूत्र संविधान की भूमिका और तीसरे भाग में दर्ज थे। भूमिका में दिए गए मूल्य और आदर्श तथा तीसरे भाग में प्रस्तुत अधिकार उस व्यक्ति की तसवीर बनाते थे, जो आजाद भारत का सामान्य नागरिक होगा। उस व्यक्ति की वैचारिक सेहत और ताकत तथा हैसियत से मिलकर देश की स्वतंत्रता को जांचने-मापने का पैमाना बनता है जिसे इस्तेमाल करने की गंभीर जरूरत आज महसूस होती है।
संविधान-सभा में हुई तमाम बहसें सरकार और आम जन के रिश्तों को एक नए वैचारिक धरातल पर लाने में कामयाब हुईं, इसमें शक नहीं। फिर भी यह एक शुरुआत भर थी। उस शुरुआत को आगे बढ़ाने का काम आज भी जारी है। उस काम को जारी रखने और विस्तार देने में सबसे बड़ी भूमिका उच्चतम न्यायालय ने निभाई है। गौतम भाटिया, जो सुप्रीम कोर्ट के युवा तकील हैं, अपनी ताजा पुस्तक में न्यायालय की इस ऐतिहासिक भूमिका को एक धीमे युगान्तर की तरह देखते हैं। कई दशकों में घटे इस सूक्ष्म युगान्तरण को गौतम भाटिया ने नौ बड़े मुकदमों की छानबीन करके समझा है। यह एक रोमांचक शोध है जो हमें एहसास दिलाता है कि स्वाधीन हो चुके देश में स्वाधीन व्यक्ति की रचना और जिंदगी को संभव बनाना कितना बौद्धिक और सामाजिक परिश्रम मांगता है। इस परिश्रम में 21वें अनुच्छेद की विवेचना ने सबसे बड़ी और संगीन चुनौतियां पेश की हैं। इस अनुच्छेद का विषय है जीवन का अधिकार।
सुनने में यह अधिकार बड़ा सामान्य या मामूली लगता है पर जब हम इसे अन्य बुनियादी अधिकारों के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, तभी इसकी जटिलता उभरती है। सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए मुकदमों में यही हुआ है। इन मुकदमों में हुई बहसों के जरिए धीरे-धीरे यह बात उजागर होती चली गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन केवल जान की दृष्टि से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन को एक अधिकार की तरह देखने का अर्थ उन मूल्यों के संदर्भ में प्रकट होता है जो संविधान के ढांचे और शब्दों में निहित हैं। समता, न्याय, भाईचारा जैसे सामाजिक आदर्श मिलकर स्वतंत्रता या ‘लिबर्टी’ को रूपायित करते हैं।
हिंदी में आमतौर पर अंग्रेजी के ‘फ्रीडम’ और ‘लिबर्टी’ शब्दों को समानार्थी मान लिया जाता है। इसी तरह की आदत ‘स्वतंत्रता’, ‘स्वाधीनता’, ‘आजादी’ और यहां तक कि ‘स्वराज’ को समानार्थी मानने में दिखाई देती है। मूल अंग्रेजी के संविधान और उसके शासकीय हिंदी अनुवाद में यह समस्या मौजूद है।
आज जब हमारे सामाजिक माहौल में संविधान कई प्रसंगों में बेगाना और विस्मृत प्रतीत होता है, ‘फ्रीडम’ और ‘लिबर्टी’ का अंतर समझना जरूरी है। देश अंग्रेजी राज से मुक्त हो गया, इस सफलता के बाद उसे स्वतंत्र या स्वाधीन अर्थात अपने अधीन होकर चलना था। इसी उद्देश्य की खातिर स्वाधीन भारत ने अपना राज्य और उसका तंत्र बनाया, जो संविधान में विस्तार से दर्ज है। राज्यतंत्र का विधान (यानी कानून) भारत में रहने वाले हर इंसान को आजादी देता है। यह वैधानिक मुक्ति ही ‘लिबर्टी’ है। जीवन का अधिकार देने वाले 21वें अनुच्छेद का शीर्षक हैः ‘प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऐंड पर्सनल लिबर्टी’। इस शीर्षक का शासकीय अनुवाद अनुच्छेद की भावना को स्पष्ट नहीं करता। ‘पर्सनल लिबर्टी’ ऐसे जीवन का हक देती है जो राज्य के कानूनों से संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले और कथन इस जीवन को चित्रित कर चुके हैं। इन फैसलों की रोशनी पिछले सात दशकों में इतनी बढ़ चुकी है कि अब किसी विचारधारा या संकट की आड़ में इनसान के जीवन को कानून से मिले संरक्षण को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती।
एक तरफ यह कानूनी संरक्षण बराबरी और सहनशीलता का कवच देता है, तो दूसरी तरफ गरिमा को जिंदगी का अनिवार्य तत्व बताता है। इतनी विशद तैयारी संविधान के बुनियादी मूल्यों और सामाजिक आदर्शों को चरितार्थ करने में निहित मुश्किलों का अंदाज देती है। संविधान सभा की बहसों से पता लगता है कि उसके सदस्य धर्म, भाषा, जीवन-शैली, आर्थिक विषमता और जाति-व्यवस्था में निहित उत्पीड़न और भेदभाव की ताकत को लेकर कितने आशंकित थे। संस्कृति के ताने-बाने में इस ताकत को लिंग, जाति और वर्ग की पारंपरिक विषमता के हवाले से अक्षुण्ण रखने की व्यवस्था थी। संविधान का ढांचा और तीसरे खंड में दिए गए मूलभूत अधिकार इसी व्यवस्था पर चोट करते हैं। इस वैधानिक चोट से पैदा होने वाली परिवर्तनकारी ऊर्जा पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती जाए, भारत की विविधता मजबूत होती जाए, यही संविधान का सपना है। आप इसे आजादी का सपना भी कह सकते हैं।
आज के समय में बार-बार घट रही कई घटनाएं यह संदेह पैदा करती हैं कि यह सपना कहीं सत्ता के नशे में डूब तो नहीं रहा है। ऐसा होता है तो सपने को संस्मरण बनने में देर नहीं लगेगी। अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता की समाप्ति का यह बहत्तरवां अगस्त है। रोज के अखबार में किसी निहत्थे नागरिक को भीड़ द्वारा मार डाले जाने, किसी बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या, किसी औरत के साथ कई पुरुषों द्वारा मिलकर बलात्कार किए जाने, पुलिस द्वारा झूठा मामला दर्ज किए जाने, नैराश्य से घिरे अन्याय के पीड़ित द्वारा आत्महत्या सरीखी खबरें कागज पर छपकर सुबह-सुबह करोड़ों नागरिकों की चेतना में प्रवेश करती हैं। शायद वे थोड़े-से लोगों को झकझोरती हैं, पर पाठकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी खबरों को सामान्य जीवन का अंग मान चुका है। यह स्थिति संविधान में वर्णित स्वाधीन भारत की कल्पना से मेल नहीं खाती, एक भटके हुए समाज का संकेत देती है। भटकाव के लक्षण अनेक हैं, उनकी व्यंजना एक है कि देश अपनी सयानी राजनैतिक और आर्थिक तैयारी का इस्तेमाल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नहीं कर पा रहा है।
ऐसा क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर बाराबंकी में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की ने दिया है। जिस अवसर पर उसकी आवाज दुनिया ने सुनी है, वह था बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चलाया गया एक जागरण अभियान। एक पुलिस अधिकारी इस अभियान की सभा में मौजूद थे। अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की कटिबद्धता का गीत गाया। इसके जवाब में इस छात्रा ने पूछा कि जब बलात्कारी सत्ता से जुड़ा हो तो पुलिस कैसी सुरक्षा देगी। उसने उन्नाव की घटना का दो-टूक शब्दों में हवाला दिया। जब वह बोल रही थी, सभा में बैठी लड़कियां बार-बार ताली बजाकर उसकी बात को बल दे रही थीं। हर बार ताली बजने पर इस छात्रा के चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान उभरती थी। इस मुस्कान के जरिए वह अपनी साथिनों को जताती थी कि वह अपने प्रश्नों का महत्व जानती है। क्षण भर के लिए उभरकर मुस्कान गायब हो जाती थी और चेहरा तीखे प्रश्नों की कठोरता व्यक्त करने लगता था। इन प्रश्नों ने आगंतुक पुलिस अधिकारी को स्तब्ध कर दिया। वे सिर्फ हेल्पलाइन का नंबर बोल सके।
इस प्रसंग को विस्तार देना और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का जिक्र इन दिनों चुप रहने की लाचारी के साथ किया जाता है। पत्रकारिता की दुनिया में मालिकों और सरकार के दबाव के कई प्रसंग बहुचर्चित हो चुके हैं। दमन, आतंक और हिंसा की घटनाएं घटी हैं। अखबारों में विचार की जगह सिकुड़ी है, कई कालेजों और विश्वविद्यालयों में खुली बहस करना संभव नहीं रहा। सोशल मीडिया में कोई स्वतंत्र विचार रखना कई तरह के जोखिम पैदा कर रहा है। इस चतुर्दिक, घेराव के बीच बाराबंकी की छात्रा का उन्मुक्त प्रश्न आश्वस्त करता है कि संविधान में दर्ज स्वतंत्रता शिक्षा के जरिए समाज में फैली है। शिक्षा का अपना संकट भले कितना गहरा हो, उसके प्रसार ने उच्चतम न्यायालय का साथ दिया है।
संभव है, यह आश्वस्ति सिर्फ सांत्वना हो। राजनैतिक छल और प्रशासनिक जड़ता के प्रहार सहते समाज में चेतना की मात्रा का सवाल बेमानी नहीं है। यह भी सही है कि चेतना की प्रखरता दो-चार युवा आवाजों से नहीं मापी जा सकती।
सावन-भादों के महीने बादलों और बारिश से आशा और आशंका के मेल से ऐसे-ऐसे मनोभाव जगाते हैं जिनका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल होता है। कभी लगता है, वह वैचारिक पूंजी जो आजादी के आंदोलन में इकट्ठा हुई थी, अभी चुकी नहीं है। कभी लगता है कि वह लोकतंत्र के कर्मकांड और राष्ट्रवाद की नारेबाजी में खर्च हो गई। शायद कोई एक आकलन या फैसला न उचित है, न पर्याप्त। विषमता तेजी से बढ़ रही है, विविधता पर भारी दबाव है, सत्य की विजय सदैव होकर रहती है, यह विश्वास भी तेजी से घटा है। संविधान में ढूंढे़ं या गांधी के महाप्रयास में, भारत की आजादी का स्वप्न बार-बार टूटता है तो उठकर बेचैनी महसूस होती है।
आजादी का एक और अर्थ था जो अंग्रेजी के ‘इंडिपेंडेंस’ शब्द में निहित है। यह शब्द याद दिलाता है कि अंग्रेजी राज का एक अर्थ निर्भरता भी था। गांधी का नेतृत्व इसी अर्थ से मुक्ति पर केंद्रित था। आत्मनिर्भरता, जिसका आदर्श गांधी ने गांव में पाया था, उनके ‘स्वराज’ की आत्मा थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गोद में खुशी से खेलता आज का भारत एक नया देश है जो गांधी के स्वराज को भूल चुका है। गांधी और संविधान ऐसे दो ही बिंदु थे जिन पर बनी राष्ट्रीय सहमति अभी तक आजादी को आधार दिए रही। सहमति के ये दोनों बिंदु आज की मनोदशा में कुछ खोए-से लगते हैं।
संविधान की भूमिका में चिह्नित आदर्शों में समता, भाईचारा और पंथनिरपेक्षता कई के मन में खुंदक पैदा कर रहे हैं। गांधी नहीं, उनके हत्यारे की प्रशंसा करके कोई चुनाव जीत सकता है। नए भारत की यह झलक कुछ अपरिचित-सी लगती है और अगस्त की उमस को बढ़ा रही है।
(लेखक प्रखर शिक्षाविद और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)