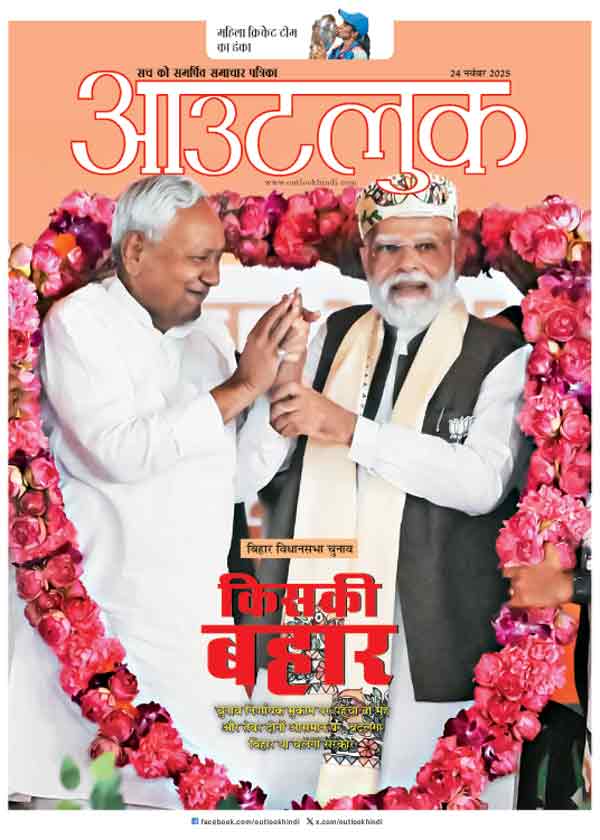पश्चिम बंगाल के मौजूदा चुनावों में जलपाईगुड़ी जिले में शीतलकुची में तपसिली समाज के मारे गए हिंदू-मुस्लिम राजबोंशी हों या नमोशुद्र मतुआ बिरादरी, दोनों ही अनुसूचित जातियां हैं और उनके वोट हासिल करने की हर ओर जद्दोजहद है। बंगाल में कहिए कि ये बिरादरियां अरसे से कांग्रेस या वाम मोर्चे या तृणमूल कांग्रेस के साथ रही हैं लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उनके कुछ वोट भाजपा की ओर झुके तो इस बार पार्टी उन्हें अपनी ओर करने की कोई जतन बाकी नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के दिन अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रसिद्ध मतुआ मंदिर के दर्शन को गए। शीतलकुची की घटना के बाद कई नेताओं के बयानों से भी लगता है कि राजबोंशी वोटों की जोड़-तोड़ की कोशिश है। बंगाल में अन्य अनूसूचित बिरादरियों के वोट हासिल करने के लिए इसी तरह पार्टियों का जोर है, जो राज्य की आबादी में लगभग 27 फीसदी की हिस्सेदारी रखती हैं।
अब आइए बंगाल से दूर उत्तर प्रदेश में, जहां इस 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक नया राग देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संविधान निर्माता की 130वीं वर्षगांठ के मौके पर दलित बस्तियों में जाकर “दलित दिवाली” मनाने और दलित मुद्दों को उठाने के लिए ‘बाबा साहेब वाहिनी’ के गठन का ऐलान किया। इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस और खासकर भाजपा से जुड़े दलित नेताओं की ओर से ही आई। उनकी दलील थी कि डॉ. आंबेडकर को सिर्फ दलित नायक बताना ठीक नहीं है।
दरअसल उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है, जहां पिछले तीन दशकों से दलित राजनीति सबसे मुखर रही है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का अपने दम पर सत्ता में पहुंचना उस राजनीति का अब तक चरम रहा है। लेकिन उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में खासकर मध्य उत्तर प्रदेश की कई दलित जातियों का रुझान कांग्रेस की ओर दिखा तो कांग्रेस को 22 सीटें हासिल हो गई थीं। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोटे तौर पर जाटवों को छोड़कर बाकी दलित जातियों का रुख भाजपा की ओर हुआ और वह अभी तक बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा-सपा गठजोड़ की एक वजह शायद यह भी रही कि मायावती भाजपा की ओर से इन जातियों को अपनी ओर लौटा लाना चाहती थीं। लेकिन चुनावी नतीजों से इस प्रयास में बड़ी सफलता नहीं दिखी। सो, अब बसपा और सपा दोनों अलग तरह की योजनाओं में जुटी हो सकती हैं। इस दौर में उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के एक और किरदार भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी उभरे हैं, जो आजाद समाज पार्टी बनाकर चुनावों में अपनी दखल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे तमाम राज्यों में दलित राजनीति का शिराजा बिखर-सा गया है, जहां आजादी के बाद के दशकों और खासकर 1980 के दशक में उसका बोलबाला शुरू हुआ था। उसकी गूंज उत्तर, पूरब, पश्चिम और मध्य भारत के लगभग हर राज्य में सुनाई देने लगी थी। तब कांग्रेस और भाजपा या जनता दल से टूटकर बनी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए दलित राजनीति करने वाली पार्टियों से तालमेल मजबूरी जैसी बन गई थी। लेकिन, आज महाराष्ट्र में रामदास आठवले या प्रकाश आंबेडकर की न वह अपील बची है, न उत्तर प्रदेश में मायावती की और बिहार में रामविलास पासवान के बाद न कोई ऐसा नेता दिखता है जिसकी दलितों में बड़ी अपील हो।
दलित आवाज बेशक सबसे अधिक मुखर होकर आजादी के आंदोलन के दौरान उठी, जब महानायक डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलित मुक्ति का आंदोलन छेड़ा। उससे अंग्रेजों ने चुनावी राजनीति में दलित जातियों को अलग कम्युनल अवार्ड देने की पेशकश की। महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार का आंदोलन छेड़ा और कम्युनल अवार्ड के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। उनके लंबे अनशन के बाद डॉ. आंबेडकर के साथ समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से चर्चित है। यही अनुसूचित जातियों-जनजातियों और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का आधार बना। डॉ. आंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। दक्षिण में अन्ना दुरै के नेतृत्व में ऐसा ही ब्राह्मणवाद विरोध आंदोलन जोर पकड़ गया था।
1956 में डॉ. आबेडकर की मृत्यु के बाद मोटे तौर पर यह राजनीति बिखर-सी गई। कांग्रेस में कुछ बड़े नामचीन नेता उभरे, जिनमें जगजीवन राम का नाम प्रमुख है। इंदिरा गांधी के दौर में तो कांग्रेस का मूल आधार ही ब्राह्मण, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक माने जाते थे। लेकिन 1970 के दशक में बिहार में बेलछी कांड एक तरह से नई दलित राजनीति के उभार का प्रतीक बना। वैसे, वह इंदिरा गांधी की सत्ता की वापसी का भी कारण बना, जो इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी से बुरी हार झेल चुकी थीं। इसी दशक में बिहार में रामविलास पासवान ने पहले दलित पैंथर बनाकर ऐलान किया कि वे दलितों के हर अत्याचार की जगह जाएंगे। महाराष्ट्र में रामदास आठवले, प्राकश आंबेडकर जैसे नेताओं की तूती बोलने लगी। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कांशीराम के नेतृत्व में पहले बामसेफ, फिर डीएस-4 के बैनर तले सभी दलित और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। बाद में यही बसपा के रूप में उभरा।
उस दशक में दलित सक्रियता कैसे आकार ले रही थी, उसका सबसे नायाब नमूना 1985 का उत्तर प्रदेश में बिजनौर का लोकसभा उपचुनाव है, जिसकी याद अब बहुत कम लोगों को होगी। वह चुनाव कांग्रेस के सांसद गिरधारी लाला के निधन के बाद हुआ था। कांग्रेस ने जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को खड़ा किया। उनके बरक्स जनता दल से पासवान थे। ये दोनों बिहार से थे। तीसरी उम्मीदवार मायावती थीं। बसपा तब शैशव काल में थी, इसलिए चुनाव चिन्ह तय नहीं था। मीरा कुमार महज 6,000 वोटों से जीतीं। तीसरे नंबर पर रहीं मायावती को 61,000 वोट मिले। पासवान और मायावती ने उत्तर प्रदेश में मीरा कुमार की हैसियत बता दी। लेकिन 1987 के हरिद्वार लोकसभा चुनाव में जीता तो कांग्रेस का उम्मीदवार मगर मायावती थोड़े अंतर से दूसरे नंबर पर रहीं और पासवान की जमानत जब्त हो गई। इस तरह पासवान की उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का सपना टूटा मगर बिहार में उन्होंने अपने लिए पक्की जगह कायम कर ली, जिसके बूते वे मृत्यु पर्यंत दो दशक तक लगातार केंद्र में मंत्री बने रहे।
उत्तर प्रदेश में कांशीराम सक्रिय थे। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में दलित और अति पिछड़ी जातियों की बस्तियों में सांझ ढलने के बाद उनकी बैठकें हुआ करती थीं। 1988 में इलाहाबाद लोकसभा के चर्चित उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बरक्स कांग्रेस के सुनील शास्त्री के साथ तीसरे उम्मीदवार कांशीराम भी थे। कांशीराम को करीब 90,000 वोट मिले थे। कांशीराम की कोशिशों ने जाटवों, वाल्मीकि, पासी, राजभर, बिंद, मल्लाह जैसी तमाम जातियों को जोड़ा। इसी आधार के बूते उनके शांत होने के बाद मायावती उत्तर प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में दलितों की एकछत्र नेता बनीं।
लेकिन दलित राजनीति और सामाजिक न्याय की यह धारा कैसे अब बिखरती दिख रही है, इसकी कहानी सिर्फ कांग्रेस या बाद में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में ही निहित नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार दलित नेताओं की सत्ता की चाह भी है। दलित राजनीति पर मजबूत दावा पेश करने वाले चंद्रशेखर आजाद की बातों में भी कुछ संकेत मिलता है। उन्होंने आउटलुक से कहा, “मायावती जी को अब किसी ऐसे युवा को कमान सौंपनी चाहिए, जो सीबीआइ और ईडी से न डरता हो।” इन नेताओं में पारिवारिक राजनीति को ही आगे बढ़ाने का ढर्रा शायद उनके प्रति मोहभंग पैदा कर रहा है। मायावती के साथ उनके भतीजे आनंद कुमार दूसरी कमान ही नहीं दिखते, बल्कि उनके रवैए से वाल्मीकि, पासी, राजभर, बिंद, मल्लाह जैसी जातियों के रसूख रखने वाले ज्यादातर नेता भाजपा की ओर और कुछ बाकी दलों में जा चुके हैं।
बिहार में पासवान के पुत्र चिराग को ही कमान नहीं मिली है, बल्कि उनके भाई और परिजनों को भी सत्ता-सुख हासिल है। दूसरे नेताओं में जीतनराम मांझी के भी पुत्र अब कमान संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के दलित नेताओं रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर की भी अपील ऐसी खो गई है कि वे भीमा कोरेगांव घटना में बंद बुद्धिजीवियों खासकर आनंद तेलतुमडे की गिरफ्तारी के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सके। तेलतुमडे की न सिर्फ बौद्धिक जगत में ख्याति है, बल्कि आंबेडकर परिवार के दामाद भी हैं।
बहरहाल, अप्रासंगिक दिखते दलित नेताओं के बावजूद दलित शख्सियतों के उभार और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की कामयाबी उम्मीद की किरण की तरह उभरती है। इनमें कुछ शख्सियतों का जिक्र इस अंक में है लेकिन ऐसे बहुत-से लोग हैं, जिनकी हम चर्चा नहीं कर पाए हैं या जो अनाम रहकर गंभीर काम कर रहे हैं। यही नहीं, दलित वोटों के लिए तमाम पार्टियों के बीच जो जद्दोजहद दिखती है, उससे भी नए दलित दौर के आगाज की किरण झिलमिला रही है।