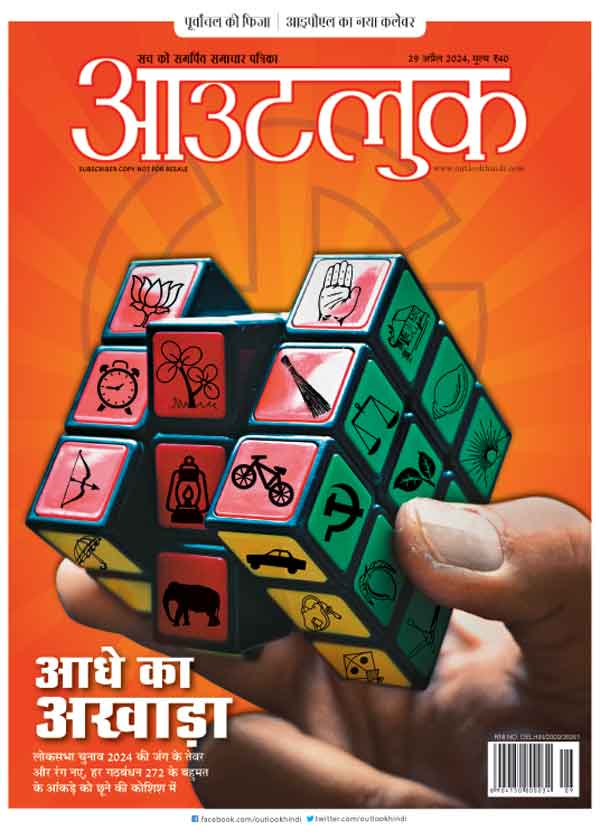गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर अचानक बहस के केंद्र में आ गए। यूं भी पिछले तीन दशकों के दौरान लगातार उनके जीवन और विचारों का महत्व बढ़ता गया है और उनसे प्रेरणा लेने वालों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सही है कि उनकी राजनीतिक एवं बौद्धिक भूमिका, अवदान और विरासत का विश्लेषण और आलोचनात्मक परीक्षण बहुत कम हुआ है और उनके दलित अनुयायी उन्हें लगभग भगवान बनाने की कोशिश में लगे हैं। हकीकत यह है कि गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य किसी भी नेता-विचारक की तरह आंबेडकर भी अपने समय और समाज की उपज थे। जरूरत उनकी राजनीतिक एवं वैचारिक विरासत में से तात्कालिक तत्वों को छांट कर अलग करने और सार्वकालिक तत्वों को अपनाने की है, अंधानुकरण की नहीं।
मसलन 27 सितंबर, 1951 को आंबेडकर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह कानून मंत्री थे लेकिन योजना मंत्रालय चाहते थे। इस्तीफे के बारे में संसद में बयान देने के बजाय उन्होंने अखबारों को बयान देना अधिक मुनासिब समझा। इस्तीफे के कारणों में से एक कश्मीर समस्या पर मतभेद भी था। आंबेडकर चाहते थे कि हिंदू बहुल और बौद्ध बहुल इलाके भारत में रहें और मुस्लिम बहुल इलाके यानी कश्मीर घाटी समेत कुछ अन्य इलाके भी पाकिस्तान को दे दिए जाएं। क्या आज कोई इस विचार का समर्थन करेगा या आंबेडकर की विरासत के इस हिस्से को अपनाएगा? उनके कुछ भक्त अपना भी सकते हैं लेकिन बहुसंख्यक भारतीय तो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आंबेडकर की असली विरासत है जाति का समूल नाश करने का उनका संकल्प। ब्राह्मणवाद का सार इस मान्यता में निहित है कि किसी भी व्यक्ति अथवा समूह का गुण-दोष निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाए। यह दृष्टिकोण एक प्रकार का नस्लवाद ही है जो नात्सीवाद की ओर ले जाता है। इस मान्यता को ऋग्वेद के पुरुषसूक्त उद्धृत करके पुष्ट किया जाता है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः, उरू तदस्य यदवैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अ जायत। अर्थात ब्राह्मण विराट पुरुष का मुख हैं, क्षत्रिय बाहु हैं, वैश्य जंघा हैं और शूद्र पांव हैं। वर्णों की ऊंच-नीच का यह सर्वप्रथम धार्मिक-सैद्धांतिक आधार है। इस आधार पर समाज का विभाजन करके एक विशाल जनसमूह को केवल उसके जन्म के कारण हजारों साल तक एक ही तरह के काम करने और अछूत माने जाने के लिए अभिशप्त बना दिया गया।
आंबेडकर ने अपने जीवन में इस अपमान के दंश को बहुत समय तक बहुत तीव्रता के साथ झेला था। इसलिए 1936 में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उनका जन्म भले ही हिंदू के रूप में हुआ हो लेकिन उनकी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। निधन से कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लेकिन क्या जाति केवल एक विचार है? क्या मेरे या मुझ जैसे लाखों व्यक्तियों के इस विचार से मुक्त हो जाने मात्र से यह समाप्त हो सकती है? ऐतिहासिक अनुभव तो यही बताता है कि ऐसा संभव नहीं है। इस्लाम और ईसाइयत के भारत में आने के बाद निचली जातियों के लोग बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई बने क्योंकि वे सामाजिक समानता की तलाश कर रहे थे और इन धर्मों में उन्हें इसकी गुंजाइश नजर आती थी। बाद में अनेक सिख धर्म में भी दीक्षित हुए क्योंकि सिख गुरु भी जाति भेद के खिलाफ थे। लंगर में सबका एक साथ बैठकर खाना इसका प्रमाण है। लेकिन क्या भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में जातिभेद नहीं है? वह वहां भी बरकरार है। बौद्ध बनने से भी दलितों की समस्या नहीं सुलझ पाई और आंबेडकर द्वारा दिखाया गया यह रास्ता भी अंधी गली में जाकर खत्म हो गया। इसका कारण यह है कि भारत में, विशेष रूप से गांवों में जाति व्यवस्था केवल जाति की विचारधारा पर नहीं बल्कि जटिल बुनावट वाले आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने पर आधारित है। उसका सीधा सा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसे चलाने के लिए आवश्यक श्रम से है। जब तक यह ताना-बाना कमजोर और अंततः छिन्न-भिन्न नहीं होता तब तक जाति का समूल नाश नहीं हो सकता और आंबेडकर द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंबेडकर भी इस हकीकत से अच्छी तरह परिचित थे कि केवल कानून बना देने से मूलभूत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता। यह अकारण नहीं कि जाति का संहार नामक अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति (इसे लाहौर में जात-पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के तौर पर लिखा गया था पर कुछ अप्रिय कारणों से वह अधिवेशन ही रद्द हो गया) में आंबेडकर ने लासाल के 1861 में दिए गए एक भाषण को उद्धृत किया था जिसमें लासाल ने कहा था कि केवल उन्हीं राजनीतिक संविधानों का मूल्य या स्थायित्व है जो किसी समाज में उपस्थित शक्तियों की बिलकुल सही अभिव्यक्ति करते हैं। भारतीय संविधान में आदर्श प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं लेकिन अमल में वे कहीं नजर नहीं आते क्योंकि समाज में जिन शक्तियों का वर्चस्व है, उनका एजेंडा कुछ और ही है। आज के हालात में आंबेडकर के इन शब्दों को याद रखना जरूरी हैः ‘‘धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकती है लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही की ओर ही ले जाती है।’’
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और कला-संस्कृति पर लिखते हैं)