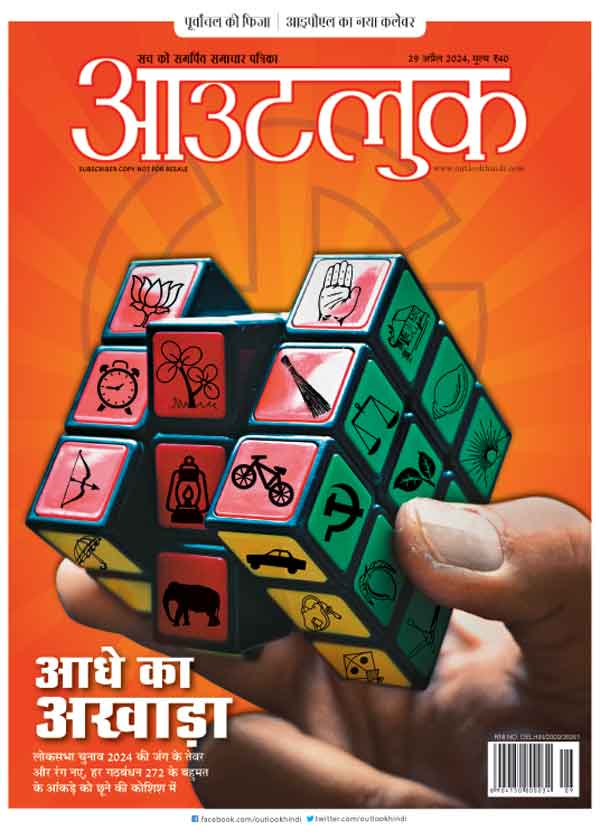पिछली शताब्दी के पूर्वार्द्ध का यूरोपीय इतिहास रक्तरंजित रहा है और प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध भी यूरोपीय राजनीति के कारण ही हुए थे। इसी दौरान इटली में फासीवाद, जर्मनी में नात्सीवाद और स्पेन में फ्रांकोवाद ने जड़ें जमाईं। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। जर्मनी में तो जैसे हिटलर ने वहां की जनता पर वशीकरण मंत्र ही फूंक दिया था क्योंकि अधिकांश जर्मन अपने फ्यूहरर के पीछे पागल थे। लेकिन क्या यह आकस्मिक था कि फासीवाद और नात्सीवाद का उदय हुआ, इन एक-दूसरे से मिलती-जुलती राजनीतिक प्रवृत्तियों में निहित अमानवीयता और हिंसा को इतनी व्यापक सामाजिक-राजनीतिक स्वीकृति मिली और जनसामान्य द्वारा अपने नेताओं की लगभग पागलपन की हद तक जाकर पूजा की गई? इसका उत्तर खोजने के लिए यूरोपीय बौद्धिक जगत में उत्पन्न होने वाले विचारों और उनके द्वारा समर्थित घटनाओं पर एक नजर डालनी होगी। इससे भी पहले यह याद रखना होगा कि अमेरिका में जिस तरह यूरोपीय देशों के लोगों ने जाकर वहां के मूल निवासियों का सामूहिक जनसंहार किया और उनका लगभग सफाया ही कर दिया, वह मानव इतिहास में दर्ज सबसे पहला और सबसे अधिक अमानुषिक हिंसक कांड था।
जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने 4 मई, 1898 को अल्बर्ट हॉल में दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में घोषणा की कि ‘‘दुनिया के राष्ट्रों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जीवंत और मरणशील’’ उस समय हिटलर नौ साल का बालक था। तब तक उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में इस धारणा को व्यापक स्वीकृति मिल चुकी थी कि साम्राज्यवाद ने पृथ्वी से निम्नतर नस्लों का सफाया करके मानव-सभ्यता की बहुत बड़ी सेवा की है और साम्राज्यवाद एक ऐसी अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरान प्रकृति के नियमों के अनुसार हीनतर नस्लों का विनाश होता है।
उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत ही तस्मानिया नामक द्वीप में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के 1803 में आगमन से हुई और अगले ही साल से वहां के मूल निवासियों का सफाया किया जाना शुरू हो गया। अंतिम मूल निवासी की मृत्यु 1869 में हुई। 1904 में जर्मनों ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ऐसा ही अभियान चला कर हेरोरो लोगों का सफाया कर दिया। उस समय युद्ध को भी दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया : सभ्य राष्ट्र-राज्यों के बीच होने वाले युद्ध जिनमें युद्ध के नियम लागू किए जाएंगे और औपनिवेशिक युद्ध जिनमें प्रकृति के नियम यानी निम्नतर नस्लों के खात्मे का जैविक अनिवार्यता वाले नियम लागू किए जाएंगे। प्रसिद्ध अश्वेत फ्रेंच कवि एमी सीजेर ने लिखा है कि बीसवीं शताब्दी के हर अतिविशिष्ट, अति मानवीयतावादी और हर अति धार्मिक ईसाई बुर्जुआ के भीतर एक हिटलर सो रहा है लेकिन फिर भी यूरोपीय बुर्जुआ हिटलर को माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने यूरोप के साथ वही बर्ताव किया जो अल्जीरिया के अरबों, भारत के कुलियों और अफ्रीका के नीग्रो के साथ किया जाता था।
मुझे आज यह सब क्यों याद आ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ साल से न केवल भारत में राजनीतिक-सामाजिक हिंसा बढ़ती जा रही है बल्कि अब तो सत्तारूढ़ पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी खुलेआम उन लोगों की हत्या के लिए पांच और दस करोड़ रुपये की सुपारी की घोषणा कर रहे हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। क्या यह सब अचानक हो रहा है या फिर पिछले दशकों के दौरान हमारे समाज में ऐसी चिंतनधाराओं को धीरे-धीरे स्वीकृति मिलती गई है जो हिंसा का महिमामंडन करती हैं और प्रेरणा के लिए हिटलर जैसे (खल)नायकों की ओर देखती हैं।
भारत के बारे में आम तौर पर यह धारणा रही है कि यहां सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होते रहे हैं और हिंसा ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। लेकिन क्या वाकई हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है? हाल ही में इतिहासकार उपिंदर सिंह द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्राचीन भारत में राजनीतिक हिंसा प्रकाशित हुई है। हम बचपन से ही ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ सूक्ति पढ़ते आए हैं लेकिन इस पुस्तक से ही पता चला कि ‘मानव धर्मशास्त्र’ अर्थात मनुस्मृति में आने वाली इस सूक्ति का असली मंतव्य आभासी हिंसा और असली हिंसा में अंतर करना है और इस तरह यह भी स्थापित करना है कि लक्ष्य ही उसे प्राप्त करने के साधनों की वैधता की कसौटी है। इसलिए वैदिक याग-यज्ञ के लिए जानवरों को मारना वास्तविक हिंसा नहीं है क्योंकि यह कल्याणकारी कर्म है। ऐसी स्थितियों में जहां दूसरे की हत्या करना आवश्यक, अर्थपूर्ण और लाभकारी हो तो उसे हिंसा नहीं माना जा सकता। जो लोग मनुस्मृति को स्वतंत्र भारत के संविधान का दर्जा देना चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वे यदि इन दिनों नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाकर मंदिर बना रहे हैं और स्मारक खड़े कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या? उनकी दृष्टि में तो महात्मा गांधी की हत्या आवश्यक, अर्थपूर्ण और लाभकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक गुजरात के दंगों के लिए खेद व्यक्त नहीं किया और न ही वे रोज घोषित की जा रही सुपारियों पर ही अपने ‘मन की बात’ बताते हैं। क्या इस मौन की जड़ें हमारे इतिहास में नहीं हैं?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और कला-संस्कृति पर लिखते हैं)