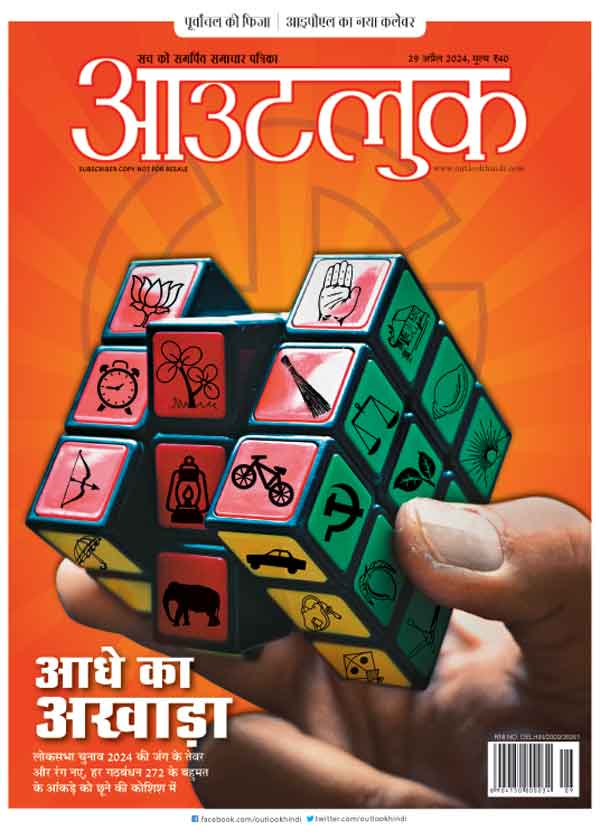बॉलीवुड नई उड़ान के लिए पंख पसार रहा है। वह उन बातों को भी हवा दे रहा है, जिन पर बात करना कई लोग वर्जित समझते हैं। इस नए दौर का अंदाज-ए-बयां कुछ कॉमिक है और हंसी-हंसी में गंभीर बातें हो रही हैं। आम दर्शक इन फिल्मों को पसंद कर रहा है, वर्जित विषयों पर बात कर रहा है। कारण? सबको लगता है ये अंदर की बात है। मगर हिंदी सिनेमा अब नए ढंग से सोच रहा है। इंटरनेट के जमाने में जब सारे पर्दे झीने हो रहे हैं, बॉलीवुड समझ चुका है कि अब बात करने का समय आ गया है। इसलिए जून में आई निर्देशक अभिषेक सक्सेना की फुल्लू (शारिब अली हाशमी/ज्योति सेठी) ने मासिक धर्म के अस्वस्थ मिथकों को तोड़ने की स्वस्थ शुरुआत की तो आयुष्मान खुराना-भूमि पेडनेकर की शुभ मंगल सावधान पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को खुल कर सामने लाई है। वैज्ञानिक तथ्य है कि अपने जीवन में हर पुरुष कभी न कभी इस समस्या का सामना करता है। फिल्म में इस मुश्किल पर पति-पत्नी के बीच बंद कमरे में चर्चा ही नहीं बल्कि विवाह से पहले वर-वधू पक्ष के बीच आकाश तले खुली बातचीत है। यहां वही आयुष्मान खुराना नपुंसकता से ग्रस्त हैं जो फिल्म विक्की डोनर (2012) में शुक्राणु दानदाता बने थे। वास्तव में ऐसे विषयों में कॉमेडी ही वह बीच का रास्ता है, जो पोंगापंथियों के गुस्से से बचाता है। बॉलीवुड इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नसबंदी जैसे विषय पर बनी फिल्म पोस्टर बॉएज भी बहुत सारी बातें हंसाते हुए कहते निकल जाती है। निर्देशक श्रेयस तलपडे की इस फिल्म में सरकारी नसबंदी अभियान में तीन ऐसे युवकों (सनी देओल, बॉबी देओल, श्रेयस तलपडे) के चेहरे पोस्टर पर छप जाते हैं, जिन्होंने नसबंदी कराई ही नहीं।
बॉलीवुड सिनेमा अपना दायरा बढ़ा रहा है। नए-नए विषय आ रहे हैं। दृश्यों और संवादों में बंदिशें टूट रही हैं। फिल्मी दुनिया मान चुकी है कि इस दौर में फार्मूले जैसी कोई चीज काम नहीं करेगी। नए समय में नई बातों, नई सोच की जरूरत है। इसीलिए उन विषयों में भी कहानियां तलाशी जाने लगी हैं, जो दबी जुबान में फुसफुसाई जाती रही हैं। अब जिस तरह से भारतीय सिनेमा में बदलाव आ रहे हैं, उससे लगता है आने वाले दिनों में कोई बात ढकी-छुपी नहीं रहेगी। मनोरंजन के साथ एजुकेशन का लक्ष्य भी जुड़ रहा है। अच्छा सिनेमा यही करता है।
इसका बड़ा उदाहरण बीते स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई अक्षय कुमार-भूमि पेडनेकर की टॉयलेटः एक प्रेमकथा है। इस फिल्म के अप्रत्याशित ढंग से 100 करोड़ से ऊपर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने फिर स्थापित किया कि लोग अपने परिवेश का सिनेमा देखना चाहते हैं। वे अच्छाइयों के साथ कमियों पर भी बात करने को तैयार हैं। इसे अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार समाज का लक्षण मान सकते हैं। खुले में शौच के विरुद्ध और घरों में शौचालय बनाने के संदेश वाली यह फिल्म जिस तरह हाथों-हाथ ली गई उसने साफ संदेश दिया कि हिंदी में बड़ी सफलता के लिए कहानियों को महानगरों से निकाल कर छोटे शहरों में स्थापित किए जाने की जरूरत है। डेढ़-दो दशक पहले एनआरआई सिनेमा के दौर में हिंदी पट्टी मुंबई में स्थित फिल्म इंडस्ट्री के लिए केवल बी-ग्रेड कहानियों की जगह थी। मगर अब बाजी पलट गई है। हिंदी पट्टी और छोटे शहर कहानियों के केंद्र में आ गए हैं। मिडिल क्लास और कस्बे से हीरो निकल रहा है। निल बटे सन्नाटा में एक घरेलू नौकरानी के सपनों की कहानी बुनने वाली, निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी की बरेली की बर्फी जैसी कम बजट फिल्म ने धीमी शुरुआत के बावजूद अच्छा बिजनेस किया। बड़े पर्दे पर मध्यम और गरीब वर्ग के चरित्र, चिंताएं, आशाएं, प्रेम, संवेग और हताशा बड़े दर्शक वर्ग को सिनेमाघरों तक ला रही हैं।

अक्षय कुमार फिल्मों के नए सामाजिक-राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर आए हैं। उनकी अगली फिल्म पैडमैन भी बड़े सामाजिक संदेश के साथ है। फुल्लू के बाद अक्षय की यह फिल्म भी महिलाओं के मासिक धर्म की चिंताओं पर बात करते हुए ऐसे व्यक्ति की कहानी कहेगी, जो सस्ती दर पर सैनेटरी पैड्स बनाने की मशीन का आविष्कार करता है। सिनेमा के कंधे पर सिर्फ मनोरंजन की जिम्मेदारी ही नहीं है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह घर-परिवार के संग मिल बैठ कर देखने योग्य सामग्री दे। ऐसे में वर्जित समझे जाने वाले विषयों वाली फिल्मों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनकी कहानियां घर-परिवार और रिश्तों में बुनी गई हैं। यह देश-समाज की बदलती तस्वीर को भी पेश करती हैं। नए माता-पिता स्वीकार रहे हैं कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा सही ढंग से मिलनी चाहिए। ताकि वे गलत राह पर न चलें। डाइनिंग टेबल पर भले संभव नहीं, मगर परिवार और दोस्तों की मंडली में ये बातें सहजता से जगह बनाने लगी हैं। फिल्में भी जुगुप्सा पैदा करने के बजाय इन विषयों को स्वस्थ ढंग से पेश करने की कोशिश में हैं। पहलाज निहलानी के सेंसर बोर्ड की चेयरमैन पद से विदाई और प्रसून जोशी के आने के बाद एक उदार दौर शुरू हो चुका है।
फिल्मकार पुरानी बातों को भी नए ढंग से कहने का जोखिम ले रहे हैं। सोचने-कहने का ढंग बदला है। रेप और समलैंगिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आई फिल्मों में भी पिछले दिनों यह बात दिखी। पिंक और अलीगढ़ ने इन्हें नए नजरिए से देखा। पिंक जहां लड़की की ‘ना का मतलब ना’ जैसा ठोस संदेश देती है, वहीं अलीगढ़ समाज में समलैंगिक व्यक्ति के बंद कमरे के भीतर निजी स्पेस की वकालत करती है, जिसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं। ये फिल्में आने वाले दिनों का संकेत हैं जब निजता का मौलिक अधिकार कागज से निकल कर साकार रूप लेना शुरू करेगा।
सिर्फ सेक्स ही नहीं, अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सिनेमा पहले खुल कर बोलने से बचता था क्योंकि हर कोने से हमले का डर था। राजनीतिक-धार्मिक वजहों से कुछ विषयों को नहीं छुआ जाता था। मगर अब सिनेमा साहस दिखा रहा है। पिछले दिनों आई निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव की लिपस्टिक अंडर माई बुरका की चार में से दो कहानियों में खुल कर मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, बुरके और पुरातनपंथी सोच से आजादी के लिए छटपटाहट की कहानियां दिखाई गईं। दीवाली पर आ रही आमिर खान प्रोडक्शंस की सीक्रेट सुपरस्टार भी बुरके में रहने वाली ऐसी किशोरी की कहानी है, जो संगीत की दुनिया में पहचान बनाने से पहले घर में संघर्ष करती है। संगीत को अपने धर्म के विरुद्ध मानने वाले पिता के विरोध के बावजूद वह किशोरी अपनी जिद से दुनिया में पहचान बनाती है। तय है इस दौर में कोई आवाज दबाई नहीं जा सकती। चाहे वह एक गायक की प्रतिभा हो या विचारों पर बहस की गुंजाइश। आने वाले दिनों में राजकुमार राव की न्यूटन भी ऐसा ही संदेश देती दिखेगी। यह एक ऐसे चुनाव अधिकारी की कहानी है, जिसकी ड्यूटी नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके में लगी है। वहां मात्र 76 वोट हैं। सवा सौ करोड़ की आबादी में 76 वोटों की क्या गिनती? लेकिन फिल्म बताती है कि एक-एक वोट का महत्व क्या है। इसे हल्के में न लें।
गौर करें कि प्री-मैरिटल (विवाह पूर्व) सेक्स सहज ही बॉलीवुड की कहानियों का हिस्सा बन गए हैं। दर्शक इसे अन्यथा नहीं लेते। हाय-तौबा नहीं मचाते। पिछले दो-तीन वर्षों में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जमकर बहस हुई है। भले ही कई लोगों ने इसे लेकर निराशावादी रवैया अपनाया मगर फिल्मों में अभिव्यक्ति मुखर हुई। इसका श्रेय सीधे-सीधे दर्शकों के खाते में जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे सिनेमा को स्वीकार किया। धर्म, जाति, वैचारिक पिछड़ेपन और किसी भी तरह के पाखंड या नकलीपन से ऊपर उठ कर नई कहानियों को हिट बनाया। दर्शकों ने बताया है कि वह काल्पनिक नहीं, वास्तविक कहानियां देखना चाहते हैं। यही वजह है कि बड़े सितारे भी ऐसी कहानियों पर ध्यान दे रहे हैं। जो फिल्में पहले खास दर्शक वर्ग की कहलाती थीं, वह अब आम लोगों की हो चुकी हैं। इससे यह विश्वास भी पुख्ता होता है कि आम लोग ही भविष्य में नए भारत की तस्वीर गढ़ेंगे।