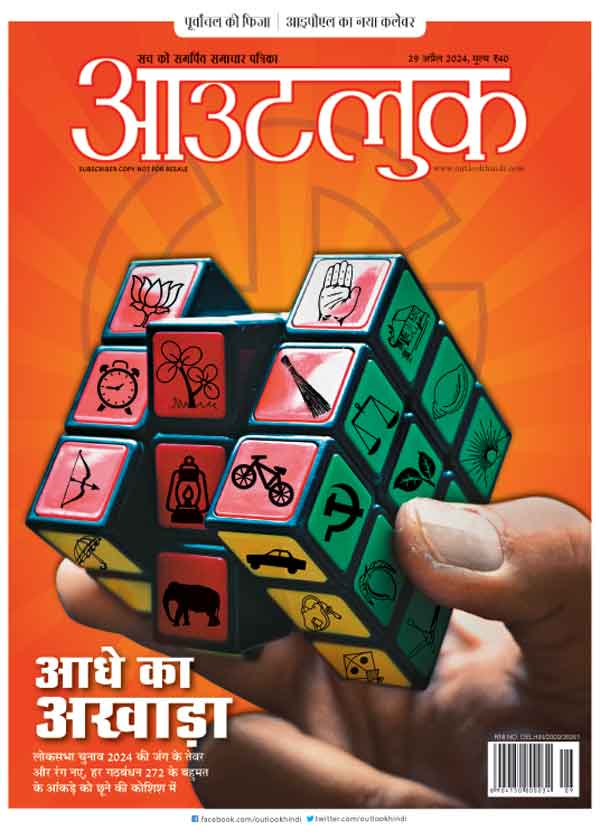भारतीय विश्वविद्यालयों में 1960 के दूसरे भाग में आदर्शवाद और क्रांतिकारिता का बोलबाला था। चारों ओर समाजवाद के नारे गूंज रहे थे। नक्सलवाद का जन्म भी इसी दशक में हुआ था। विश्वविद्यालयों के गलियारों, छात्रावास, कॉफी-हाउसों की बहसों में क्रांति छाई हुई थी, चे ग्वारा की डायरी और माओ की लाल किताब तेजी से हाथों से दिलों में उतर रही थीं। "चेयरमैन माओ को लाल सलाम" अक्सर सुनने को मिलता था। ठीक इसी समय फ्रांस में पेरिस जल रहा था। छात्र आंदोलन क्रांति की होली जला रहा था। इसकी गूंज भारत के विश्वविद्यालयों में भी सुनाई पड़ रही थी। छात्रों के बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी भी नहीं कट रही थी। देश के भद्र लोगों के दुर्ग सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज भी क्रांति की आंधी की चपेट में आ चुके थे। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों के छात्रावास मानो पूंजीवाद से मुक्त क्षेत्र से लग रहे थे। जब 1974 में मैंने सोवियत संघ से लौटकर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पदभार संभाला, मेरा मन आनंद विभोर था। विश्वविद्यालय के सभागारों, कॉफी-हाउसों, पार्कों–चारों ओर मानो विचारों का मंथन चल रहा था। दीवारें होने वाली विचार-गोष्ठियों, सभाओं आदि के बारे में हस्त-लिखित इश्तिहारों से लदी पड़ी थीं। रूस से लौटकर मुझे लगा कि मैं किसी स्वप्नों के देश में आ पहुंचा हूं। लगता था कि हर कोई देश के भविष्य, न्यायपरक समाज, भगत सिंह के सपनों के भारत की खोज में रमा हुआ है। यह भी मुझे लगता था कि आजादी के दीवानों की तरह युवा लोग अपने बारे में कम और देश के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित थे। यहां तक कि उच्चवर्गीय अहंकार का गढ़ सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजों के छात्र भी भगत सिंह के रंग में रंगे हुए थे और उन्होंने अपने दकियानूसी दुर्ग को मानो धराशायी कर दिया था।
पर शीघ्र ही यानी 1975 में शुरू हुआ इमरजेंसी का विकराल तांडव नृत्य। सारे माहौल को खामोशी ने निगल लिया, चारों ओर सन्नाटा, निःशब्दता का बोलबाला।
चारों ओर धर-पकड़, रातोरात ब्लैक मारिया आईं और न जाने कितनों को अपने अंदर ठूंसकर उठा ले गईं। सभाएं बंद, बहसें, तर्क-वितर्क, हंसी-ठिठोली सब गायब। खाने की मेज पर बैठकर एक दूसरे से मात्र मौसम के हाल के बारे में दो-चार शब्दों का ही आदान-प्रदान होता था। कमोबेश सभी विश्वविद्यालयों में यही हाल था।
इमरजेंसी की समाप्ति पर विश्वविद्यालयों में वैचारिक जीवंतता लौटना शुरू हुई। याद है मुझे वह दृश्य जब आर्ट्स फैकल्टी में बोलने के लिए आए जॉर्ज फर्नांडिस का स्वागत वर्तमान में पॉयनियर अखबार के मालिक और संपादक चंदन मित्रा बड़ी गर्मजोशी से “कामरेड जॉर्ज–लाल सलाम” के नारे लगाकर कर रहे थे। हम सब भी बेहद रोमांचित थे।
धीरे-धीरे माहौल इमरजेंसी से पहले जैसा होता गया। सरकारें बनीं, बिगड़ीं, फिर बनीं पर विश्वविद्यालयों में आदर्शवाद का परचम लहराता रहा। 1980 के दशक में सोवियत संघ में पिरिस्त्रोयका यानी पुनर्निर्माण का दौर शुरू होकर 1990 तक अपने चरम पर पहुंच गया। इधर भारत में उथल-पुथल जारी थी। 1984 में सिखों के नरसंहार के दौरान भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक भी सिख विरोधी घटना नहीं हुई। बल्कि अध्यापकों ने अपने सिख साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे। आदर्शवाद का दीया अभी बुझा नहीं था। 1986 में देश में तीन महीने चलने वाली अध्यापकों की हड़ताल हुई। हम सब दीवानों की तरह बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। 1987 में फिर इसी प्रकार की हड़ताल हुई। इस बार मुद्दा था कॉलेजों में प्रोफेसरशिप की स्थापना। हड़ताल आंशिक रूप से सफल रही। चौथे वेतन आयोग के तहत देश के प्राध्यापकों को आइएएस के साथ बराबरी का वेतनमान मिला। पर यहीं से शुरू हुआ प्राध्यापकों के वर्ग चरित्र में बदलाव।
सोवियत संघ 1990 में ढह गया, सारे विश्व में मानो क्रांति का सपना ध्वस्त हो गया। 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। सांप्रदायिक कत्लेआम का दौर सारे देश में चला। देश के विश्वविद्यालयों में भी सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठाने लगीं। अध्यापकों और छात्रों के जेहन में आदर्शवादी जुनून धीमा पड़ने लगा। देश में मनमोहन सिंह द्वारा जनित उदारीकरण और बाजारवाद की हवाएं चलने लगीं। इसी क्रम में 1996 में पांचवें वेतन आयोग ने अध्यापकों के उच्चवर्गीय चरित्र को और पुख्ता कर दिया। न जाने कितने अध्यापक स्टॉक एक्सचेंज की चपेट में आते गए। प्राध्यापन कक्षों में भी शेयरों के उतार-चढ़ाव की चर्चाएं होने लगीं। महिला कॉलेजों के स्टाफ-रूमों में साड़ियों और आभूषणों की छोटी-छोटी प्रदर्शनियां लगने लगीं। काफी बड़ी संख्या में अध्यापक मार्केट मानसिकता का शिकार होते गए।
बीसवीं सदी के अंत में कंप्यूटर और मोबाइल फोन की आंधी जोर पकड़ने लगी। बीसवीं और इक्कीसवीं सदियों के मिलन काल में अटल जी की सरकार ने राष्ट्रीय उद्योगों के निजीकरण की मुहिम को पुरजोर तरजीह दी। इस बीच गुजरात में भारत के इतिहास में भीषण नरसंहार हुआ। देश की आत्मा लहूलुहान हो गई। पर साथ में सांप्रदायिक जुनून भी हिलोरें मारने लगा। लोग भगत सिंह, मार्क्स, माओ और चे ग्वारा को भूलने लगे।
पहले दशक के अंत तक मनमोहन सिंह का उदारीकरण का अभियान चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था। विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर बेंगलूरू, हैदराबाद आदि सूचना टेक्नोलॉजी गढ़ बने नगरों में आकर्षक ‘पे पैकेज’ मिलने लगे। युवा पीढ़ी पे-पैकेज के डिस्कोर्स की जकड़ में आने लगी। कंप्यूटर शिक्षण और प्रशिक्षण के तहत ‘पुश बटन’ व्यक्तित्व या यूं कहिए ‘कॉग्स इन द ह्वील’ व्यक्तित्व या अव्यक्तित्व थोक में तैयार होने लगे।
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि सूचना प्रौद्योगिकी के तहत युवा-पीढ़ी के व्यक्तित्व को तहस-नहस किया जा रहा है। अधिकतर युवा अब साहित्यिक किताबें नहीं पढ़ते, राजनैतिक बहस नहीं करते, सामाजिक और देश की समस्याओं के बारे में नहीं सोचते। वे तो बस अधिकांश समय मोबाइल पर लटके रहते हैं, फेसबुक आदि पर घटिया टिप्पणियां करते रहते हैं। दिमाग उनके कुंद होते जा रहे हैं, विवेक मृतप्राय होता जा रहा है, संवेदनशीलता लुप्त हो रही है। ऐसी पीढ़ी आसानी से किसी भी अंधविश्वास का शिकार हो सकती है। इसे आसानी से जात्यंधता, धर्मांधता व छद्म वादों में फंसाया जा सकता है, भड़काया जा सकता, उकसाया जा सकता है। मोबाइल से हटकर वे आसानी से हाथ में तलवार पकड़ सकते हैं, चाकू ले सकते हैं और बेझिझक जाति, धर्म के नाम पर अपने ही देशवासियों का खून बहा सकते हैं। ऐसे पढ़े-लिखे ‘अनपढ़’, कुंद दिमागों वाले युवा हाथ में तलवार या पिस्तौल लेकर क्या-क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचकर तो दिल दहल जाता है। ऐसे में भगत सिंह के आदर्शवाद के जुनून के लिए युवा पीढ़ी के जेहन में भला स्थान कैसे बचेगा!
आदर्शवाद के खात्मे के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। 2006 के छठे वेतन आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के उच्चवर्गीय चरित्र को संपूर्णता दे दी। 1960 और 1970 के दशकों में सेवारत हुए आदर्शवादी अध्यापकों की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है, वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नई पीढ़ी के अधिकतर अध्यापकों के मूल्यों और मानसिकता में देश-समाज में न्यायपरकता लाने के लिए 1960 या 1970 के दशकों जैसा जुनून नहीं रहा। आज प्रेगमैटिज्म का बोलबाला है, लेसेज-फेयर का जमाना है।
अंत में एक और त्रासदीपूर्ण प्रक्रिया की ओर ध्यान खींचने की नितांत आवश्यकता है। वह है विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में अकादमिक, नैतिक व दूरदृष्टि का ह्रास। आजकल कुलपति बनने के लिए पहले तो प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है। और यदि लंबी सूची से संक्षिप्त सूची तक पहुंच जाए तो फिर साक्षात्कार देना पड़ता है। उन्हें न चुने जाने का अपमान और किरकिरी झेलनी पड़ती है। परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रोफेसर जिन्हें अपना स्वाभिमान प्यारा है वे तो प्रार्थना-पत्र ही नहीं भेजते। हर कीमत पर कुलपति बनने के लिए अपने जमीर का सौदा करने के लिए उतावले उम्मीदवारों से हम न्यायपरकता, विवेकशीलता और आदर्शवादिता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं।
लिहाजा, देश के चोटी के विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग कुलपति बनने लगे जिन्हें साहित्य से घृणा है, किताबों से नफरत है। राजधानी के एक जाने-माने विश्वविद्यालय में ऐसे ही एक कुलपति ने बनते ही सबसे पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय की पुस्तकों की दुकान को यह कहकर बंद करवा दिया कि किताबें युवा पीढ़ी का दिमाग खराब करती हैं। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की ऊंची चार-दीवारी पर लोहे की सीखचों के ऊंचे-ऊंचे द्वार बनाकर विश्वविद्यालय के सभागारों को गोष्ठियों आदि के लिए बंद कर दिया, शिक्षक संगठन को भी अपनी सभाएं सड़कों पर करनी पड़ीं। कोने-कोने पर सीसीटीवी लगाकर शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के कार्य-कलापों को गिद्ध दृष्टि से देखा जाने लगा। शिक्षकों के वजूद को धूल में मिला दिया गया। कुलपति को पिछली सरकार के शिक्षामंत्री की कृपादृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने विश्वविद्यालय में कायदे-कानूनों की धज्जियां उड़ा दीं। नियुक्तियां मात्र कुलपति की जाति के लोगों की होने लगीं, विपक्ष के प्रोफेसरों को विभागाध्यक्ष नहीं बनाया गया। छुट्टी के दिन भी अध्यापक कहीं धरने पर बैठ जाएं तो उनके वेतन में कटौती की जाने लगी।
कुलपति ने शिक्षक संघ को अपने एक पिछलग्गू अध्यापक संगठन की मदद से दो फाड़ कर दिया। हर तरह के विरोध को दबा दिया गया। अध्यापकों की भर्ती में खुलकर पैसे का आदान-प्रदान होने लगा। ऐसे में भला आदर्शवाद कहां टिक सकता था।
नई सरकार से उम्मीद थी कि वह ऐसे भ्रष्ट कुलपति और उसकी चांडाल चौकड़ी के विरुद्ध कदम उठाती। पर नई शासक पार्टी से भी कहीं जाति के नाम पर, कहीं विचारधारा के नाम पर संरक्षण मिल गया और भ्रष्ट चांडाल चौकड़ी न केवल साफ-पाक बच गई बल्कि आज भी उनका बोलबाला है, उन्हीं की लाठी घुमक रही है।
पुराने शिक्षामंत्री ने हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसी महिला को कुलपति बनाया जो उन्हें कनाडा की सैर कराने ले गई थी। विधिवत गठित खोज कमेटी को अवैध तरीके से भंग करवाकर नई खोज कमेटी की सिफारिश लेकर इस महिला को कुलपति बनवाया गया। पांच वर्ष के कार्यकाल में इस कुलपति ने इतना ही विकास कार्य किया कि परिसर के कोने-कोने में सीसीटीवी लगवाकर छात्रों और अध्यापकों पर दमन का चक्र चलाया, बहुत सारे कोर्स अवैध तरीके से बंद कर दिए। छात्रों से छात्रवृत्तियां छीन लीं, दलित विद्यार्थियों को निष्कासित किया, अध्यापकों को अन्याय का शिकार बनाया।
वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में बताया जाता है कि इस कुलपति ने कुलपति का एक आलीशान बंगला होने के बावजूद, अपने निजी मकान का यूनिवर्सिटी के खर्चे पर जीर्णोद्धार करवाया, उसे पूरी तरह फर्निश करवाया और बिजली-पानी बिलों को यूनिवर्सिटी से अदा करवाया। ऊपर से महोदया ने अवैध तरीके से आवासीय भत्ता भी लिया।
बताया जाता है कि जब भी वह किसी मीटिंग के लिए दिल्ली आदि जातीं, पूरा का पूरा दोतरफा विमान भाड़ा मेजबान संगठन से भी लेती रहीं और अपने विश्वविद्यालय से भी। इस सबके बावजूद उनके कार्यकाल पूरा होने पर नई सरकार ने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया। इसी तरह दसियों उदाहरण दिए जा सकते हैं।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बारे में तो सभी जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। कहने का लब्बोलुआब यही है कि आज देश में देशमुख, वीकेआरवी राव, के.एन. राज, सरूप सिंह, उपेंद्र बक्षी, दीपक नायर जैसे जाने-माने विद्वानों की नियुक्ति नहीं होती। इस स्तर पर यदि ह्रास हुआ है तो अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के स्तर पर गिरावट आना जरूरी है।
कुलपतियों के उपर्युक्त दृष्टांत इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि वर्तमान में देश के विश्वविद्यालयों में माहौल अत्यधिक दमघोंटू हो गया है और उच्च शिक्षा के संस्थान ऐसे स्थान नहीं रह गए जहां विचारों के सौ फूल खिल सकें और विश्वविद्यालय ऐसे उद्यान नहीं रहे जहां नाना प्रकार की सुगंध आती हो। जाहिर है, ऐसे वातावरण में आदर्शवाद का ह्रास अवश्यंभावी है। देश को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह तो भविष्य ही बताएगा!
(लेखक प्रख्यात भाषाविद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश ऐंड फॉरेन लैंग्वेज, हैदराबाद के संस्थापक कुलपति हैं)