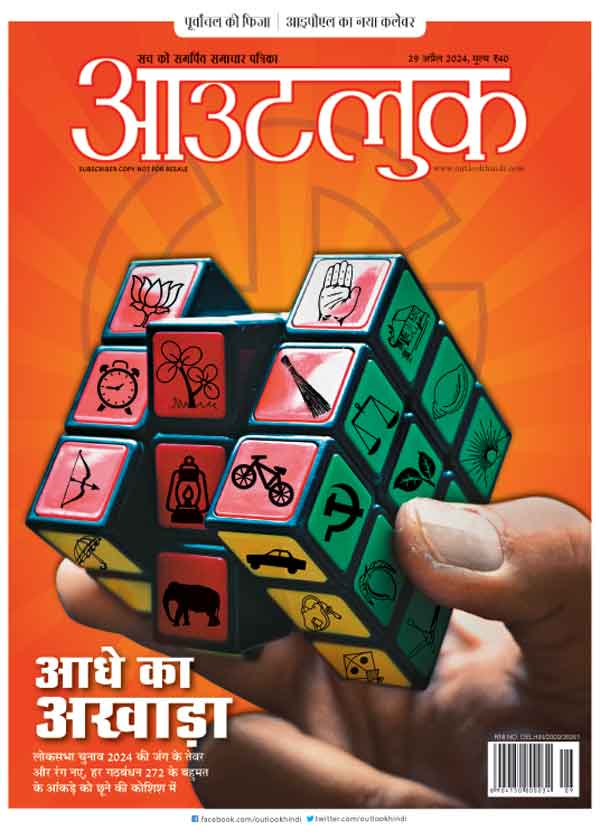बचपन में हमारे अंदर आदर्शवाद और विचारधारा स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बनाती है। हममें से ज्यादातर के लिए उसे आत्मसात करने में कोई परेशानी नहीं होती। हम अपने शुरुआती अनुभवों और अपने 'खास दूसरों' की सीख से उसमें आसानी से रच-बस जाते हैं। जैसे-जैसे हम बचपन और किशोरावस्था से गुजरते हैं, हमारी नैतिक संवेदनशीलता नया आकार लेती है, जो हमें माता-पिता, संगी-साथी, धार्मिक-राजनैतिक रहनुमाओं और उन नायकों से प्राप्त होती है जिनके बारे में हम पढ़ते या सुनते हैं। इस तरह वह आदर्शवाद और विचारधारा उभरती है, जिसे हम अपना मानते हैं। जाहिर है, मैं यहां पश्चिम के नव-प्लेटोवाद और शाश्वत दर्शन या पूरब के बौद्ध और वेदांत दर्शन से जुड़े आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूं। न ही उस तरह की विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसे कार्ल मार्क्स और कार्ल मैनहेम ने परिभाषित किया था। इन दोनों अवधारणाओं को मैं उस रूप में ले रहा हूं, जैसा ये आम जीवन में और राजनैतिक समाजशास्त्र तथा राजनैतिक मनोविज्ञान में इस्तेमाल होती हैं।
************
आदर्शवाद की बुनियाद तब पड़ती है, जब बच्चा पारंपरिक नैतिकता की दहलीज पार करता है और जटिल, सामाजिक रूप से संवेदनशील, नैतिक विकल्प के चयन में सक्षम हो जाता है। यह परिवर्तन प्राय: बच्चे की चेतना के दायरे से बाहर होता है। यह सामान्य बाल विकास का हिस्सा है, जो उस प्रक्रिया के तहत होता है जिसे मनोविश्लेषक सुपर इगो कहते हैं और जिसे बाल मनोवैज्ञानिक ज्यां पियगे और लॉरेंस कॉलबर्ग सामान्य नैतिक विकास कहते हैं।
दीर्घकालीन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का आग्रह करने वाली विचारधारा की तलाश बाद में, किशोरावस्था के दौरान होती है। यह तलाश अधिक सचेतन और बौद्धिक हो सकती है। आमतौर पर उसे मालूम होता है कि वह अपने लिए उपयुक्त विचारधारा की तलाश कर रहा है और अपनी तरजीह की वजह भी बता सकता है। लेकिन ऐसी वजहें भ्रामक हो सकती हैं क्योंकि विचारधारा का यह चयन उसकी ऐसी मानसिक स्थितियों से प्रभावित हो सकता है, जिसका उसे कोई अंदाजा ही न हो। विचारधारा इंसान में गहरे पैठी अनिश्चितता और असुरक्षा दूर करने का माध्यम भी हो सकती है, यह उसके विकास के दौरान बनी नैतिक संवेदनशीलता और आदर्शवाद से बंधी भी हो सकती है। यह कुछ इस तरह भी हो सकती है जैसे कोई कमजोर और हाशिए पर खड़ा आदमी खुद को ताकतवर और काबिल महसूस करने के लिए अति-मर्दवादी विचारधारा को चुन ले।
यह प्रक्रिया व्यक्ति की स्व-चेतना से जुड़ी होती है इसलिए वह विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा को नियंत्रित कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी विचारधारा को दृढ़ उत्साह या थोड़ी निर्लिप्तता के साथ अपना सकता है, ताकि वह राजनैतिक सत्ता, सामाजिक रुतबे, अकादमिक मान-सम्मान हासिल करने या फिर जनसंहार से लेकर चोरतंत्र की स्थापना तक हर प्रकार की दुष्टताओं को जायज ठहराने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल कर सके।
विचारधारा व्यावहारिक राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं से निबटने के लिए आदर्शवाद को गैर-जिम्मेदार, भावुक और रूमानी बताकर खारिज करने का आजमाया तरीका है। अक्सर यह इतना कारगर होता है कि कई लोग तीखी आलोचनाओं से बचने के लिए आदर्शवाद को विचारधारा की चाशनी में लपेटना सीख जाते हैं। अगर इससे भी काम न बने तो आप किसी असहज आदर्शवाद को खारिज करने के लिए किसी विचारधारा का सहारा ले सकते हैं और उसे राजनैतिक रणनीति से सुप्त विरोधी विचारधारा बता सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि कई लोग जोर देते हैं कि वयस्क के नाते हमें आदर्शवाद और विचारधारा से ऊपर उठ जाना चाहिए और मौका पड़ने पर सार्वजनिक जीवन में दोनों का इस्तेमाल राजनैतिक औजार के तौर पर करने में सक्षम होना चाहिए।
हालांकि, इन दो अवधारणाओं में कुछ ऐसा भी है जो सम्मोहक है। यहां तक कि जो लोग अश्लीलता की हद तक कामयाब, हाई-कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी गिनने वाला जीवन जीते हैं, वे भी अपने आदर्शवाद और विचारधारा के फितूर से गुजरने की बातें बड़े चाव से करते पाए जाते हैं। मैंने कई पुराने नेताओं और बड़े कारोबारियों को गर्व से बताते सुना है कि जब तक जीवन के अनुभवों ने उन्हें कठोर, धूर्त और कुटिल बनना नहीं सिखाया था, वे कितने भोले और आदर्शवादी हुआ करते थे। शायद वे यह जाहिर करना चाहते हैं कि वे भी सरल, सज्जन और सदाचारी हुआ करते थे जब तक अधिक यथार्थवादी स्वप्न का पीछा करने के लिए उनका त्याग नहीं करना पड़ा था। घनश्याम दास बिड़ला ने एक बार कहा था कि अगर वे युवा होते तो नक्सलियों की जमात में शामिल हो जाते।
सौभाग्य से, वे यूपीए-2 या भाजपा के दिन नहीं थे, वरना, बिड़ला तमिलनाडु के उन 6000 ग्रामीणों के साथ देखे जाते, जो अपने गांव में परमाणु रिएक्टर का विरोध करने की वजह से राजद्रोह के मुकदमे झेल रहे हैं। उनके नेता, शांतिशोधक उदयकुमार के खिलाफ 101 मुकदमे हैं। गांववाले अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि राजद्रोह क्या और क्यों है? अगर परमाणु रिएक्टर इतनी ही सुरक्षित और सुंदर चीज है, तो उन जगहों पर क्यों नहीं बनाए जा सकते, जहां ताकतवर और धनी-मानी लोग बसते हैं।
************
आदर्शवाद और विचारधारा चचेरे भाई जैसे हैं। सामान्य दौर में वे एक-दूसरे की अतियों पर अंकुश रखते हैं। लेकिन फिलहाल भारत में यह सामान्य दौर नहीं है। महाभारत की तरह, ये चचेरे भाई खंडित परिवार का हिस्सा हैं। ये तभी साथ होते हैं जब राजनीति का हमला होता है। राजनीति का काम अक्सर विचारधारा के नाम पर आदर्शवाद को खारिज करना और आम तौर पर राजनैतिक यथार्थवाद के नाम पर विचारधारा को विकृत करना है। मुझे देंग जियाओ पिंग के एक बयान से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। मुझे बताया गया कि उन्होंने एक बार कहा था, “पश्चिम ने पूंजीवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद को अपनाया। हमने समाजवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद को अपना लिया।’’ विचारधारा और आदर्शवाद के बीच टकराव और वजूद बचाए रखने की राजनीति में फंसे देंग यह कहकर महज बतौर व्यावहारिक नेता अपनी प्राथमिकताओं का ही खुलासा कर रहे थे।
भारतीय सार्वजनिक जीवन में, ‘राजनीति करना’ अपशब्द हो गया है। फिर भी, राजनीति करने की स्वतंत्रता और काबिलियत ही लोकतंत्र की जीवंतता की अंतिम निशानी है। लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि किसी पार्टी या अपनी पसंद के आंदोलन के नाम पर लोगों को संगठित करने या वोट मांगने का हक भी है। उत्तरी कोरिया में लगातार चुनाव होता है और उसके वंशवादी शासक लगातार 90 फीसदी से ज्यादा मत पाकर चुनाव जीतते हैं। मगर कोई भी उस देश पर लोकतंत्र होने का आरोप तक नहीं लगाता।
लोकतंत्र तब मरने लगता है, जब आदर्शवाद, विचारधाराओं और राजनीति में सामान्य प्रतिक्रियाएं होनी बंद हो जाती हैं और सर्वसत्तावादी राजनीति हावी हो जाती है। ऐसी राजनीति के तीन तत्व होते हैं। एक, सब कुछ राजनीति में ही सिमट जाता है और हर मामले में राजनीति घुसपैठ करने लगती है। कभी जाति और धर्म आधारित राजनीति और वंशवादी राजनीति को लोकतंत्र में आदिम व्यवस्थाओं की घुसपैठ माना जाता था। आज ये सामान्य राजनीति का हिस्सा हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह विविधता गैर-बराबरी वाले समाज का अवश्यंभावी हिस्सा है, जिसमें राजनैतिक विचारधाराओं की ज्यादा अहमियत नहीं है तो आपके मनोरंजन के लिए गौरतलब है। मसलन, विश्वविद्यालय की राजनीति (जिसमें छात्र राजनीति, कॉलेज में प्रवेश, अध्यापकों और कुलपतियों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम की राजनीति सब समाहित होती है) विज्ञान और वैज्ञानिक बिरादरी के नौकरशाहों की राजनीति, खेल और सिनेमा की राजनीति और इन सब दायरों को लांघती अवॉर्ड की राजनीति (जिसे हमेशा सामान्य राजनीति के हिस्से के तौर पर देखा जाता रहा, जब तक अवॉर्ड वापसी की राजनीति नहीं आ गई और इसे फौरन सरकारी तौर पर बकवास, राष्ट्रद्रोही, षड्यंत्रकारी राजनीति करार दे दिया गया)। अब इस फेहरिस्त में एक नई रंगीन रवायत को जोड़ सकते हैं- रिटायरमेंट के बाद के लाभों की राजनीति।
इस तरह की लगभग तमाम राजनीति में भारतीय राज्य अहम भूमिका निभाता है। फिर भी, कोई यह नहीं कहता कि भारतीय राज्य पर बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने भी नहीं, जिन्होंने न्यायपालिका पर भारी बोझ से रातों की नींद गंवा दी है, न ही उन्होंने जो यह जान कर चकित होते हैं कि हमारे अतिव्यस्त प्रधानमंत्री देश में नए लोकप्रिय खेल, लिंचिंग पर बोलने के लिए दो साल में समय क्यों नहीं निकाल पाए।
दूसरे, हाल के दौर में भारत में राजनैतिक संघर्ष और राजनैतिक गोलबंदी की तकनीक बदल गई है। लोकलुभावन वाकपटुता, मीडिया खासकर सोशल मीडिया का चालाकी से प्रयोग, स्मार्ट नारेबाजी की वजह से चुनाव अभियानों का अहम हिस्सा बन गई है। हम यह समझ ही नहीं पाए हैं कि हमारे नेताओं ने एक अहम सत्य फिर ईजाद कर लिया है, जिसे छुटभैए और प्रोपगैंडा वाले हमेशा से जानते थे। वह यह कि राजनीति में नफरत की रफ्तार सकारात्मक भावों से ज्यादा होती है, खासकर जब लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही हो या जब राज्य का शासन तंत्र कमजोर पड़ने लगे।
नफरत हमारे दुश्मनों को परिभाषित करती है। और यह परिभाषा हमेशा हमारी मित्रताओं से तीखी होती है। इसी वजह से सभी राष्ट्रवाद, खासकर जब वह राज्य-केंद्रित हो, नफरत आधारित होता है। केवल वही राष्ट्रवाद अपवाद है जो राष्ट्रवाद के पारंपरिक अर्थ को खारिज करता है और उसे देशभक्ति का पर्याय मानता है। देशभक्ति अधिक पुराना शब्द है जिससे क्षेत्र विशेष के प्रति प्राकृतिक मानवीय भावना का आभास होता है। राष्ट्रवाद की तरह यह कोई विचारधारा नहीं है। दोस्तों के बजाय दुश्मनों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना आसान होता है।
तीसरे, आंकड़ों वाला राष्ट्रवाद हर नागरिक से अकेले जुड़ने की फिराक में रहता है। यह समुदाय पर शक करता है और सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों और यहां तक कि व्यापार संगठनों, एनजीओ, छात्र संगठनों, नागरिक आंदोलनों, पेशेवर संगठनों के बारे में उसकी अलग राय होती है। इस मुद्दे पर सारे राजनीतिक दलों में आम सहमति जान पड़ती है, जो बाकी मामलों में बेहद बंटे हुए हैं। इस तरह अकेला नागरिक राज्य का अकेले सामना करता है क्योंकि कोई स्वायत्त संस्था, समुदाय या आंदोलन हस्तक्षेप करने को बचा नहीं रह जाता है। राज्य पर अंकुश रखने वाली कुछेक संस्थाओं में एक न्यायपालिका अपने खर्चीले और समय खपाऊ प्रक्रिया के चलते आम आदमी की पहुंच से बाहर है।
विभिन्न आयोग जिनसे समाज के विभिन्न तबकों जैसे अल्पसंख्यकों, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति और प्रेस के मानवाधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है, अमूमन बेअसर होते हैं या मौके पर काम नहीं आते, जैसे गोरक्षकों और नैतिक पहरुओं के मामले में। समय के साथ (1) जनमत के विविध स्वर खुद ही विभाजनकारी और कर्कश आवाजों में गुम हो जाते हैं। (2) राजनीति में विपक्ष का वजूद ही सत्ता प्रतिष्ठान और राष्ट्र-राज्य के खिलाफ षड्यंत्र की तरह पेश किया जाता है। (3) पहले ही छोटी नीति निर्माताओं की टोली और सिकुड़ने लगती है।
चौथे, जियाउद्दीन सरदार (दार्शनिक, विज्ञान और इस्लामिक विचार के इतिहासकार) जिसे पोस्ट-नॉर्मल टाइम या उत्तर-सामान्य समय कहते हैं, उसकी लहरें भारत के तट तक पहुंच चुकी हैं। अगर मैं इसमें एक और कथन जोड़ सकूं तो हम सार्वजनिक जीवन की उत्तर-सामान्य संस्कृति के दौर में हैं जहां सामान्य समय का विचार अब लागू नहीं होता। वह अतीत की तरफ धकेल दिया गया है या भविष्य की तरफ, ऐसा भविष्य जो परिभाषित नहीं है। (यह गांधी का रामराज्य कतई नहीं है, जो वर्तमान की तीखी आलोचना है। यह रामराज्य का ऐसा संस्करण है, जिसकी वर्तमान से मिलीभगत है और जो इसे बेहिचक बढ़ावा देता है।)
इसलिए, वर्तमान को इस गहरी वास्तविकता से दो-चार होना पड़ेगा जो इन क्षणिक गतिविधियों की वजह से अभिशप्त है और खुद को शालीन तरीके से दफनाए जाने का इंतजार कर रहा है। इस दौर में, सामान्य शराफत, किसी भी तरह का आदर्शवाद, राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता, यहां तक कि विभिन्न धर्मों की आध्यात्मिक चेतना को छोटे से रेगिस्तान सरीखी जगह पर जिंदा रहना होगा। जहां तक बड़े सार्वजनिक दायरे की बात है, तो उसे रोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों की तरह, जो कथित तौर पर नागरिकों को ‘रोटी और सर्कस’ मुहैया करवाने के दम पर बचा रहा, भारतीयों को भी ‘सर्कस और सर्कस’ की असीमित खुराक से संतुष्ट होना पड़ेगा।
(लेखक राजनैतिक-सामाजिक मनोविज्ञान के प्रख्यात विद्वान, सीएसडीएस के मानद फेलो हैं)