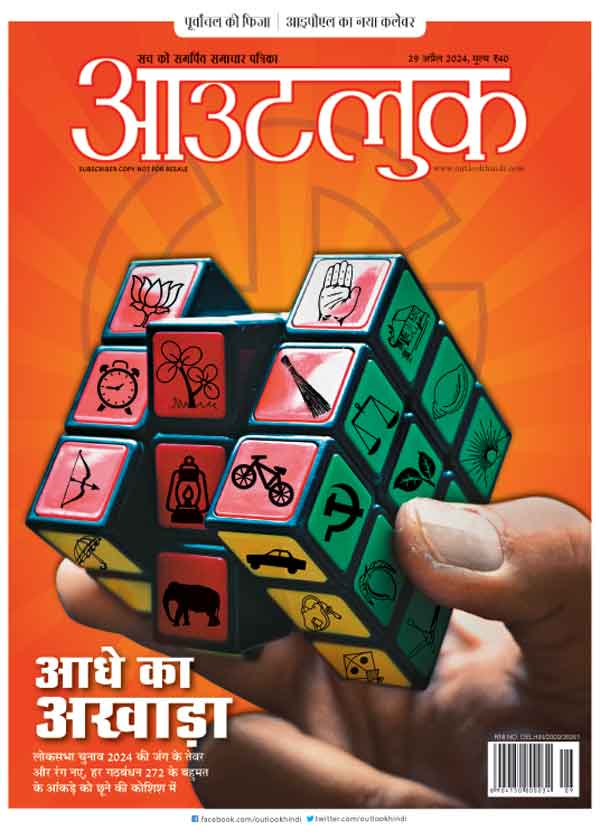कृष्णा सोबती 93 वर्ष की हो गई थीं। कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं, किन्तु वृद्धा नहीं लग रही थीं। लेखक के रूप में तो वे अंत तक प्रयोगधर्मी और अभूतपूर्व बनी रहीं। उन्होंने अपने को कभी दुहराया नहीं। उनके व्यक्तित्व की ऊर्जा और ताजगी उनके लेखन में रची-बसी थी। वे महिला लेखिका कहलाना नापसंद करती थीं। वे स्त्रीवादी नहीं थीं। वे अपने को केवल लेखक कहलाना पसंद करती थीं।
छठे दशक के शुरुआती दिनों की बात होगी। यारो के यार प्रकाशित हुई थी। एक गोष्ठी में एक लेखक ने चुनौती दी, “क्या कृष्णा जी उन शब्दों का (आशय अश्लील शब्दों से था) इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से कहीं कर सकती हैं जिसका इस कहानी में किया है?” कृष्णा जी चुपचाप उठीं। उस शब्द का उच्चारण कर चुपचाप बैठ गईं।
उनके निधन से एक हफ्ते पहले मैंने फोन किया था। मैंने समझा था इतनी बीमार हैं तो धीरे से, कराहकर बोलेंगी। मुमकिन है फोन पर बात भी न कर सकें। वे ठठा कर ऐसे हंसीं कि लगा ही नहीं कि बीमार हैं। वे मृत्यु के बारे में निर्भीक होकर हंसी-मजाक कर रही थीं। उनका मूड आश्वस्त करने वाला था। आखिर तक वे लिखती रहीं, जहां मन हुआ जाती रहीं, और बड़ी बात कि दूसरों का लिखा पढ़ती और अपनी राय देती रहीं। वे अनथक लेखिका और अनथक पाठिका थीं। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू इन भाषाओं के बारे में हमारी जानकारी है, संभवतः वे कुछ अन्य भाषाएं भी जानती रही होंगी। जो अच्छा लगे, उस पर फौरन राय देती थीं। बुरा लगे उस पर भी। वे जागरूक और सक्रिय नागरिक थीं। प्रगतिशील, मानवीय राजनीति की पक्षधर, ऐसी राजनीति जो संस्कृति का ही एक आयाम हो, संकीर्णताओं से दूर ही नहीं उनकी विरोधी हो। वे समय-समय पर अपने विचारों को समाचार-पत्रों में लिखकर प्रकाशित कराती थीं। उन्होंने जीवन अपनी रुचि और शर्तों पर जिया।
अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले और कई लोग देखे हैं। अकेला जीवन जीने वाले निर्भीक तो देखे हैं किंतु संतुलित और शिष्ट बहुत कम। उनके व्यक्तित्व की कोई कोर दबी रह जाती है और वे प्रायः घोर मनोग्रंथियों के शिकार हो जाते हैं। सीधे कहूं तो उनके लिए अपना अभाव या अपने जीवन की कमी इतनी बड़ी हो जाती है कि वे किसी और का सुख नहीं देख पाते। जब हम कहते हैं कि कृष्णा जी ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी तो उसका मतलब ही होता है कि वे आजीवन अंतर्बाह्य की लड़ाई लड़ती रहीं। उनके परिचित और मित्र जानते हैं कि वे किसी भी मौके पर बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं देना नहीं भूलती थीं। अगर आपसे मित्रता है तो आपके पूरे परिवार की खोज खबर लेती रहतीं, पूछताछ करती रहती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि कृष्णा जी के साथ कहीं गए, उन्हें कुछ सामान खरीदना था। आप गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं और कृष्णा जी लदी-फंदी लौट रही हैं। वे अपना सामान खरीदकर आ रही हैं, आकर उन्होंने आपको भी एक-दो पैकेट पकड़ा दिए- फल, मिठाई की टोकरी, कुछ नहीं तो पेन या खूबसूरत पैड ही। वे स्वभाव से उत्सवधर्मी थीं। लद्दाख गईं तो वहां के बारे में अद्भुत सुंदर चित्रों से भरी हुई एक किताब दी। माइकल ऐंग्लो की कृतियों की एक संग्रहणीय किताब भेंट की। हाल ही में निधन से कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा टेबल लैंप विष्णु नागर और मुझे भेंट किया। घर पहुंचने पर जैसा स्वागत वे करती थीं, वह वर्णनातीत था। सुखद इस अर्थ में कि छद्म और अतिरिक्तता से दूर। वे समझौता नहीं करती थीं, न जीवन में न लेखन में, न राजनीतिक विचारों में। ये दृढ़ता उनकी शिष्टता में ही समाहित थी। विरोध करने पर असहमति दर्ज करते समय वे छोटा-बड़ा नहीं देखती थीं। उन्हें प्रसन्न करना आसान था किंतु मना पाना कठिन।
साहित्यकार शब्दों को बरतता है। शब्दों का उसके लिए परम महत्व है। लेकिन साहित्यकार शब्दों की सुरक्षा के लिए लड़ते कम देखे गए हैं। लड़ने वालों की संख्या ज्यादा नहीं होती। विशेषकर हमारे समय में जब केदारनाथ सिंह को लिखना पड़ा कि हमारे समय का मुहावरा है, “फर्क नहीं पड़ता/जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क।” ऐसे समय में जब देश में सुविधाजीविता, अवसरवादिता मूल्यहीनता अबाध हो गई है, कृष्णा जी ने ‘जिंदगीनामा’ शब्द के लिए दीर्घकालीन मुकदमेबाजी की। वह भी अमृता प्रीतम जैसी लेखिका से जिनके समर्थन में खुशवंत सिंह जैसे पत्रकार खुलकर सामने आए। कृष्णा जी के ही अनेक मित्रों ने समझाया-जाने दीजिए, शब्द का ही तो मामला है। आपने उपन्यास का नाम रखा जिंदगीनामा अमृता प्रीतम ने रख लिया हर दत्त का जिंदगीनामा। कौन बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन कृष्णा जी के लिए उनकी रचना सचमुच संतान की तरह होती थी। उसकी सुरक्षा में उन्होंने जोखिम उठाया। कितनी दौड़-धूप करनी पड़ी। कितना पैसा खर्च करना पड़ा। कितने नाराज हुए, इसकी जांच-पड़ताल अभी नहीं की गई है।
सम्मान-पुरस्कार के लिए उन्होंने कोई कोशिश कभी नहीं की। कई सम्मान नहीं लिए। कई लौटा दिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार कर लेने के लिए उन्हें कितना मनाना पड़ा। अंत में भी वे उसे ग्रहण करने नहीं पहुंच पाईं, अस्वस्थता के कारण।
कृष्णा सोबती उदार मानवीय संवेदना की लेखिका थीं। संकीर्णता छू तक नहीं गई थी। राजनीति में संकीर्णता का विरोध करती थीं। चुप रहकर या केवल बातचीत में नहीं। समय-समय पर लिखित वक्तव्यों के प्रकाशन के द्वारा और हिंदी समाज और अन्य भाषा-भाषी विज्ञ-जन भी उनकी बात ध्यान से सुनते और प्रभावित होते थे। यों वे ठेठ पंजाबिन थीं। पंजाबियत उनमें रची-बसी थी। उनकी भाषा, पोशाक, खान-पान, रहन-सहन में पंजाबियत साफ झलकती थी। भारत विभाजन से पंजाबियत को कितना झटका लगा था, उसका गहरा आघात वे महसूस करती थीं। जिंदगीनामा विभाजन की ही ऐतिहासिक मानवीय ट्रेजेडी का लेखा-जोखा है जिसे संभवतः कई खंडों में पूरा होना था। दुर्भाग्यवश उसका लेखन और प्रकाशन ही उनके व्यक्तिगत जीवन का इतिहास खंड तो बन गया, लेकिन रचना पूरी नहीं हुई।
कृष्णा जी लगभग पूरे जीवन अकेली ही रहीं। अंतिम दौर के कुछ वर्षों में डोगरी साहित्यकार शिवनाथ जी के साथ रहने लगीं, विवाह करके। शिवनाथ जी लंबे, गोरे, शिष्ट व्यक्ति थे। कहते हैं वय में कृष्णा जी से कुछ छोटे थे। दुर्भाग्यवश वे पहले चले गए। कृष्णा जी फिर अकेली रह गईं। हां, विमलेश जी नामक महिला ने इस स्थिति में उनकी जो सेवा की उसके लिए कृष्णा जी के मित्रों, पाठकों और हिंदी समाज को उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अशोक वाजपेयी ने शोक-सभा में बताया कि कृष्णा जी रज़ा फाउंडेशन को एक करोड़ से अधिक राशि दे गई हैं, साहित्य सेवा में उपयोग के लिए।
कृष्णा सोबती की हर रचना एक प्रयोग है। वे प्रत्येक रचना पर लगभग शोध करके उसे शब्दों में ढालती थीं। मित्रो मरजानी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसे भैरवप्रसाद गुप्त ने मित्रो मरजानी और अन्य कहानियां नामक पुस्तक में छापा था। बाद में यह उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। कृष्णा जी को पारिवारिकता नहीं मिली लेकिन पारिवारिकता से उनका आंतरिक लगाव था। उनकी रचनाओं में पारिवारिक विवरण ऐसी सहृदयता से बिखरे पड़े हैं कि वे कल्पित हो ही नहीं सकते। अपने जीवन में परिवार न मिला हो, किंतु मित्रों, परिचितों के परिवारों को देखा था। गहराई से देखा था। मानो कृष्णा जी उस परिवार के सुख-दुख खुद भोग रही हों। कृष्णा सोबती के साहित्य में जीवन का पारिवारिक अभाव ही विभाव बन गया है जो विभिन्न पात्रों-स्थितियों में दिखाई देता है। मित्रो, हिंदी साहित्य की विलक्षण पात्र है। वह शरीर ही शरीर है। उसमें शारीरिकता की उद्माम भूख है और पति सरदारी लाल उसकी तुलना में ठंडा, दब्बू। कथा की रीढ़ इतनी ही है, किंतु कृष्णा जी ने इस परस्पर विरोध को लंबे-चौड़े फलक में, चार-चार भाइयों, सास-ससुर, जेठानी-देवरानी, ननद, मित्रो की कुलटा मां को विवरण संकुल परिदृश्य में घटित किया है। परिवार में चलने वाला उल्लास, हंसी-विनोद, चालाकियां, दांव-पेच, ईर्ष्या-जलन और पारिवारिक सुख के बीच मित्रो की शारीरिकता की कहानी विकसित होती है।
कहानी की कालजयिता इस बात में है कि प्रेम या पारिवारिक संबंध, पति-पत्नी का संबंध इसी शारीरिकता की जमीन पर उगता है। मित्रो शारीरिक वासना को लगभग पशु के रूप में महसूस करती है। पशुओं में संबंध नहीं होता। वे नर-मादा होते हैं, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्र नहीं होते। कमाल का शिल्प यह है कि संबंध, जो अनन्यता का भाव है, ईर्ष्या मनोविकार से पैदा होता है। मित्रो अपने पति को शराब पिला कर उसे बेसुध कर मायके के एक लंपट प्रेमी के साथ शारीरिक सुख भोगने की तैयारी करती है। किंतु उसे ध्यान आ जाता है कि पति अकेला उसकी कुलटा मां के साथ रहेगा और यही मनोविकार-अपनी मां के साथ ही ऐसा शक- अभूतपूर्व नाटकीयता से उसमें पति का संबंध जगा देता है। “यह मेरा है, मैं इसकी हूं, यह किसी और का नहीं, मैं किसी और की नहीं।” अनन्यता का यह भाव मनुष्य ने सुदीर्घ काल यात्रा में अर्जित किया है। कहानी दूसरी साहित्य विधा कही जाती है किन्तु मित्रो मरजानी महाकाव्यात्मक प्रभाव उभारती है। सिक्का बदल गया, डार से बिछुड़ी, जिंदगीनामा, दिलो-दानिश, हम हशमत और हाल में छपी उनकी आत्मकथात्मक रचना में जीवन का उच्छल प्रवाह है।
(लेखक वयोवृद्ध कवि, आलोचक, उपन्यासकार और संस्मरणकार हैं)