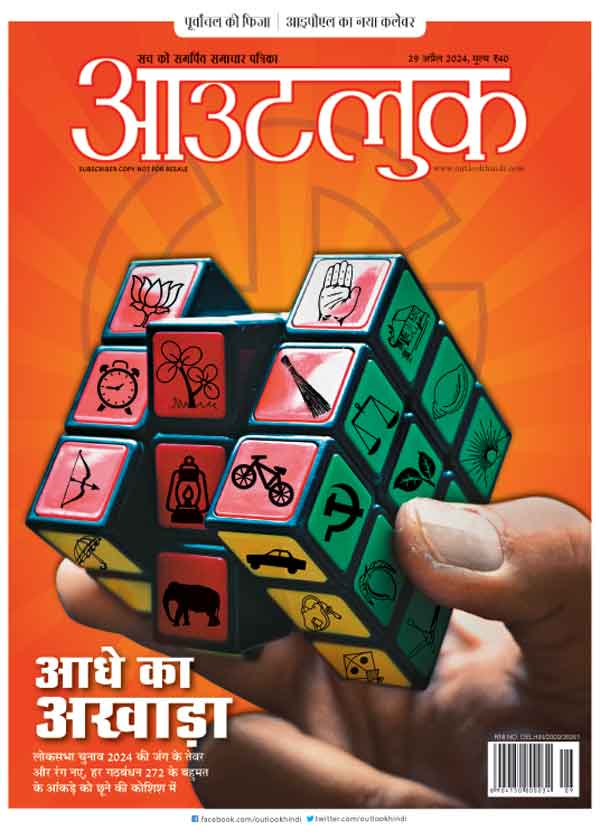रामायण और महाभारत हमारे देश के दो महाकाव्य हैं और विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीय वांग्मय और चिंतन परंपरा रामायण को काव्य और महाभारत को इतिहास मानती है। आम हिंदू इन्हें धर्मग्रंथों और पवित्र पुस्तकों का दर्जा देता है। हमारे वर्तमान शासक इन दोनों महाकाव्यों को उसी अर्थ में इतिहास मानते हैं जिस अर्थ में आज इतिहास को समझा जाता है। इन हिंदुत्ववादी शासकों की समझ लगभग हर मामले में इकहरी है और ये महाकाव्य भी इसका अपवाद नहीं। उनके बयानों से ही लग जाता है कि उनमें से अधिकांश ने इन महाकाव्यों को कभी सरसरी तौर पर भी नहीं पढ़ा। रामायण के नाम पर उनका ज्ञान अधिकांशतः तुलसीदास-कृत रामचरितमानस में वर्णित रामकथा पर आधारित है। रामकथा के उन विभिन्न रूपों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है जिन्हें देश की अन्य भाषाओं में रचा गया और जो अनेक शताब्दियों से उन भाषिक और क्षेत्रीय समुदायों के लोकजीवन का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। महाभारत के भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय अनेक संस्करण मिलते हैं। इनमें पाठांतर के अतिरिक्त संकलित सामग्री में भी अंतर देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों महाकाव्य अपने समग्र रूप में भारतीय संस्कृति की बहुलतापरक समृद्धि, जटिलता और बहुस्तरीय चरित्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अर्थ में उसके प्रतीक भी हैं।
यह एक विचित्र बात है कि उत्तर भारत में आम तौर पर लोगों को महाभारत पढ़ने के प्रति निरुत्साहित किया जाता है। आम जनता के बीच यह मान्यता है कि यदि घर में महाभारत की प्रति होगी तो परिवार में महाभारत छिड़ जाएगा। इसलिए रामचरितमानस लगभग हर घर में मिलेगा। कुछेक घरों में वाल्मीकि-कृत रामायण की प्रति भी मिल सकती है। लेकिन महाभारत की प्रति बहुत कम घरों में पाई जाती है। क्या यह इसलिए है कि जहां रामायण में चरित्रों का आदर्शीकरण और सरलीकरण किया गया है, वहीं महाभारत में प्रत्येक चरित्र धूसर, बहुरंगी और जटिल है, केवल श्वेत या श्याम नहीं? इसके अलावा महाभारत में प्रश्नाकुलता है, हर सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक मान्यता पर प्रश्नचिह्न लगाने और उसे चुनौती देने की प्रवृत्ति है और जीवन-संघर्ष की नियति की खोज है। इसमें हर बात परिवर्तनशील है, जड़ और स्थिर नहीं। इसके पहले अध्याय ‘आदिपर्व’ में ही विस्तार से इस ग्रंथ का उद्देश्य मानव जीवन के “चार पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष...” की प्रकृति का अन्वेषण बताया गया है। ये चारों पुरुषार्थ एक-दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। इनमें से किसी भी एक की शेष तीन के बिना कोई सार्थकता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मानव नियति के इस महाख्यान में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि यद्यपि धर्म ही वह नींव है जिस पर सभी मानवीय संबंध टिके हुए हैं, लेकिन इन चारों में प्राथमिकता केवल काम को प्राप्त है। यहां काम का अर्थ यौनेच्छा नहीं, व्यापक अर्थ में वासना यानी इच्छा है जो प्रत्येक मानवीय कर्म में अंतर्भुक्त है। काम को अनिवार्यतः धर्म पर आधारित होना चाहिए क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात सभी वासनाओं से मुक्ति है। सभी इच्छाओं की पूर्ति धर्मानुसार की जानी चाहिए, वरना अधर्म का बोलबाला होगा जो अंततः विनाश की ओर ले जाएगा।
यह धर्म क्या है? प्रसिद्ध दर्शनवेत्ता बिमल कृष्ण मतिलाल ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारतीय परंपरा, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराएं शामिल हैं, में हजारों साल तक हुए धर्मचिंतन में ईश्वरीय सत्ता को विशेष महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि धर्म और रिलिजन में तात्विक भेद है। धर्मचिंतन का लक्ष्य विवेकपूर्ण आधार पर मानव व्यवहार को निर्धारित और नियमित करना रहा है। और जब धर्म है तो उसके साथ धर्मसंकट यानी दुविधा या अनिश्चय भी जुड़ा है जिसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे किंकर्तव्यविमूढ़ता, धर्मविकल्प, कृत्याकृत्य-विवेक-निर्णय आदि। इसी के साथ यह सच्चाई भी जुड़ी है कि धर्म-अधर्म का ज्ञान होने से ही धर्मानुसार आचरण सुनिश्चित नहीं हो जाता। महाभारत में स्वयं दुर्योधन ने स्वीकार किया है, “जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः।। जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।।” (ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं जानता, लेकिन जानने के बावजूद उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि मैं अधर्म को नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती।) महाभारत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधर्म के परिणाम से किसी को भी मुक्ति नहीं है। जब जीवन में कभी असत्य-भाषण न करने वाले युधिष्ठिर ने, भले ही अनिच्छा के साथ लेकिन जानते-बूझते हुए “अश्वत्थामा हतो हतः” कहकर झूठ बोला, तो सदा भूमि से कुछ अंगुल ऊपर रहकर चलने वाला उनका रथ तत्काल नीचे गिरकर अन्य रथों के स्तर पर आ गया। मनुष्य को आईना दिखाने वाला ऐसा महाभारत कोई भला क्यों पढ़े?
इसी महाभारत में केवल द्रौपदी ही एकमात्र स्त्री है जिसे मनस्विनी कहा गया है। यही मनस्विनी जब कौरव राजसभा में बैठे विदुर और भीष्म जैसे धर्मज्ञों से पूछती है कि क्या स्वयं को हार जाने के बाद युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना धर्मसम्मत था, तो भीष्म “धर्म की गति अति सूक्ष्म है” कहकर कोई राय व्यक्त करने से बचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि संस्कृतज्ञ राधावल्लभ त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है, यह पूरा प्रसंग न्यायालय में होने वाली बहस जैसा है। इसे पढ़कर क्या आज के भारत की न्यायपालिका याद नहीं आ जाती? क्या आज के हमारे सोली सोराबजी और फली नरीमन विदुर और भीष्म से भिन्न दीखते हैं?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और कला-संस्कृति पर लिखते हैं)