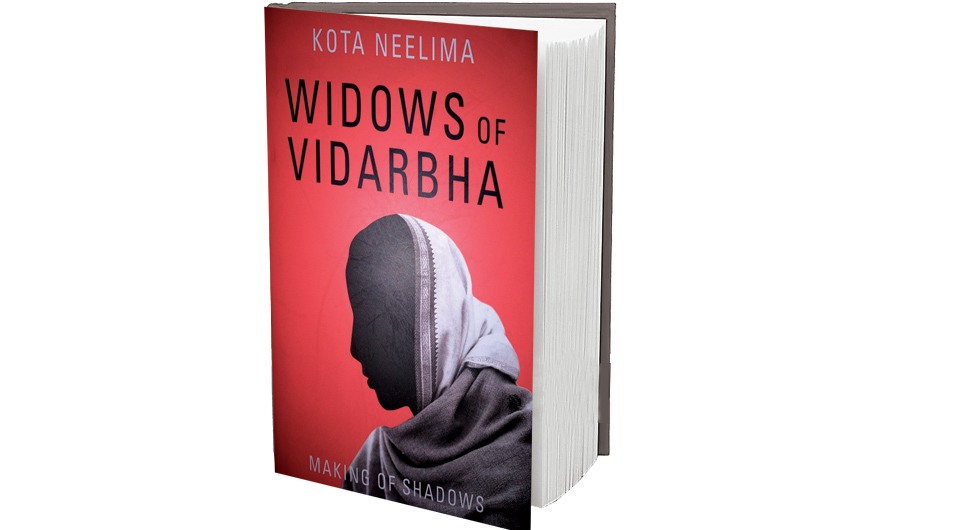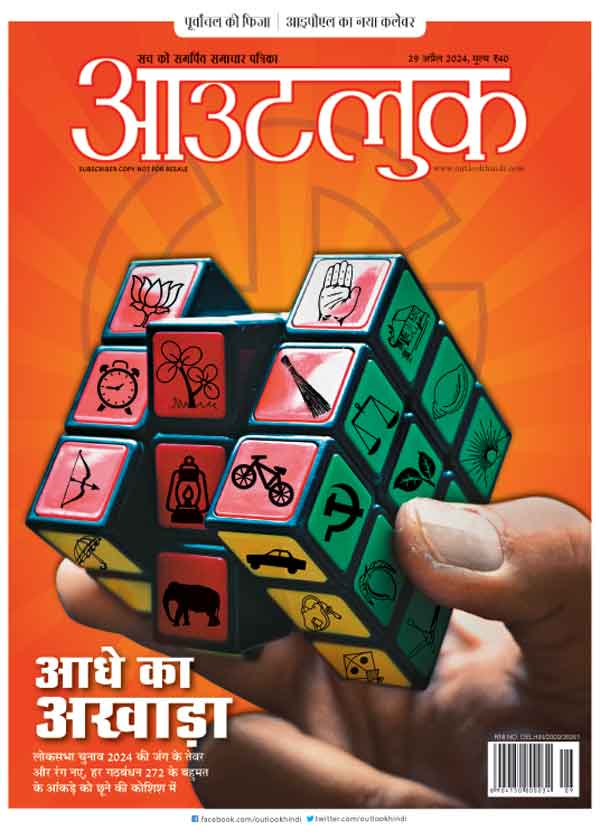अखबार पत्रिकाएं किसानों की आत्महत्याओं पर फोकस करती रहती हैं। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या ऐसा राजनीतिक मसला है, जो जाने कितने चुनावों में इस्तेमाल हुआ है। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या के आर्थिक संदर्भ हैं। सामाजिक संदर्भों की तरफ ध्यान कम पत्रकारों और लेखकों का जाता है। विडोज ऑफ विदर्भ - मेकिंग ऑफ शैडोज किताब लिखी है कोटा नीलिमा ने। इस किताब में विदर्भ के किसानों की आत्महत्याओं को देखने-समझने की कोशिश की गई है।
किसानों की आत्महत्या लगातार चुनावी चर्चा का विषय बनती है। खासकर महाराष्ट्र में यह सदाबहार मुद्दा है। पुस्तक में एक तालिका दी गई है, जिसमें 2001 से 2013 तक की किसान आत्महत्याओं के आंकड़े दिए गए हैं। पैंतालीस हजार से ऊपर आत्महत्याओं के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है। इस सूची में आश्चर्य यह है कि केरल जैसा छोटा राज्य छठे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल सातवें नंबर पर। केरल और बंगाल में वामपंथी प्रभाव जबरदस्त रहा है। वामपंथ का केंद्र मजदूरों और किसानों के लिए काम रहा है, फिर केरल और बंगाल का इस सूची में होना गहरे प्रश्न उठाता है। अगर वाम चेतना से लैस राज्यों में ही किसानों के जीवन की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि किसानों की आत्महत्याओं से जुड़े मसले खासे जटिल हैं और उन पर लगातार और गंभीर काम किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसान आत्महत्याओं के मामले में नवें नंबर पर है। दस की सूची में गुजरात सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश में भी किसान गरीब हैं, पर यहां आत्महत्याएं वैसी नहीं हैं, जैसी महाराष्ट्र में हैं। किसानों की आत्महत्याओं के मामले में टॉप पांच राज्य (2001-2013) में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहे हैं।
किसान आत्महत्या कर लेते हैं, खबर बन जाते हैं पर उनके जाने के बाद उनके परिवारों का संघर्ष खासकर उनकी विधवाओं का संघर्ष खबर नहीं बनता। कोटा नीलिमा ने विदर्भ की विधवाओं के जीवन संघर्ष पर लिखा है। इससे यह साफ होता है कि किसानों की आत्महत्या का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि परिवार का मुख्य कमाऊ व्यक्ति चला गया। भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति को लेकर भी यह किताब कई मुद्दे रेखांकित करती है।
पेज 16 पर कोटा नीलिमा जो लिखती हैं उसका आशय यह है कि वंदना राठौड़ जो 22 अगस्त 2013 को विधवा हुई थीं, को बच्चों के भविष्य की चिंता है। पर, उनके पास कोई योजना नहीं है। कोई सपने नहीं हैं। कुछ ऐसा नहीं है, जिसके बारे में सोचा जा सके।
किताब पढ़कर कोई शहरी स्तब्ध रह सकता है कि जितनी रकम में बढ़िया एप्पल फोन आता है उसकी आधी रकम के कर्ज के लिए किसान आत्महत्या कर लेता है। पेज 106 में दर्ज है कि गणेश सावनकर पचास हजार का कर्ज बैंक को वापस करने में असमर्थ था और निजी साहूकारों का कुछ कर्ज भी था उसके ऊपर। गणेश सावनकर की विधवा जयश्री ने बताया कि जिन कर्जों की वजह से उनके पति ने आत्महत्या की, उन्हीं कर्जों की अदायगी की मांग निजी साहूकारों ने उनसे की। उनके पास पैसे ही नहीं थे कर्ज की वापसी के लिए। जयश्री आगे जो बताती हैं, उसका आशय है कि पुरुष डर कर आत्महत्या कर लेते हैं, महिलाएं हिम्मती होती हैं, हर हाल में लड़ती हैं। वैसे यह बात सोचने की है कि आत्महत्याओं की खबरें पुरुष किसानों की ही आती हैं। महिला किसान, महिला मजदूर कितनी भी संकट में फंसी हों, आत्महत्या का रास्ता चुनती दिखाई नहीं पड़तीं। सरकार की तरफ से आत्महत्या का मुआवजा जैसा कुछ करीब एक लाख रुपये मिलने की बात किताब में दर्ज है। यह तथ्य भी यहां दर्ज किया जा सकता है कि एप्पल का महंगा फोन भी करीब इतने ही रुपये में आता है। एक ही अर्थव्यवस्था में कितनी समानांतर दुनियाएं चल रही हैं। किसान जान देता है, तो लाख रुपये उसका परिवार पा जाता है, उतनी ही रकम में कोई एक एप्पल फोन एक दो साल इस्तेमाल करने के लिए खरीद लेता है।
किसान आत्महत्या कर लेता है फिर परिवार की बेबसी शुरू हो जाती है। पेज 125 में एक विधवा ज्योति भूंबार कहती हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकतीं। इंग्लिश स्कूल में पढ़ा नहीं सकतीं। एक किसान के बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल बहुत महंगे हैं। बतौर मजदूर काम करने वाली ज्योति कहती हैं, “मैं अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ करती हूं, फिर भी मेरे बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित नहीं है।” विधवाओं के प्रति समाज उदार नहीं है। विधवाओं को मिलने वाले मुआवजे पर परिवार के दूसरे सदस्यों की नजर रहती है। कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययन होने चाहिए, जिनसे साफ हो पाए कि किसान पति की आत्महत्या के बाद उनकी विधवाओं के साथ समाज सलूक कैसा करता है। विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं के मसलों का राजनीतिक और आर्थिक अध्ययन तो हुआ है पर, उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन होना बाकी है।
हाल में मुंबई में किसानों ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। कर्जमाफी की मांग उनकी मांगों में शामिल थी। कर्जमाफी की मांग को स्वीकार कर लेना कुल मिलाकर ऐसा है, जैसे गंभीर चोट के दर्द से निपटने के लिए किसी को दर्द निवारक दवा दे दी जाए। इससे दर्द चला जाता है फौरी तौर पर, पर दर्द की वजहें नहीं जातीं। किसान की मूल समस्या है कि उसकी लागत लगातार बढ़ती जाती है, वह उसके नियंत्रण में नहीं है। पर उसे मिलने वाली कीमत पर बाजार का, सरकार का नियंत्रण है। सरकारें कृषि उत्पादों की कीमतों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, ये एक हद से ऊपर चली गईं, तो दूसरी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। किसान को मिलने वाली कीमत पर नियंत्रण है, किसान को पड़ने वाली लागत पर कोई नियंत्रण नहीं है। खेती घाटे का सौदा बन रही है। घाटे की पूर्ति छोटा किसान कर्ज से करता है, वह कई बार जानलेवा बन जाता है।
यह किताब हर आर्थिक पत्रकार को पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समानांतर अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। एक अर्थव्यवस्था वह है जहां एक लाख रुपये के कर्ज के लिए जान चली जाती है और एक अर्थव्यवस्था वह है जहां लाखों की मोटरसाइकिल खरीदने वालों की लाइन लगी है।