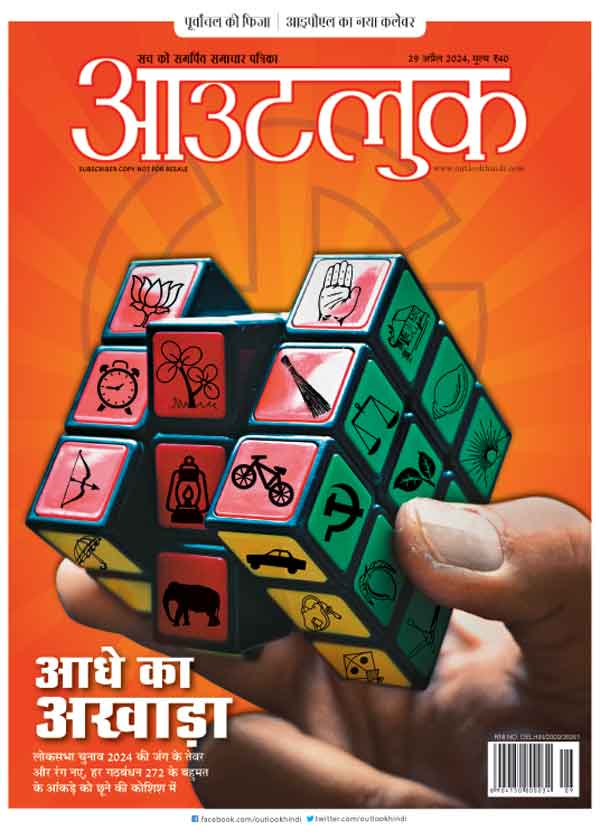पिछले साल मिली असलफता के बावजूद रूपक शरर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ‘प्रेमक बसात’ कमाई के मामले में भले ही फिसड्डी रही लेकिन यह परिणाम भी उन्हें अपनी मातृ भाषा को पुनर्जीवित करने के मिशन से डिगा नहीं पाया। रूपक ने इसी फिल्म से अपनी निर्देशकीय पारी की शुरुआत की थी। लंबे समय बाद आई मैथिली फिल्म में अपने श्रम को दिखाने के लिए रूपक गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक अलग-अलग शहरों में मैथिली फिल्मों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित करते हैं।
वह क्या है जो शरर जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा में फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिस भाषा का कभी भी फलता-फूलता फिल्म उद्योग नहीं रहा और इसका व्यावसायिक रिटर्न भी कुछ नहीं है? ऐसा कहा जा सकता है शायद, अपनी भाषा में कहानियां सुनाने का जुनून। शरर ने आउटलुक से कहा, “जहां भी मैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करता हूं, दर्शकों को आश्वस्त करता हूं कि मैं तब तक विराम नहीं लूंगा जब तक मैथिली सिनेमा को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर दूंगा। मुझे मैथिली भाषी लोगों का समर्थन चाहिए।”
43 साल के निर्देशक मैथिली सिनेमा की किस्मत में बदलाव के बारे में आश्वस्त हैं। लेकिन तथ्य अलग हैं। 1960 के दशक की शुरुआत के बावजूद सिनेमा में मैथिली की जड़ें नहीं जम पाईं। मैथिली संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा है और 2011 की जनगणना के अनुसार 1.35 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा (नेपाल को छोड़कर वहां यह दूसरी आधिकारिक भाषा है) बोली जाती है। यहां तक कि 2016 में बनी नीतू चंद्रा की फिल्म मैथिली मखान भी उद्योग को पुनर्जीवित करने में विफल रही। यह हाल तब है जब इस फिल्म को मैथिली भाषा का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नीतू चंद्रा के भाई नितिन चंद्रा द्वारा निर्देशित और बिहार के मिथिलांचल में ही फिल्माई गई यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में प्रदर्शन की बाट जोह रही है।
फिर भी, भावुक फिल्म निर्माताओं का एक समूह वहां जा रहा है जहां अधिकांश लोग कदम रखने से डरते हैं। ‘प्रेमक बसात’ अब तक की सबसे महंगी मैथिली फिल्म थी जिसके निर्माता मुंबई के कपड़ा व्यापारी वेदांत झा थे। शरर कहते हैं, “मैंने अपने निर्माता को आगाह किया था कि मैथिली फिल्म में पैसा लगाना जुए की तरह है और उन्हें पैसे डूबने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने को कहा।” ऐसे युग में जब मल्टीप्लेक्स में छोटे बजट की हिंदी फिल्मों के लिए भी स्क्रीन मिलना मुश्किल है, ऐसे में क्षेत्रीय फिल्म निर्माता इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि एक उदार निवेशक की तलाश कर सकें। मुख्य रूप से बिहार में 1.27 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली मगही बोली में ‘देवन मिसिर’ फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा था। 1965 के बाद बनी यह पहली मगही फिल्म थी जो सिनेमाघरों में आई। ‘देवन मिसिर’ के प्रचार में कहा गया, ‘जुगन बाद पहली बार’ (सालों बाद पहली बार।)
मिथिलेश ने आउटलुक को बताया कि मगध के बुद्धिमान दिग्गज देवन मिसिर के जीवन पर बनी मगही बोली की ये केवल तीसरी फिल्म है। वह बताते हैं, “कम लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध फिल्मकार फणी मजूमदार (जिन्होंने 1965 में मैथिली में कन्यादान भी बनाई थी) पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1960 की शुरुआत में भैया नाम से मगही में फिल्म बनाई थी। उस फिल्म के करीब पांच दशक बाद ‘देवन मिसिर’ सिनेमाघरों में आई है।”
बिहार के थिएटर दिग्गज मिथिलेश कहते हैं कि कि उन्होंने मूल रूप से एक टीवी धारावाहिक के लिए पटकथा लिखी थी, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर सके। वह कहते हैं, “बाद में मैंने इसे नाटक के रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन जहां भी मैं यह नाटक करता, लोग मुझे इसे दोहराने के लिए कहते। इससे मुझे फिल्म बनाने का विचार आया।” राज्य सरकार के समर्थन के बिना, उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। वह कहते हैं, “बिना किसी बड़े क्षेत्रीय सितारे के ‘देवन मिसिर’ ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की।” हालांकि बड़े पैमाने पर इस फिल्म को भी रिलीज का इंतजार है।
क्षेत्रीय सिनेमा देखने वालों का मानना है कि मैथिली और मगही फिल्म उद्योग तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को नियमित रूप से भोजपुरी फिल्मों की तरह मौका नहीं दिया जाता है। शरर कहते हैं, “सस्ता जिनगी महग सेनूर 1999 की बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन इसके बाद कोई भी मैथिली फिल्म इस सफलता को नहीं दोहरा पाई। गया में देवन मिसिर हाउस फुल चल रही थी लेकिन एक बड़ी भोजपुरी फिल्म के लिए इसे सिनेमाघर से उतार लिया गया। लेकिन दो ही दिन बाद स्थानीय लोगों ने मालिक पर दबाव डाला कि देवन मिसिर को ही दोबारा सिनेमाघरों में चलाया जाए।”
यह अपवाद हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में किसी भी अनुभवहीन फिल्मी उद्योग के लिए बॉक्स ऑफिस पर सिक्के बरसाने वाले लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन जब से जोश से भरे फिल्मकार भाषा की परवाह किए बिना अपनी रचनात्मकता को सामने लाना चाहते हैं तब से कमर्शियल सफलता कोई बाधा नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली फिल्मकार प्रवीण मोरछले ने ‘वॉकिंग विद द विंड’ बनाने के लिए लद्दाख का चुनाव किया जिसे 2018 में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तब से इस फिल्म ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की यात्रा की और कई पुरस्कार जीते। जिनमें गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में यूनेस्को गांधी पदक और कोलंबो में सार्क फिल्म महोत्सव में निर्देशन और कहानी के लिए एक विशेष जूरी पुरस्कार शामिल है।
चूंकि ‘वॉकिंग विद द विंड’ 10 साल के एक पहाड़ी लड़के के बारे में है इसलिए प्रवीण ने इसे लद्दाख में फिल्माने का निर्णय लिया। हालांकि वे खुद यहां की स्थानीय भाषा नहीं जानते। आउटलुक से बात करते हुए वह कहते हैं, “मेरा ऑब्जर्वेशन मेरी प्रेरणा है जो मेरी कहानियों का आधार भी। मैं वास्तविक लोगों को देखता हूं और उनका जीवन मेरे मन में कई कहानियां उत्पन्न करता है। वॉकिंग विद द विंड ऐसी ही फिल्म है।”
एक अनौखा प्रयास
देर से ही सही लेकिन प्रवीण जैसे निडर फिल्म निर्माताओं की कोई कमी नहीं हुई है, जो उन क्षेत्रों में जाकर फिल्म बनाने के लिए लंबी यात्राएं करने से भी गुरेज नहीं कर रहे जहां ये विविध भाषाएं बोली जाती हैं। रिधम जानवे को ही लीजिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चरवाहों द्वारा बोली जाने वाली गड्डी बोली फिल्म बनाई। फिल्मकार के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए, ‘द गोल्ड-लादेन शिप एंड द सेक्रेड माउंटेन’ जैसी शानदार फिल्म बनाकर वो चर्चा में आए। यह फिल्म एक बूढ़े चरवाहे के बारे में है जो अपने भेड़ों के झुंड को सिर्फ इसलिए बेसहारा छोड़ देता है ताकि हिमालय में दुर्घटनाग्रस्त एक विमान के पायलट को खोजा जा सके। रिधम कहते हैं, “मैंने कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए और मुझे लगा उनकी बोली पर एक फिल्म बनाना चाहिए। मैंने तय किया, इसके लिए किसी व्यवसायिक अभिनेता को नहीं लूंगा बल्कि स्थानीय लोगों से ही काम कराऊंगा।”
इसका परिणाम शानदार रहा। इसमें कलाकारों का शानदार काम और अप्रतिम दृश्य थे। ठीक इसी तरह एक और नवोदित निर्देशक शरीफ एसा जिन्होंने केरल के वायनाय में रहने वाले अड़िया समुदाय की बोली रवुला में ‘कंठा: द लवर ऑफ कलर’ बनाई। उस साल इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राज्य पुरस्कार मिला।
धीरे-धीरे ऐसे फिल्मकारों की जमात बढ़ रही है। पिछले साल लक्ष्यद्वीप में बोली जाने वाली मलयालम की एक बोली जसारी में बनी संदीप पंपली की सिंजर और तुलु बोली में अभया सिम्हा की पद्दाई ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। इस साल लद्दाखी में प्रिया रामसुब्बन की ‘चुस्किट’ और अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा शेरडुपकिन में बनी बॉबी सरमा बरुआ की ‘मिशिंग द एपरिशन’ ने अच्छा प्रभाव डाला था। हालांकि दोनों ही फिल्में शायद थियेटरों में रिलीज न हो सकीं।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, आलोचक और निर्देशक उत्पल बोरपुजारी कहते हैं कि इसका व्यावसायिक पहलू नहीं है, बल्कि अपनी-अपनी भाषाओं में कहानी कहने का आग्रह है जो इन फिल्मकारों को प्रेरित करता है। वह कहते हैं, “किसी भी मामले में, जब आप किसी विशेष समुदाय के बारे में एक कहानी बता रहे हैं, तो यह अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह से कही जा सकती है। इससे सांस्कृतिक और सामाजिक बारीकियों को भी ज्यादा अच्छे ढंग से पकड़ा जा सकता है।”
सामाजिक बुराई डायन प्रथा पर पर बनी फिल्म ईशू (2017) को खूब सराहना मिली थी। यह फिल्म बोरपुजारी ने बनाई थी। एक बच्चा इस घटना को कैसे देखता है, इसे बोरपुजारी ने फिल्म में दिखाया है। यानी यह एक बच्चे के नजरिए से बनी फिल्म है। उनका कहना है कि इन फिल्मों की थिएटर रिलीज असंभव है क्योंकि इनका दर्शक वर्ग बहुत छोटा है। वह कहते हैं, “अरुणाचल प्रदेश की जातीय भाषा में कई फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन इस तरह की फिल्में शायद ही ईटानगर में भी दर्शकों को आकर्षित करें क्योंकि कम ही लोग विभिन्न जनजातीय भाषाओं को समझ पाएंगे।” बोरपुजारी के अनुसार उम्मीद की एकमात्र किरण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वह कहते हैं, “ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऐसी फिल्मों के लिए वैश्विक दर्शक प्रदान कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एक फिल्म निर्माता के लिए उन प्लेटफार्मों पर एक फिल्म कितनी कमाई करेगी, लेकिन अपनी भाषाओं में कहानी कहना उनकी प्रमुख प्रेरणा बनी रहेगी।”