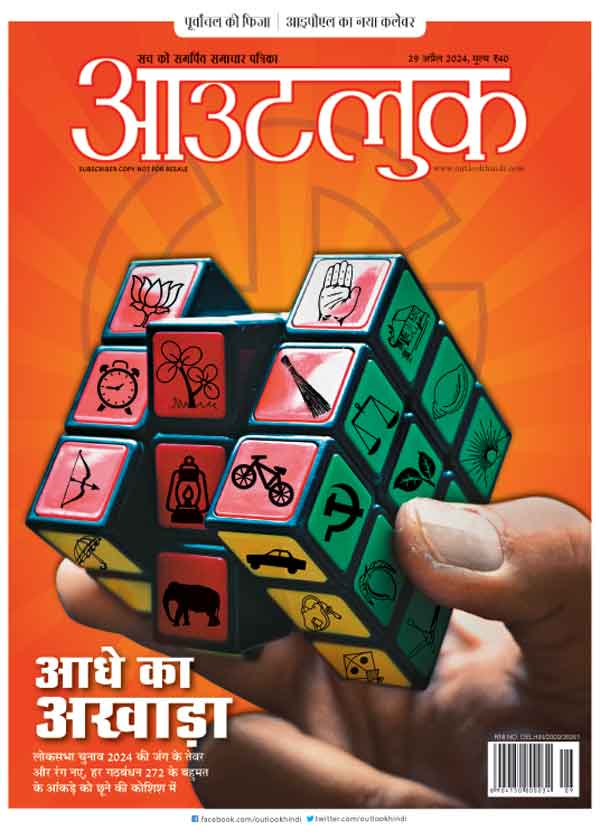ताकि संविधान और देश के मौलिक विचारों और लोगों के बुनियादी अधिकारों पर आघात के प्रति सचेत रहें
अगर कोई पूछे कि इस गणतंत्र दिवस पर, 70 से ज्यादा उम्र के गणतंत्र का क्या हाल है, तो हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस उसे सड़क का रास्ता बता देना है। सारा देश सड़कों पर है, जिसे स्कूलों-कॉलेजों में होना चाहिए था, बाजारों और दूकानों में, घरों और दफ्तरों में होना चाहिए था, वह अगर सड़कों पर उतर आए तो समझ लेना चाहिए कि देश की गाड़ी पटरी से उतर रही है। जिस नागरिक ने देश को गुलामी से मुक्त किया, अपने देश का अपना लोकतंत्र बनाया, इस और ऐसी कितनी ही सरकारों को बनाया-मिटाया, आज उसी नागरिक से, उसकी ही बनाई सरकार उसकी वैधता पूछ रही है और उसे अवैध घोषित करने का कानून बना कर इतरा रही है। कोई कहे कि नौकरों (प्रधानसेवक!) ने मालिक तय करने का अधिकार ले लिया है, तो गलत नहीं होगा। जब सरकार संविधान से मुंह फेर लेती है; विधायिका विधान से नहीं, संख्याबल से मनमाना करने लगती है; नौकरशाही जी-हुजूरों की फौज में बदल जाती है और न्यायपालिका न्याय का पालन करने और करवाने के अलावा दूसरा सब कुछ करने लगती है, तब देश पटरी से उतर जाता है।
हमने जिस सरकार को देश के लिए चुना था, उसने देश को दल में बदल लिया है और हमने लोकसभा में उसे जो बहुमत दिया था, उसे उसने मनमाना करने का लाइसेंस मान लिया है। वह भूल गई है कि नागरिक उससे नहीं हैं, वह नागरिकों से है। नागरिक उसे जब चाहे तब बदल सकता है; वह चाहे तो भी नागरिक को बदल नहीं सकती है।
नागरिकता की एक परिकल्पना और उसका आधार हमारे संविधान ने हमें दिया है कि जो भारत में जनमा है वह इस देश का नागरिक है। फिर उसी संविधान ने यह भी कहा कि कोई जनमा कहीं भी हो, यदि वह इस देश की नागरिकता का आवेदन करता है और संविधानसम्मत किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है, तो सरकार उसे नागरिकता देगी. ऐसा करते समय सरकार न लिंग का भेद कर सकती है, न धर्म या जाति का, न रंग या रेस या देश का। नागरिकता अनुल्लंघनीय है, नागरिक स्वयंभू है। सरकार को याद कराना जरूरी है कि उसने नागरिक प्रमाणित करने का जो अधिकार लपक लिया है, वह लोकतंत्र, संविधान, राजनैतिक नैतिकता और सामाजिक जिम्मेवारी के खिलाफ जाता है।
इतिहास में उतरें हम तो 1925 से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से, एक सीधी और साफ धारा मिलती है, जो हिंदुत्व का अपना ही नया दर्शन बनाती है और दावा करती है कि देश धर्मों से बनते हैं और इसलिए वह हिंदू बहुमत के इस देश को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेगी। विनायक दामोदर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर आदि से प्रेरित और उनके द्वारा ही संगठित-संचालित हिंदुत्व के इस दर्शन को सबसे पहला और सबसे बड़ा समर्थन मिलता है मुस्लिम लीग से। सावरकर-जिन्ना धर्म आधारित राष्ट्र के इस मंच पर एक साथ खड़े मिलते हैं। इन दोनों की इस सांप्रदायिक सोच को, उसके जन्म से लगातार ही महात्मा गांधी से सबसे बड़ी चुनौती मिलती रही।
गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के सेनापति भर नहीं थे, भारतीय समाज के नए दार्शनिक भी थे। वे खुद को हिंदू कहते थे, सनातनी हिंदू! लेकिन हिंदुत्व के संघ-परिवारी दर्शन के किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते थे। गांधी को सीधी चुनौती देकर, साथ लेने की बनावटी मुद्राएं धरकर और फिर छल की सारी कोशिशों के बाद भी जब गांधी हाथ नहीं आए और भारतीय जनमानस पर उनके बढ़ते असर की काट ये नहीं खोज पाए तब जाकर यह तय किया गया कि उन्हें रास्ते से हटाया जाए। यही वह फैसला था, जो पांच विफल कोशिशों के बाद, 30 जनवरी 1948 को सफल हुआ और गांधी की हत्या हुई। योजना यह थी कि हत्या से देश में ऐसी अफरा-तफरी मचेगी, मचाई जाएगी कि जिसकी आड़ में हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेंगी।
हिंदुत्व की इनकी अवधारणा तानाशाही की है और इसलिए वह सत्ता की बैसाखी के बगैर चल ही नहीं पाती है। सत्ता इनके लिए अस्तित्व का सवाल है। हत्या तो कर दी गई लेकिन देश में वैसी अफरा-तफरी नहीं मची कि जिसकी आड़ लेकर ये सत्ता तक पहुंचें। गांधी का रचा राष्ट्र-मन, जवाहरलाल और सरदार की दृढ़ एकाग्रता ने देश को अफरा-तफरी से बचा भी लिया और निकाल भी लिया। इसलिए सरदार की आड़ में नेहरू इनके निशाने पर थे और हैं। तब से आज तक हिंदुत्व का यह दर्शन समाज में न वैसी जगह बना सका जिसकी अपेक्षा से ये काम करते रहे और न सत्ता पर इनकी कभी ऐसी पकड़ बन सकी कि ये अपने एजेंडे का भारत बना सकें। अटल बिहारी वाजपेयी के पांच साल के प्रधानमंत्रित्व-काल में यह हो सकता था लेकिन अटल जी ‘छोटे-नेहरू’ का चोला उतारने को तैयार नहीं थे। वे संघी हिंदुत्व की मदद तो लेते थे लेकिन उसके खतरों से बचते भी थे। इसलिए अटल-दौर संघी हिंदुत्व की सत्ता का नहीं, जमीन तैयार करने का दौर बना और उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला नरेंद्र मोदी के गुजरात में खोली गई। सत्ता की मदद से हिंदुत्व की जड़ जमाने का वह प्रयोग संघ और मोदी, दोनों के लिए खासा सफल रहा। दोनों की आंखें खुलीं।
फिर कांग्रेस के चौतरफा निकम्मेपन की वजह से दिल्ली नरेंद्र मोदी के हाथ आई। तब से आज तक दिल्ली से हिंदुत्व का वही एजेंडा चलाया जा रहा है जो 1925 से अधूरा पड़ा था। यह गांधी को खारिज कर, भारत को अ-भारत बनाने का एजेंडा है। अब ये यह भी जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये अपना वह एजेंडा पूरा करने में तेजी से जुट गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक उलट-फेर की संभावनाएं खत्म हों और सत्ता अपने हाथ में स्थिर रहे। नोटबंदी से लेकर राष्ट्रीय नागरिकता बंदी तक सारा खेल समाज की ताकत को तोड़ देने, संविधान को अप्रभावी बना देने तथा संवैधानिक संस्थानों को सरकार का खोखला खिलौना बनाने के अलावा कुछ दूसरा नहीं है।
आज कांग्रेस अपनी ही छाया से लड़ती, लड़खड़ाती ऐसी पार्टी मात्र है जिसका राजनैतिक एजेंडा मोदी तय करते हैं। विपक्ष के दूसरे सारे दल सत्ता की बंदरबांट में हिस्सा लपक लेने से ज्यादा की न हैसियत रखते हैं, न सपने पालते हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र का विपक्ष कहां है? वह संसद में नहीं, सड़कों पर है। आज युवा और नागरिक ही भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष हैं।
सड़कों पर उतरे युवाओं-छात्रों-नागरिकों में सभी जातियों-धर्मों के लोग हैं। सीएए किसी भी तरह मुसलमानों का सवाल नहीं है। वे निशाने पर सबसे पहले आए हैं, क्योंकि दूसरे असहमतों को निशाने पर लेने की भूमिका बनाई जा रही है। इसलिए लाठी-गोली-अांसू गैस की मार के बीच भी सड़कों से आवाज यही उठ रही है कि हम पूरे हिंदुस्तान को, और इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को सम्मान और अधिकार के साथ भारत का नागरिक मानते हैं। कोई भी सरकार हमारी या उनकी या किसी की नागरिकता का निर्धारण करे, यह हमें मंजूर नहीं है। इसलिए कि सभी सरकारें जिस संविधान की अस्थाई रचना हैं, जनता उस संविधान की रचयिता भी है और स्थाई प्रहरी भी!
सरकारें स्वार्थ, भ्रष्ट और संकीर्ण मानसिकता वाली हो सकती हैं। सांप्रदायिक भी हो सकती हैं और जातिवादी भी! सरकारें मौकापरस्त भी होती हैं और रंग भी बदलती हैं। यह संविधान से बनती तो है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं करती है; यह वोट से बनती है लेकिन वोटर का मखौल उड़ाती है। यह झूठ और मक्कारी को हथियार बनाती है और इतिहास को तोड़-मरोड़ कर मतलब साधना चाहती है। आज यह हमारी नागरिकता से खेलना चाह रही है, कल हमसे खेलेगी। यह चाहती है कि इस देश में नागरिक नहीं, सिर्फ उसके वोटर रहें। सत्ता के खेल में यह समाज को खोखला बना देना चाहती है। इसलिए लड़ाई सड़कों पर है। जब संसद गूंगी और व्यवस्था अंधी हो जाती है, तब सड़कें लड़ाई का मैदान बन जाती हैं।
इसे पहचाना है हमारी न्यायपालिका के प्रमुख एस.ए. बोबडे साहब ने। किन्हीं वकील पुनीत कुमार ढांढा की याचिका थी कि अदालत सीएए को संवैधानिक घोषित करे और उसके खिलाफ चल रहे सारे आंदोलन को असंवैधानिक घोषित करे। न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और सूर्यकांत की तरफ से इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अदालत से ऐसी कोई मांग सुन रहा हूं कि वह संसद द्वारा पारित किसी कानून को संवैधानिक करार दे। सभी जानते हैं कि संसद द्वारा पारित हर कानून संवैधानिक होता है। अदालत का काम यह देखना मात्र है कि जो पारित हुआ है वह कानूनसम्मत है या नहीं। देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसी याचिकाओं से इसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ऐसी और इतनी व्यापक हिंसा फैली हुई है कि सबसे पहले देशव्यापी शांति का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सीएए की वैधता पर विचार किया जा सके।
अदालत ने जो कहा, वह सही ही कहा लेकिन अधूरा कहा। आधी या अधूरी बात न न्याय के हित में होती है, न समाज के। देश में हिंसा की यह जो आग भड़की है और दावानल की तरह फैल रही है, वह सामाजिक आग है जो अकारण न तो लगती है और न बेवजह फैलती है। यह योजनापूर्वक भड़काई गई है और जिसके दावानल बनते जाने में किसी को अपना राजनैतिक फायदा दीख रहा है। इसलिए इसे बुझाने की जगह इसके खिलाफ एक दूसरी हिंसा खड़ी की जा रही है। सड़क पर घबराई-डरी और भटकाई भीड़ की हिंसा, जो हिंसा नहीं बल्कि छूंछे क्रोध में की जा रही तोड़-फोड़ भर है, के सामने आप राज्य द्वारा नियंत्रित और संचालित हिंसा को खड़ा करते हैं तो यह आग में घी डालने से कम बड़ा अपराध नहीं है। यह अलोकतांत्रिक भी है, अनैतिक भी और असंवैधानिक भी।
उन्मत्त भीड़ की दिशाहीन तोड़-फोड़ और राज्य की प्रायोजित कुटिल हिंसा को एक ही पलड़े पर रख कर नहीं तोला जा सकता है। हिंसा गलत है, बुराई की जनक है और घुन की तरह आदमी को भी और उसके समाज को भी खोखला कर जाती है। इसलिए उसका समर्थन कोई भी साबुत दिमाग आदमी कैसे कर सकता है? लेकिन हिंसा और हिंसा के बीच फर्क करने का विवेक हम कैसे खो सकते हैं? चूहे को अपने फौलादी जबड़े में दबोच कर, झिंझोड़ती बिल्ली की हिंसा और अवश चूहे द्वारा पलट कर उसे काटने वाली हिंसा में फर्क तो महात्मा गांधी भी करते हैं।
महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब दूसरा कोई विकल्प न हो सामने, तो कायरता और हिंसा में से मैं हिंसा को चुनूंगा। इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि महात्मा गांधी हिंसा की वकालत कर रहे थे? नहीं, वे हिंसा और हिंसा के बीच के फर्क को रेखांकित कर रहे थे। हमारी अदालत को भी हिंसा की इस आग पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले यह फर्क समझना सीखना होगा और हिंसा के जनकों को संविधान का आईना दिखाना होगा।
समाज हिंसा की तरफ तब जाता है जब उसका विश्वास टूटता है; और चौतरफा हिंसा और अराजकता तब छाती है, जब समाज चौतरफा विश्वासघात से घिर जाता है। आज राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में जैसा पतन हम देख रहे हैं, गुंडों-बटमारों-सांप्रदायिकों-कुशिक्षितों की आज जैसी बन आई है, वह सब इसी चौतरफा भरोसाहीनता का परिणाम है। लोकतंत्र का यह कूड़ाघर आज का नहीं, पुराने समय से जमा होता रहा है। आज के सत्ताधारियों ने इसे चरम पर पहुंचा दिया है। हिंसा और क्षोभ का यह माहौल देश को ही ले डूबे इससे पहले हिंसा के जनक कौन हैं, इसकी पहचान कर लेना जरूरी है।
वह न्यायपालिका हिंसा की जनक है जो समय पर हस्तक्षेप कर, किसी भी सरकार या संवैधानिक संस्थान को उसकी मर्यादा से बाहर जाने से रोकती नहीं है। हमारे संविधान ने ऐसी अत्यांतिक परिस्थिति के लिए अपने संस्थानों को ऐसी विशेष शक्तियां दे रखी हैं, जिनसे वे एक-दूसरे का पतन रोक सकती हैं। हमारी बेहतरीन संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही नहीं, दूसरे संवैधानिक संस्थान भी अपने-अपने दायरे में स्वयंभू-से हैं, लेकिन संविधान ने उन सबकी दुम आपस में बांध भी दी है। ये सभी परस्परावलंबी स्वयंभू हैं। अदालत यह कह ही कैसे सकती कि जब तक शांति नहीं होगी तब तक वह संविधान की कसौटी पर किसी सरकारी कदम को जांचने का काम स्थगित करती है। उसे तो विधायिका या कार्यपालिका की विफलता से धधकते दावानल में पैठ कर अपनी संवैधानिक भूमिका देश के सामने रखनी ही चाहिए, ताकि हिंसा की जड़ काटी जा सके।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी हिंसा की आग को संविधान के छींटे से बुझाना न्यायपालिका की पहली जिम्मेवारी है। जब-जब वह ऐसा करने से चूकती है, तब-तब वह हिंसा की जनक बनती है। हमारे संविधान ने इसलिए ही न्यायपालिका को सिर्फ कान नहीं दिए हैं बल्कि आंखें भी दी हैं; और स्वत:संज्ञान ले कर वह किसी को भी कठघरे में खड़ा कर सकती है। क्या न्यायपालिका इस जिम्मेवारी से खुद को अलग करती है? संविधान उसे इसकी इजाजत नहीं देता है।
वह प्रधानमंत्री और उसकी कृपा पर बने वे सभी मंत्री-गण हिंसा के जनक हैं जो सच छुपाने में और येन-केन-प्रकारेण अपनी सत्ता की रखवाली में लगे हैं। सत्ता की निरंकुश हिंसा जिस प्रधानमंत्री को न दिखाई देती हो और जिसका मंत्रिमंडल हुआं-हुआं करने वाले सियारों से ज्यादा की औकात नहीं रखता हो, हिंसा की यह आग उसकी ही लगाई हुई है। देश में छिड़ा नागरिकता आंदोलन सरकारी दोमुंहेपन से पैदा हुआ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़, वाराणसी के विश्वविद्यालयों में जैसी क्रूर और नंगी हिंसा हुई है, उसके बाद भी क्या किसी को कहने की जरूरत है कि हिंसा के जनक कौन हैं और कहां हैं? यह राजधर्म में हुई वैसी ही अक्षम्य चूक है जैसी चूक 2002 में, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे को भड़काने और उसे निरंकुश चलते रहने देने में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब ही आज के प्रधानमंत्री को, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सार्वजनिक रूप से फटकारते हुए राजधर्म का सवाल खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आज उसके पास कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। आज उसके पास वह मुख्यमंत्री है जिसने अपने विपक्षी अवतार में सार्वजनिक संपत्ति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है, महात्मा गांधी के बारे में हद दर्जे की फूहड़, घटिया बातें कही हैं। आज वह मुख्यमंत्री सार्वजनिक घोषणा करता है कि वह नागरिकों से ‘बदला लेगा’, कि सीसीटीवी कैमरे में कैद प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें देख-देख कर, उनसे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेगा। यह स्वयंभू राजा का वह फरमान है जिसके सामने लोकतंत्र लज्जा से मुंह छिपा ले। ऐसा आलम बनाया गया है कि लाचार होकर पूछना पड़ता है कि क्या राज्यतंत्र गुंडातंत्र में बदला गया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कपड़ों से पहचान रहे हैं कि आंदोलनकारी कौन हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कैमरे से पहचान कर रहे हैं कि आंदोलनकारी कौन हैं; और आंदोलनकारी नागरिक कह रहे हैं कि हम हिंसक असंवैधानिक हरकत करने वालों का चेहरा पहचान रहे हैं। यकीनन, कपड़े बदल जा सकते हैं, कैमरे खाली किए जा सकते हैं लेकिन चेहरे का आप क्या करेंगे?
इस हिंसा के जनक वे आला पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिस मैनुअल के सारे निर्देशों और पेशेवराना नैतिकता को सिरे से भूल कर, सत्ताधारियों की कृपादृष्टि के कायर याचक भर रह गए हैं। आज से ज्यादा रीढ़विहीन पुलिस अधिकारियों की जमात देश ने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। जब पुलिस-अधिकारी ऐसे हों तब हम सामान्य कांस्टेबल से किस विवेक की अपेक्षा कर सकते हैं? वह डंडे चलाता है तो वह समझता भी नहीं है कि जिसकी पीठ-सर-हाथ-पांव पर वह बेरहमी से वार किए जा रहा है, गालियां उगल रहा है, वह लोकतंत्र का मालिक नागरिक है, कल जिसके दरवाजे इनके सारे आका कोर्निस बजाते मिलेंगे। यह विवेकहीनता हिंसा की जनक है।
वे सारे कलमधारी निरक्षर पत्रकार, चैनलों के विदूषक अौर बौद्धिकता का चोला ओढ़कर राजनैतिक दलों की दलाली करने वाले संभ्रांत लोग हिंसा के जनक हैं, जो स्थिति को संभालने और शांत करने की जगह उसे भड़काने का आयोजन करने में लगे होते हैं। उनकी मुद्रा, उनकी भाषा, उनके शीर्षक और उनके निष्कर्ष सब किसी जहर-कुंड से निकले दिखाई और सुनाई देते हैं।
हिंसा न हो यह सामूहिक जिम्मेवारी है-उनकी सबसे ज्यादा जो सत्ता की उन जगहों पर बैठे हैं जहां से सामूहिक हिंसा का आदेश भी दिया जाता है और आयोजन भी किया जाता है। हम सब अपनी सूरत आईने में देखें और हिंसा के पाप में अपनी भागीदारी का सार्वजनिक प्रायश्चित करें। यह गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पाप की गठरी ढीली करने का इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता है।
लेकिन यह बात भी जोर से कही और बताई जानी चाहिए और सड़कों पर उतरे लोगों को यह अहसास होना ही चाहिए कि हिंसा हमेशा आत्मघाती होती है, गांधी की इस बात को भूलना आत्महत्या करना होगा। निजी हो या सार्वजनिक, किसी भी संपत्ति का विनाश दरअसल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब लड़ाई व्यवस्था से हो तब व्यक्ति गौण हो जाता है। सरकार को यह समझाना है या समझने के लिए मजबूर करना है कि वह नागरिकता के निर्धारण का अपना कदम वापस ले ले। यह उसका काम है ही नहीं। अगर देश में घुसपैठियों का संकट है तो यह सरकार की, और सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपनी व्यवस्था को चुस्त बनाए। घुसपैठिए बिलों से देश में दाखिल नहीं होते हैं। वे व्यवस्था की कमजोरी में सेंध लगाते हैं। वे जानते हैं कि सेंध वहीं लग सकती है जहां दीवार कमजोर होती है। इसलिए आप सरकार बनें, षड्यंत्रकारी नहीं; आप अपनी कमजोरी दूर करें, नागरिकों को कमजोर न करें।
आज से कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब वर्दीधारी पुलिस राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारी बन कर उतरी थी। सरकार के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ उसने नारे लगाए थे। सड़कें जाम कर दी थीं। तब वे वर्दीधारी वकीलों का मुकाबला करने में जनता का समर्थन चाहते थे। तब किसी ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे क्या? लाठियां मारीं क्या? पानी की तलवारें चलाईं? नागरिकों ने एक स्वर से कहा था कि ये अपनी बात कहने सड़कों पर तब उतरे हैं जब दूसरे किसी मंच पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस को भी ऐसा ही समझना चाहिए। पुलिस को नागरिकों से जैसा समर्थन मिला था, क्या नागरिकों को पुलिस से वैसा ही समर्थन नहीं मिलना चाहिए? आज पुलिस नागरिकों से ऐसे पेश आ रही है मानो दुश्मनों से पेश आ रही है।
पुलिस भी समझे, सरकारी अधिकारी भी समझें, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी समझें, हमारे और उनके मां-बाप भी समझें कि यह लड़ाई नागरिकता को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हिंसा नहीं, हिम्मत; गालियां नहीं, वैचारिक नारे; पत्थरबाजी नहीं, फौलादी धरना! गोडसे नहीं, गांधी; भागो नहीं, बदलो; डरो नहीं, लड़ो; हारो नहीं, जीतो; और इसलिए भीड़ का भय नहीं, शांति की शक्ति और संकल्प का बल ही नागरिकों की सबसे बड़ी ताकत है। वह यह ताकत और संयम न खोए तभी यह सरकार समझेगी। सरकार समझे और अपने कदम वापस ले, तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा मजबूत बन कर उभरेगा। यह आज का राजधर्म है, जिस पर गौर करना चाहिए।
(वरिष्ठ टिप्पणीकार, लेखक, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष)