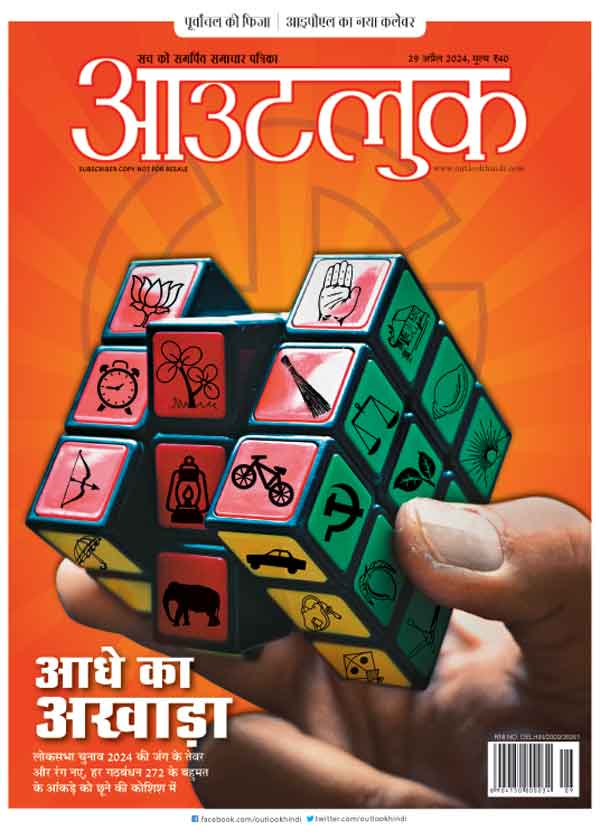राइजिंग कश्मीर के संपादक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शुजात बुखारी की हत्या राज्य में पीडीपी-भाजपा गठबंधन के टूटने और राष्ट्रपति शासन के एक नए दौर में प्रवेश का सबब बन गई। वैसे तो कठुआ में आठ साल की बकरवाल बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद से ही जम्मू में जिस तरह के आंदोलन चले उसने गठबंधन की दरारों को साफ दिखाना शुरू कर दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन अपने दो मंत्रियों के इस्तीफ़े के बावजूद समर्थन वापस न लेने और राज्य में रमज़ान के मौके पर इकतरफ़ा सीजफ़ायर की घोषणा से कश्मीर में एक नई शुरुआत की उम्मीदें साफ़ दिखने लगीं थीं।
अपनी हालिया कश्मीर यात्रा के दौरान खासतौर पर पत्थर फेंकने वाले नौजवानों को लेकर गृहमंत्री का बयान मरहम लगाने की नीति के अनुरूप था। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी ही बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सीजफ़ायर को भी थोड़े और दिन आजमाया जाएगा। लेकिन यह एक दुधारी तलवार थी जिससे दोनों तरफ की कट्टरपंथी ताक़तें नाराज़ थीं। देश भर में हिंदूवादी दक्षिणपंथ ने तो सीजफ़ायर का विरोध किया ही था, कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ही नहीं बल्कि हुर्रियत के गीलानी और मीरवायज़ धड़े तथा यासीन मालिक के जेकेएलएफ को मिलाकर गठित ज्वाइंट रेसिस्टेंस लीडरशिप तक ने इस सीजफ़ायर का विरोध किया था। शुजात की हत्या को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट और उसके समर्थन से जोड़कर देखने वाले लोग सीजफ़ायर की घोषणा, ट्रैक टू शांति प्रक्रिया और उसमें शुजात की भूमिका से जोड़कर नहीं देख पा रहे।
घाटी के प्रतिष्ठित पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शुजात बुखारी घाटी में हालिया शांति प्रयासों में बेहद सक्रिय थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान तक अपनी पहचान और प्रभाव के कारण वह ट्रैक टू की शान्ति प्रक्रियाओं के लिए एक उपयोगी व्यक्ति हो सकते थे और हुए भी। पत्रकार प्रवीण स्वामी बताते हैं कि बुखारी हाल में ही एक ब्रिटिश एनजीओ कोंसिलिएशन रिसोर्सेज द्वारा दुबई में आयोजित उस बातचीत का हिस्सा थे, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के इस्लामी नेता अब्दुल राशिद तूराबी, वहाँ की हुर्रियत के नेता सैयद फ़ैज़ नक़्शबंदी और अलगाववादी पत्रकार इरशाद महमूद, नेशनल कान्फ्रेंस के असलम वानी, कांग्रेस के जीएन मोगा, भाजपा के विक्रम रंधावा, पत्रकार ज़हीरुद्दीन और इफतिखार गिलानी तथा अलगाववाद समर्थक मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज़ शामिल हुए थे। इसी बातचीत में सीज़फायर की अनौपचारिक सहमति बनने की बात की जा रही है। ठीक इन्हीं वजहों से वह कश्मीर के अलगाववादियों के लिए आंख की किरकिरी बन गए।
हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन ने इसे ‘आन्दोलन की पीठ में छुरा घोंपने वाला’ तक बताते हुए इसके भागीदारों को ‘भाड़े का टट्टू’ घोषित किया तो एक अलगाववादी ब्लॉग कश्मीरफाइट में प्रकाशित लेख में शुजात पर लिखे लेख का शीर्षक था– ‘द टाउट्स हू आर बेट्रेयिंग द कश्मीर स्ट्रगल।’ यह आश्चर्यजनक है कि जिसे कल तक दलाल और भाड़े का टट्टू कहा जा रहा था वह क़त्ल के बाद शहीद बन गया और उसकी हत्या में उसी भारतीय राज्य की भूमिका देखी जाने लगी जिसका उसे दलाल कहा जा रहा था। यह शुजात की लोकप्रियता ही थी कि सभी मुख्यधारा की पार्टियों के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जेआरएल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
नब्बे के दशक से ही कश्मीर में बातचीत और सद्भाव के समर्थकों की हत्या कोई नई बात नहीं है। यहाँ सबसे पहले दो अलग-अलग धाराओं से आने वाले हृदयनाथ वांचू और फज़ल-उल-हक़ को याद किया जा सकता है। हृदयनाथ वांचू नब्बे के दशक के एक प्रसिद्ध ट्रेड युनियन एक्टिविस्ट थे जो कश्मीर घाटी से पंडितों के पलायन के ख़िलाफ़ थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। श्रीनगर के जवाहर नगर में उनके घर के सामने पार्क में उनकी समाधि है और वहाँ के टैक्सी स्टैंड का नाम उनके ही नाम पर है। उनकी हत्या को लेकर भी कश्मीर एक्सपर्ट्स में मतभेद है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिता हक्सर इसके लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार मानती हैं तो ह्यूमन राइट वाच इस षड्यंत्र का आरोप तत्कालीन राज्यपाल पर लगाती हैं। फज़ल-उल-हक़ ने वर्ष 2000 में हिज़बुल मुजाहिदीन और भारत सरकार के बीच सीज़फायर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हालांकि यह सीज़फायर बस दो हफ्ते चल पाया था। इसके बाद भी वह लगातार बातचीत से राह निकाले जाने के पक्षधर रहे। 2009 में उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया जिसमें उनकी जान तो बच गई लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए अपंग हो गया जिसके बाद से ही वह पुलिस सुरक्षा में अपने घर में ही रहते हैं। इसी साल फ़रवरी के महीने में उनके सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला करके उसकी रायफल छीन ली गई।
थोड़ा पीछे जाएँ तो 2002 में कश्मीर के बड़े नेता और भारत से बातचीत के पक्षधर अब्दुल गनी लोन की ऐसे ही अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आरोप स्टेट से लेकर पाकिस्तान तक पर लगे। इसके पहले 1990 में मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक़ की हत्या भी ऐसे ही हुई थी। दो जनवरी, 2011 को विभाजित हुर्रियत के नरम धड़े के प्रमुख प्रवक्ता अब्दुल गनी बट्ट ने कश्मीर बुद्धिजीवियों की भूमिका पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा– ‘मीरवाइज़, लोन और जेकेएलएफ के विचारक प्रोफेसर अब्दुल गनी वानी की हत्या भारतीय सेना ने नहीं भीतर के लोगों ने की थी। हमने अपने बुद्धिजीवियों को मार डाला। जहां भी हमें कोई बुद्धिजीवी मिला, हमने उसे मार डाला।’ अब्दुल गनी लोन की हत्या के बाद तत्कालीन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल ने कहा था- "हालांकि उनकी हत्या का ज़िम्मा किसी ने नहीं लिया, लेकिन इतना तो तय है कि उनके हत्यारे उनमें से ही हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो।"
सीज़फायर के दौरान शुजात और एक भारतीय सैनिक औरंगज़ेब की हत्या के बाद लगभग स्पष्ट था कि सीज़फायर को और बढ़ाया नहीं जाएगा और ऐसा चाहने वालों की कश्मीर और उसके बाहर कोई कमी नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार रिपोर्ट, शुजात की हत्या और घाटी में लगातार बिगड़ते हालात कश्मीर में आजमाए गए सभी तरीक़ों की असफलता का स्पष्ट संकेत थे और मेहबूबा सरकार से कश्मीर के भीतर या बाहर शायद ही किसी को कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। पिछले चुनावों में लगभग सभी की मान्यता थी कि अलगाववादी दलों का परोक्ष समर्थन उन्हें मिला था लेकिन सरकार में रहते हुए इन संगठनोंं की उम्मीदों को पूरा करना उनके लिए तब और भी मुश्किल था जब वह भाजपा के साथ गठबंधन में थी। खासतौर पर मुफ़्ती साहब की मृत्यु के बाद गठबंधन की खींचतान अक्सर दिखाई देती थी।
इसका एक बड़ा कारण था दोनों पार्टियों का अलग-अलग आधार, जहां पीडीपी की आकांक्षाएँ राज्य स्तरीय थीं और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि वह अलगाववादियों के प्रति नर्म रवैया अपनाते हुए बातचीत और सुलह की शुरुआत करेंगी, वहीं भाजपा की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का ही नहीं बल्कि जम्मू में जो जनाधार है, वह उससे कश्मीर में कड़ी नीति अपनाने, आर्टिकल 370 और धारा 35 ए हटाने जैसी उम्मीदें पालता है। ज़ाहिर है दोनों का साथ लंबे समय तक चल पाना नामुमकिन था। इस पूरी प्रक्रिया में मेहबूबा मुफ़्ती कश्मीर में बुरी तरह आलोकप्रिय हो चुकी हैं। हालत यह है कि वह अपने पारंपरिक चुनाव क्षेत्र अनंतनाग और बिजबेहरा जाने से भी बचती रही हैं और 2014 में उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई अनंतनाग की सीट पर अब तक उपचुनाव करा पाना संभव नहीं हुआ, यही नहीं श्रीनगर में भी वह उपचुनावों में अपने सगे भाई को जीत नहीं दिला सकी थीं। यही वजह थी कि भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस या नेशनल कान्फ्रेंस ने उन्हें साथ लेकर नई सरकार का गठन करने की जगह राष्ट्रपति शासन लगाने और जल्दी चुनाव कराने की मांग करना उचित समझा।
आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ होंगे, लेकिन जो हालात हैं उनमें यह सवाल बड़ा है कि अलगाववादियों के विरोध के सामने वहां शान्ति से चुनाव करा पाना संभव होगा भी नहीं। हमने श्रीनगर के लोकसभा उपचुनावों के दौरान व्यापक हिंसा और बहुत कम मतदान वाली स्थिति देखी है, अगर अगले कुछ महीनों में हालात नहीं सुधरते तो एक बार फिर कश्मीर में वैसी ही स्थिति देखी जा सकती है।
फ़िलहाल यह कह पाना एक क़यासबाजी ही होगी कि आगे कश्मीर में क्या होगा। राज्यपाल एनएन वोहरा का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। वह कश्मीर में लंबे समय से हैं और मुख्यधारा के राजनैतिकों सहित कश्मीर के बाक़ी स्टेकहोल्डर्स के बीच उनका सम्मान है। यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इसका उपयोग बातचीत और शांति प्रयासों के लिए किस हद तक कर पाती है। इसके विपरीत अगर सेना और अर्द्ध सैनिक बलों की सख्ती बढ़ाई गई तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि कश्मीर में शान्ति न तो केवल सख्ती से हो सकती है न ही केवल बातचीत से। शुजात की हत्या के बाद कोई भी कश्मीरी पत्रकार या राजनैतिक कार्यकर्ता मध्यस्थ की भूमिका निभाने से पहले सोचेगा ही तो सत्ता से आज़ाद होकर मेहबूबा एक बार फिर पुराना राग अलाप सकती हैं। जम्मू और घाटी में जिस क़दर दूरी बढ़ी है उसमें जम्मू में फेंकी गई चिंगारी कभी भी घाटी को जला सकती है तो घाटी की घटनाओं की जम्मू में प्रतिक्रिया अवश्यंभावी है।
ज़ाहिर है जो हालात हैं वे बेहद उलझे हैं। घाटी ज्वालामुखी के दहाने पर बैठी है और ज्वालामुखी पहले से ही धधक रही है। फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने दिसंबर 2017 में कहा था कि “हर कोई घुटन महसूस कर रहा है क्योंकि राजनैतिक व्यवस्था लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने मे असफल रही है। युवा देश की ओर बड़ी सावधानी से देख रहे हैं और चूंकि वे पढ़े-लिखे हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आतंकवादी बनना आता है। देश मे बीफ़ की बहस और गौरक्षा आन्दोलन देश को बांट रहे हैं और युवा दक्षिणपंथी उभार की प्रतिक्रिया में आतंक की राह अपना रहा है।” गुजिश्ता साल भर मेंं सुधरने की जगह हालात और बिगड़ते चले गए हैं। बुरहान वानी की हत्या के बाद से ही शुरू हुए दौर के बरक्स कश्मीर संकट हल होने की जगह एक नए दौर में जाता दिख रहा है। मारा हुआ बुरहान ज़िंदा बुरहान से हज़ार गुना अधिक प्रभावी हो गया।
80 के दशक में मक़बूल बट्ट की फांसी के बाद अब्दुल गनी लोन ने कहा था– ‘कश्मीर के विलय के सवाल पर मक़बूल पहला शहीद है। केंद्र सरकार और राज्य की फ़ारूक़ सरकार ने उसे शहीद बना दिया।” लगभग यही बात बुरहान के लिए कही जा सकती है। उसके जनाज़े में उमड़ी भीड़ और उसके बाद लगभग पूरे कश्मीर में छः महीने लम्बी चली हड़ताल हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी घटना थी जिसका असर दूरगामी था। इसके बाद ख़ासतौर पर दक्षिणी कश्मीर और श्रीनगर में पत्थरबाज़ी आम हो गई और आतंकवाद की पांतों में नई भर्तियां शुरू हो गईं। कश्मीर पुलिस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी प्रवृत्ति पहले से अलग थी– इनमें पढ़े लिखे और संपन्न घरों के लड़के ज़्यादा हैं।
अभी हाल में हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर को हिज़बुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ते और पुलवामा मुठभेड़ में मारे जाते देखा है। इसके अलावा लगभग पहली बार आतंकवादी आन्दोलन शहरी इलाक़ों से बाहर ग्रामीण इलाक़ों में पहुंचा, हर पुलिस इनकाउंटर के दौरान पत्थरबाज़ी की घटनाओं और पैलेट गनों के प्रयोग के बावजूद हर आतंकवादी के जनाज़े में उमड़ी भीड़ जनता में बढ़ती कुण्ठा और उसके क्षोभ की ही प्रतीक नहीं थी बल्कि उससे भी ख़तरनाक इंगित था– जनता के बीच मौत का खौफ़ ख़त्म हो रहा है! नब्बे के दशक के आंदोलन की आज़ादी के मांग के बरअक्स इस दौर में इस्लामी कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक जिहाद के प्रभाव ने हालात को बेक़ाबू कर दिया है। आज बहुत स्पष्ट तौर पर कश्मीर के आंदोलन का कोई ऐसा नेता नहीं जो इसे नियंत्रित कर सके। हुर्रियत हो या जेकेएलएफ, सब इसके आगे चलने की जगह पीछे-पीछे भागते ही नज़र आते हैं और इस पागलपन में जो संयमित बात करने की कोशिश करता है उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है जिसकी एक ही सज़ा है - मौत!
इसलिए आने वाले कुछ महीने कश्मीर और भारत के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण होंगे। अगर इस दौर में शांति तथा धैर्यपूर्वक कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की गई तो इस ज्वालामुखी पर नियंत्रण असंभव होता चला जाएगा।
(कश्मीरनामा : इतिहास और समकाल के बाद अशोक इन दिनों घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों पर एक किताब लिख रहे हैं)