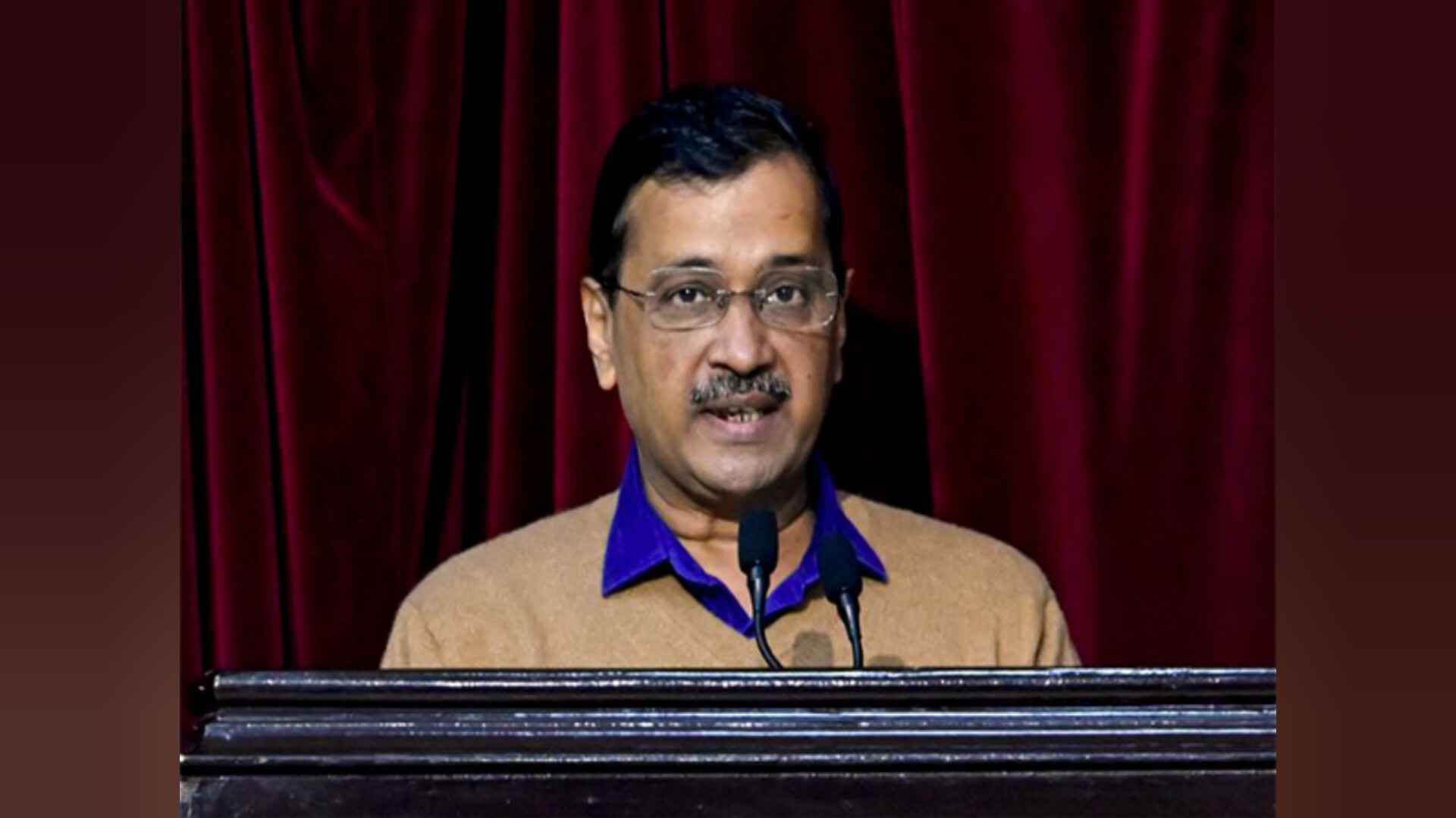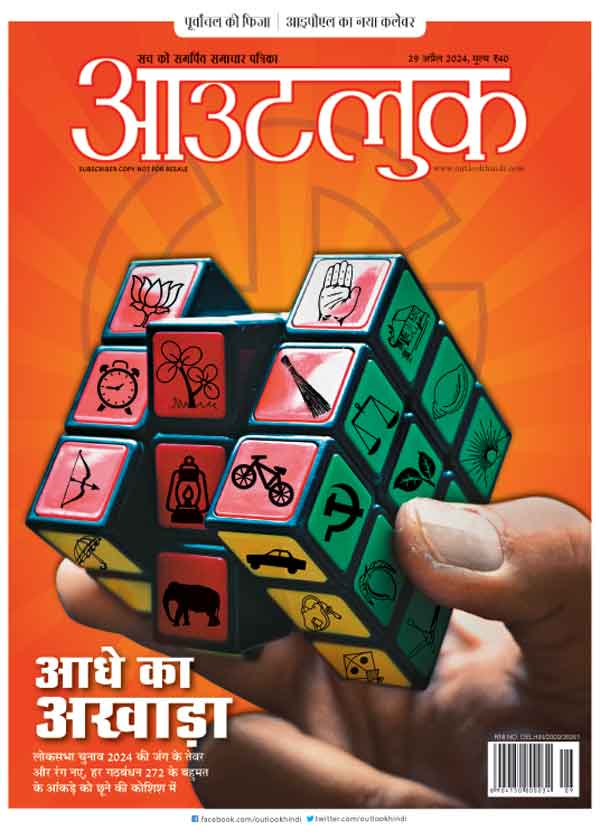दिलीप कुमार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में चर्चा का विषय बनने से बहुत पहले बिना इसके बारे में जाने अभिनय के ढंग का आविष्कार किया, अगर वो नहीं होते तो कितने ही लोगों को अदाकारी के असली मायने समझ में नहीं आता। एक ऐसे अदाकार की अदाकारी जो कल की पीढ़ी के लिए हमेशा श्रेष्ठ बनी रहेगी। उन्होंने अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित भी किया। अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार से लेकर नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान तक, लगभग हर कोई उनकी तरह अभिनय करने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन कोई भी उनके अभिनय के करीब नहीं पहुंच सका, जिसमें उनको महारत हासिल थी।
यूसुफ खान के रूप में जन्मे दिलीप उन दुर्लभ अभिनेताओं में से थे, जो अपने हर किरदार को एक साधारण आदमी की तरह जीते थे, फिर चाहे उन्होंने पर्दे पर ट्रैजेडी किंग और गांव के देहाती व्यक्ति की ही भूमिका क्यों न निभाई हो। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के ऑरिजीनल 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' थे, जिन्होंने अपनी पूरी लगन को शामिल किए बिना किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं लिया। यह ऐसा गुण था जिसने अक्सर उन पर बहुत अधिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उन्हें अपने निर्देशकों के साथ टकराव में भी डाला, लेकिन उन्होंने अपनी अभूतपूर्व लोकप्रियता के कारण सेट पर मध्यस्थ अभिनेता के रूप में ऐसा नहीं किया, बल्कि वास्तव में वो हमेशा सहयोग करना चाहते थे। जिससे प्रोजेक्ट हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरें।
उनके आश्चर्यजनक अभिनय की सूची इसकी पर्याप्त गवाही देती है। जुगनू (1947), अंदाज़ (1949), आन (1952), देवदास (1955), नया दौर (1957), मुगल-ए-आज़म (1960), गंगा जमना (1961), राम और श्याम (1967) से लेकर क्रांति तक (1981), विधाता (1982), शक्ति (1982) और सौदागर (1991) ने अपनी दूसरी पारी में बहुमुखी प्रतिभा को अपने तरीके से परिभाषित किया। लोग उन्हें न केवल एक एक्टिंग यूनिवर्सिटी बल्कि एक एक्टिंग स्कूल भी कहते थे और ये व्यर्थ नहीं था। अपने करियर के चरम पर, वो दुखद पात्रों में इतना डूब जाते थे कि वो ब्लैक एंड ह्वाइट दौर में खो जाते थे और अपने वास्तविक जीवन में उदास महसूस करने लगते थे।
दुखद भूमिकाओं का उनके जीवन पर असर डालने के बाद अपने मनोचिकित्सक के सुझाव पर, कुमार ने हल्की-फुल्की कॉमेडी वाली भूमिकाएं करने का फैसला किया। इस तरह की स्थिति के कारण उन्हें गुरु दत्त की प्यासा (1957) जैसे ड्रीम रोल ठुकराना पड़ा। ‘प्यासा’ उन तीन फिल्मों में से एक है जिन्हें उन्होंने करने से मना कर दिया था। प्यासा के अलावा भारत भूषण की बैजू बावरा (1952) और अमिताभ बच्चन की जंजीर (1973), ये दो अन्य फिल्में हैं।
दिलीप कुमार, वास्तव में उस समय के कुछ अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की पेशकश की गई थी। कुमार ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया (1962) फिल्म के लिए ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें डेविड लीन जैसे अंतरराष्ट्रीय कद के एक निर्देशक को ठुकराने का कोई अफसोस नहीं था, जो उन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया (1962) में साइन करना चाहते थे। इसके बाद यह फिल्म उमर शरीफ के पास गई और उन्हें रातोंरात अंतरराष्ट्रीय स्टार बना दिया। उस दौरान दिलीप ने अपनी सफलता को भुनाने के लिए फिल्मों को साइन करने की होड़ में जाने में विश्वास नहीं किया। 55 साल से अधिक के अपने करियर में, उन्होंने मुश्किल से 60-65 फिल्में कीं। फिल्म ज्वार भाटा (1944) के गीत में अपनी शुरुआत से लेकर किला (1998) तक, उनका करियर इस तथ्य की वास्तविकता को याद दिलाता है कि एक अभिनेता को अपने आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किए जाने के लिए सिर्फ कई सारे किरदारों को निभाने की जरूरत नहीं है। अभिनेता का काम मायने रखता है ना कि उनके द्वारा की गई फिल्मों की संख्या। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में कुमार का 75 प्रतिशत से अधिक अभिनय बिना किसी से विवाद में आज ऑल टाइम क्लासिक्स में गिने जाते हैं।
दिलीप ने 1970 के दशक में एक लंबा ब्रेक लिया था और मुश्किल से सगीना (1974) और बैराग जैसी कुछ फिल्में कीं। (1976) में वो मनोज कुमार की क्रांति के साथ लौटे और इसके बाद रमेश सिप्पी की ‘शक्ति’ के साथ आए, जहां उनके समय के मेगास्टार अमिताभ बच्चन को सपोर्टिंग रोल करना था। विधाता, मशाल (1984), और सौदागर (1991) जैसी फिल्मों के साथ अपनी दूसरी पारी में भी, उन्होंने फिल्म निर्माताओं और दर्शकों- दोनों को अपनी हथेलियों पर मनोरंजन कराया। ‘मशाल’ में वहीदा रहमान के साथ उनका दृश्य जहां वो रात में अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए एक कैब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये दृश्य सभी एक्टिंग स्कूलों में छात्रों को दिखाया जाता है।
अपने शानदार करियर में उनको एकमात्र अफसोस ये रहा कि वो एक भी फिल्म का निर्देशन नहीं कर सके। अप्रत्याशित सफलता के दिनों में वो फिल्म “गंगा जमुना” और “दिल दिया दर्द लिया”(1966) में तो पूरी तरह घोस्ट डायरेक्टर ही थे। इसमें एक सुपर हिट थी तो दूसरी सुपर फ्लॉप। उनका एकमात्र 'आधिकारिक' निर्देशन, कलिंगा जिसमें सफलता निश्चित नहीं थी, 1990 के दशक में ये फिल्म दिन के सूरज को नहीं देख सका या ये कहें कि उनका ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया।
98 साल की उम्र में उनके निधन से विश्व सिनेमा ने अंतिम महान अभिनेता को खो दिया है। उन्होंने अशोक कुमार, राज कपूर, देव आनंद और राजकुमार से लेकर असाधारण समकालीन लोगों के साथ काम किया। लेकिन उनके जैसा कोई नहीं था। खास बात तो यह है उनके जैसा कोई नहीं होगा। आने वाले सभी समयों के लिए उनकी तुलना केवल स्वयं उन्हीं से की जा सकती है।