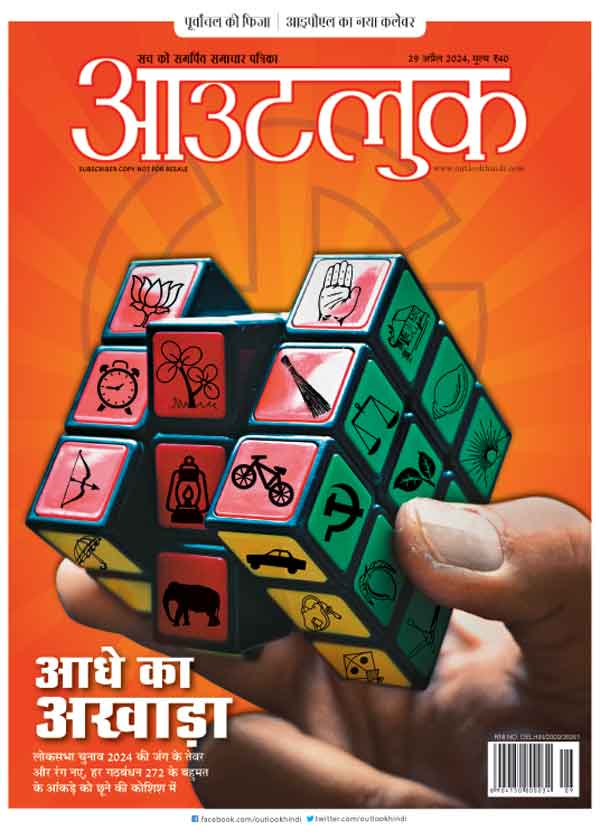भारतीय परंपरा की रक्षा करने के नाम पर उसके बुनियादी तत्वों बहुलता, परिवर्तनशीलता, संवाद और खुलेपन को हाशिये पर डाला जा रहा है: वे वक्तव्य देने के लिए ठीक हैं। पर उन्हें आचार-व्यवहार में पोसना-बरतना जरूरी नहीं रह गया हैः एक तरह की घटिया और मदेस प्रतीकात्मकता को, कर्मकांड को अध्यात्म के सत्व के रूप में प्रस्तुत किया और उसे बरतने के लिए तरह-तरह के दबाव बन रहे हैं। दंगा-फसाद, हिंसा, हत्या, भय आदि लगातार बढ़ रहे हैं। विचार, आचार, दृष्टि, धर्म, जाति आदि की अल्पसंख्यकता नाकाबिले बरदास्त हो रही है, और ऐसे सारे अल्पसंख्यकों को संदिग्ध मानने का माहौल बन गया है। ऐसा लग रहा है कि हमारी परंपरा की बहुत भोंथरी समझ और व्याख्या पर, खासकर युवा वर्ग पर डालने का एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। देश में बहस इस पर नहीं हो रही है कि गरीबी-शोषण-अत्याचार कैसे घटे, सामाजिक समरसता कैसे बढ़े पर इस पर हो रही है कि आप क्या खायें क्या न खायें, क्या देखें-सुनें क्या न देखें-सुनें, क्या पढ़ें-लिखें क्या न पढ़ें-लिखें। प्रतिष्ठित संस्थाओं का लगातार अवमूल्यन हो रहा है ताकि ज्ञान, असहमति, बौद्धिक और सर्जनात्मक साहस की सभी जगहें हाशिए पर चली जाएं। यह अजब समय है जब प्रश्नांकन द्रोह की संज्ञा पा रहा है।
यह सब न तो हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता के अनुरूप है, न इसे भारतीय परंपरा से निकला माना जा सकता है। यह दरअसल लोकतंत्र और परंपरा दोनों के साथ विश्वासघात के बराबर है। विडम्बना यह है कि यह अपमान और आघात वे शक्तियां कर रही हैं जो लोकतंत्र के सहारे आगे बढ़ी हैं और जिनका दावा परंपरा को आगे बढ़ाने का है। भारतीय साहित्य यों तो भक्ति काल से, पर उसके पहले से भी, आज तक अपने स्वभाव में उत्सवधर्मी और प्रश्नावाचक दोनों एक साथ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से उसकी प्रवृत्ति अधिकतर व्यवस्था-विरोधी रही है। यह आकस्मिक नहंी है कि उसे अंतःकरण की चौकीदारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। उसकी आवाज अंतःकरण और साहस की, कल्पना और सृजनशीलता की, प्रश्नांकन और विरोधी की, अंधेरों में उजाले की उम्मीद की, एकसेपन की विकराल व्याप्ति के बरक्स बहुलता पर आग्रह करने की रही है। उसने संवाद और बहस पर, चकाचौंध से छिपाये जा रहे अंधेरों की शिनाख्त करने पर इसरार किया है। इसलिए यह स्पष्ट पहचाना जा सकता है कि भारत का असली और टिकाऊ लोकतंत्र उसका साहित्य और कलाएं, उसका बुद्धि-व्यापार है। इस लोकतंत्र का तकाजा है और हमारे अंतःकरण की मांग कि इस मुकाम पर इस बसके विरुद्ध आवाज उठायेंः अगर हम ऐसा नहीं करते तो वर्तमान राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्था हमें भले ही नजरअंदाज करती रहे, इतिहास माफ नहीं करेगा। मैंने साहित्य अकादेमी को जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है:
अध्यक्ष महोदय,
यह कहना है कि यह साहित्य, कलाओं, परंपरा और संस्कृति सबके लिए बहुत कठिन समय है। जिस बहुलता, समावेश और खुलेपन को, बहुभाषिकता और बहुधार्मिकता को हम पोसते और उससे शक्ति पाते रहे हैं, उस पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। हम इकहरेपन की तानाशाही के कगार पर पहुंच रहे हैं और संकीर्णता, हिंसा, हत्या, असिहष्णुता, प्रतिबंध आदि सब लगातार बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक होना लगभग अपराधी होना बन गया है। ऐसे समय में हम सृजनसंप्रदाय के लोग चुप और उदासीन नहीं बैठे रह सकते।
इस मुकाम पर साहित्य अकादेमी की चुप्पी बहुत आपत्तिजनक है। आप लेखकों के राष्ट्रीय संस्थान हैं। उनमें से कुछ की हत्या तक दिनदहाड़े हो गयी और अकादेमी ने न तो इस पर कुछ कहा, न सरकार पर दबाव डाला कि वह इन हमलों को रोके और हत्यारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शीघ्र करे और करवाये।
इस दुखद परिप्रेक्ष्य में एक लेखक के रूप में मैं यही कर सकता हूं कि साहित्य अकादेमी पुरस्कार (जो मुझे 1994 में मिला था) विरोधस्वरूप वापस कर दूं। मुझे याद नहीं कि कितनी राशि मिली थी: पर 1 लाख रुपये का चैक संलग्न है।
आपका
अशोक वाजपेयी
श्री विश्वनाथ तिवारी
अध्यक्ष
साहित्य अकादेमी
नयी दिल्ली