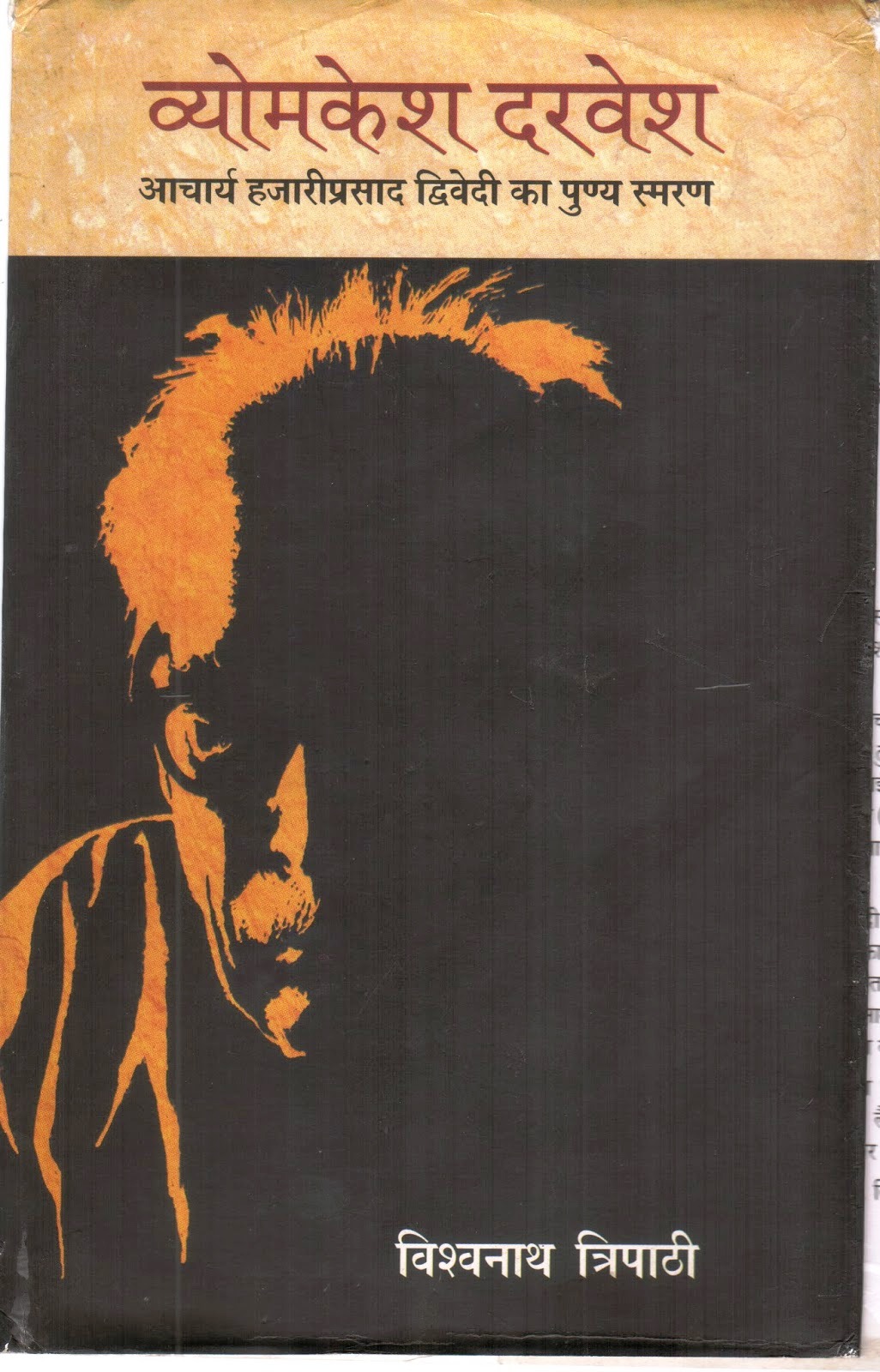पिछली आधी सदी से अधिक समय से हिंदी कविता और आलोचना में अनिवार्य उपस्थिति बन चुके गजानन माधव मुक्तिबोध (13 नवंबर, 1917-11 सितंबर, 1964) का जन्मशताब्दी वर्ष चल रहा है। अभी तक उनकी एक भी प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी सामने नहीं आई है। यह तथ्य इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि हिंदी में जीवनी लेखन की परंपरा अभी तक पूरी तरह जड़ नहीं जमा पाई है। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय 'बच्चन’ की चार-खंडों वाली आत्मकथा और यशपाल के संस्मरणात्मक लेखन के अलावा आत्मकथा लेखन तो लगभग सिरे से गायब है। कुछ संस्मरणात्मक लेखन जरूर नजर आता है लेकिन हिंदी भाषी समुदाय के विशाल आकार को देखते हुए वह ऊंट के मुंह में जीरे समान है।
साहित्य अकादेमी की 'भारतीय साहित्य के निर्माता’ शृंखला के अंतर्गत प्रकाशित लघु पुस्तिकाओं के अलावा और कहीं हिंदी के बड़े लेखकों की जीवनियां नजर नहीं आतीं। कुछ वर्ष पहले हिंदी के कवि-आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने अवश्य अपने गुरु आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी पर एक जीवनीनुमा विस्तृत आख्यान व्योमकेश दरवेश लिखा था। इसे भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्तिदेवी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था लेकिन उसके अलावा हाल के वर्षों में कोई दूसरी उल्लेखनीय जीवनी देखने को नहीं मिली। आज भी भारतेन्दु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल जैसे शीर्षस्थ साहित्यकारों की प्रामाणिक और विस्तृत जीवनियां उपलब्ध नहीं हैं। हां, प्रेमचंद के पुत्र और जाने-माने लेखक अमृत राय ने जरूर अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही लिखी थी जो जीवनी लेखन के क्षेत्र में प्रतिमान मानी जाती है। अमृत राय की पत्नी सुधा चौहान ने भी अपनी मां सुभद्रा कुमारी चौहान पर एक पुस्तक मिला तेज से तेज लिखी लेकिन उसे पूर्णत: जीवनी विधा के अंतर्गत रखना कठिन होगा। रामविलास शर्मा की तीन खंडों वाली पुस्तक निराला की साहित्य साधना ने न केवल निराला के जीवन बल्कि उनके साहित्य को समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस दृष्टि से वह एक अद्वितीय अध्ययन है। विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला के अमर कथाकार शरत चन्द्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखी जिसे उसके प्रकाशित होने के कुछ वर्षों के भीतर ही क्लासिक का दर्जा मिल गया। इस सबके बावजूद कड़वी हकीकत यही है कि हिंदी में जीवनी और आत्मकथा लेखन अभी अपने शैशवकाल में ही है। दलित साहित्यकारों की कुछ अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण आत्मकथाएं अवश्य प्रकाशित हुई हैं लेकिन उनमें लेखकों के बारे में कम, उनके जातिगत और सामाजिक अनुभवों के बारे में अधिक पता चलता है। इन आत्मकथाओं का साहित्यिक से अधिक समाजशास्त्रीय महत्व है। इनमें तुलसी राम की मुर्दहिया और मणिकर्णिका तथा ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
क्या इस अभाव के पीछे यह कारण है कि हिंदी भाषी समाज अपनी साहित्यिक-सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के प्रति पर्याप्त सचेत नहीं है और अपनी ऐतिहासिक स्मृति संजोकर रखने की विशेष आवश्यकता नहीं समझता? क्या एक कारण यह भी नहीं है कि हिंदी समाज में साहित्यकारों को वैसी प्रतिष्ठा और सम्मान हासिल नहीं है जैसा बांग्ला, मलयालम, तमिल या मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को उनके समाज में मिलता है? एक जमाना था जब हिंदी क्षेत्र के लगभग हर शिक्षित परिवार में प्रेमचंद और वृंदावनलाल वर्मा जैसे लेखकों की पुस्तकें पढ़ी जाती थीं। आज क्या कोई ऐसा हिंदी लेखक है जिसे साहित्यिक उत्कृष्टता और लोकप्रियता की दृष्टि से यह स्थान मिला हुआ हो? क्या इसका एक कारण यह भी नहीं कि हिंदी भाषी समाज में पुस्तकें खरीदने की प्रवृति लगातार कम होती गई है। आजादी के बाद के वर्षों में साक्षरता और शिक्षा का तो विस्तार हुआ है लेकिन पुस्तकें खरीदकर पढ़ने की आदत कम हुई है। वरना क्या कारण है कि हिंदी के अच्छे-से-अच्छे लेखक की किताब का एक संस्करण अधिक-से-अधिक ग्यारह सौ प्रतियों का छापा जाता है? और अक्सर उतनी प्रतियों का भी नहीं।
स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन नहीं था। उसके साथ-साथ सभी क्षेत्रों और समुदायों के बीच कुरीतियों, अशिक्षा और अंधविश्वास से मुक्ति पाने के आंदोलन भी चलाए गए थे। बकौल गालिब, 'और कुछ चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए’ यानी अभिव्यक्ति के लिए और अधिक विस्तार की हर क्षेत्र में ललक थी। छोटे-छोटे कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय भी इसी आंदोलन के तहत खोले गए थे। इसका अर्थ यह है कि आज की तरह उस समय के प्रकाशक केवल सरकारी खरीद या ग्राहक की खरीद पर ही निर्भर नहीं थे क्योंकि छोटे-बड़े सार्वजनिक पुस्तकालयों का जाल फैल गया था। आज ये पुस्तकालय या तो बंद हो गए हैं या अंतिम सांसें ले रहे हैं। यह भी इस बात का एक और प्रमाण है कि हिंदीभाषी समाज में पढ़ने-लिखने की प्रवृति का क्षरण होता जा रहा है।
जीवनी लिखना कविता-कहानी लिखने जैसा नहीं है। एक श्रेष्ठ जीवनी लिखने के लिए अनेक स्थान पर जाने, अनेक व्यक्ति से मिलने और गहन शोध करने की जरूरत होती है। इसके लिए समय और धन, दोनों चाहिए। हिंदी के कितने लेखक इतने समर्थ हैं जो एक जीवनी लिखने के लिए कई वर्ष और लाखों रुपये खर्च कर सकें? इस काम के लिए कितने प्रकाशक अग्रिम राशि देने के लिए तैयार होंगे? क्या सरकारी या निजी संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय हैं? संभवत: कुछ हों भी लेकिन अभी तक उस सक्रियता का विशेष असर देखने में नहीं आया है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस दिशा में सार्थक पहल की जाएगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और कला-संस्कृति पर लिखते हैं।)