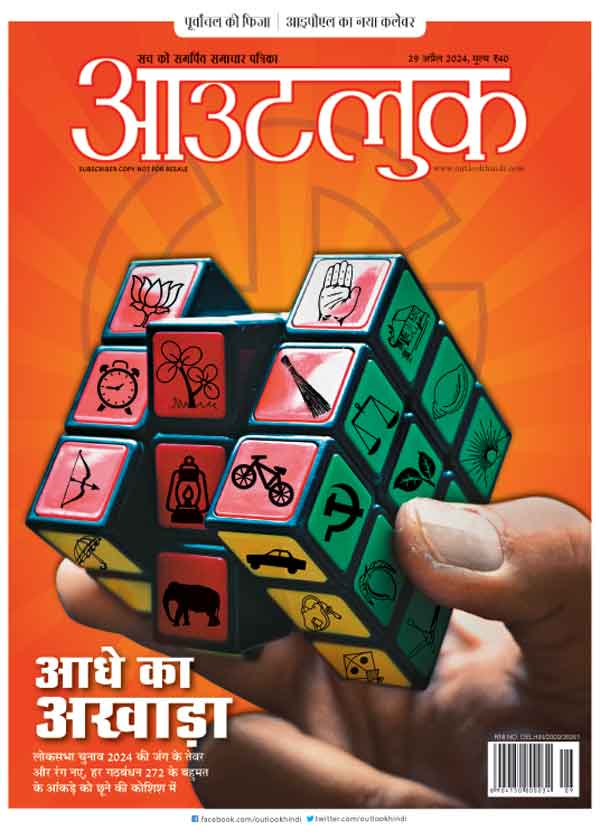एक कवि और कर भी क्या सकता है / सही बने रहने की कोशिश के सिवा - अपनी इन पंक्तियों के इर्द-गिर्द ही हम समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण और मुखर हस्ताक्षर वीरेन डंगवाल को पातेे हैं। विचारधारा का अदृश्य झोला कंधे पर लटकाए यह यारबाश कवि कैंसर के ठहाकों के साथ ही भिड़ता दीखता है। मारक कैंसर के दोबारा हमले से लड़ रहे कवि वीरेन डंगवाल के साथ बैठकी भीतर तक भिगो गई। उनके साथ संवाद के लिए साथ आए वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल ने उनकी गंभीर बीमारी को धकियाते हुए कवि-कविता-सृजन-समाज-बदलाव-संघर्ष जैसे विषयों का जो वितान खींचा, उससे बातें इंद्रधनुष के रंगों में नहाकर सामने आईं। ये दोनों कवि समकालीन हैं, दो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं, दोनों पहाड़ के हैं और दोनों लड़ते-भिड़ते दोस्त भी हैं। इन दिनों दिल्ली में वीरेन डंगवाल का कैंसर के लिए इलाज चल रहा है, महीने में तीन बार कीमोथेरेपी हो रही है; अभी उनका घाव रिसता है, जिसे वह टिशू से पोंछते हुए निर्द्वंद्व भाव से संवाद जारी रखते हैं। वह जहरीला घाव कवि को बोलने, जिंदादिली से हंसने और गले लगाकर मिलने से रोक नहीं पाता। आउटलुक की सहायक संपादक भाषा सिंह ने दो वरिष्ठ रचनाकारों-दोस्तों के बीच दरी बिछाने का काम किया और उनके विचारों को समेट कर कलमबंद किया। साथ में रहे आउटलुक के संपादक नीलाभ मिश्र। पेश हैं इस यादगार बातचीत के अंशः

मंगलेश डबरालः एक दौर हमारा था और एक यह, क्या बुनियादी फर्क नजर आता है ?
वीरेन डंगवालः कॅरिअरिज्म जैसी चीज जो आज बड़ी बन गई है, लोगों को फिराए फिर रही है, उसका हमारे समय में नामोनिशान न था।
मंगलेश डबरालः तुम्हारी किताब में इसी दुनिया में बहुत अच्छी तरह से दर्ज है कि वह दौर कितनी बेफिक्री का था, कितनी मनुष्यता का, कितनी उम्मीदों का।
वीरेन डंगवालः यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह हमारी जिंदगी या यंू कहें कि हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया था। वह एक वैल्यू सिस्टम भी था न, उसे हम अभी तक ढोए चले जा रहे हैं। यह झोला जिंदगी में शामिल है। एक अदृश्य झोला जो टंगा हुआ है, हमारे साथ चल रहा है।
भाषाः सत्तर के दशक ने बहुत रचनाकारों को गढ़ा। तब से क्या अंतर लगता है आज आपको ?
वीरेन डंगवालः जरूर सत्तर का दशक बहुत अहम दौर रहा। अस्सी के दशक तक भी इतनी मायूसी, उतनी नाउम्मीदी नहंी थी। इतनी चमक भी नहीं थी। बड़ा विरोधाभास है कि जितनी चकाचौंध बढ़ती गई है, उतनी जीवन में निराशा बढ़ी है। ऐसे में आप से आपकी चीजें छीनती चली जाती हैं। इससे दिल दुखता है।
भाषाः और वह अदृश्य झोला...
वीरेन डंगवालः वह तो है ही मेरे, या यंू कहें, हमारे जीवन का हिस्सा।
मंगलेश डबरालः हम लोग जिस दौर में शहरों में आए, उसमें एक बड़ी लहर थी जिसने हमें पटका यहां। हमारे भीतर एक बेचैनी थी, जो उबल रही थी। हमारे चेहरों को देखकर लगता था कि परिवर्तन आएगा। हमारी अपनी पहचान भी कोई अलग से नहीं थी। समूह था, विचारधारा थी। मैं उस दौर को ऐसे ही देखता हंू। उस दौर की स्मृति या अतीत से किसी कल्पना का जन्म हो सकता है ? मुझे कई बार लगता है कि स्मृति और कल्पना में गहरा संबंध है। हम इसे कैसे देखें, अतीत या कल्पना।
वीरेन डंगवालः स्मृति और स्वप्न तो पुरानी बात है, जो रचना को जमीन मुहैया कराती है। यह सतत प्रक्रिया तो हमारे भीतर चलती रहती है। उसमें थोड़ी फंफूद जरूर लग गई है। वह थोड़ी जड़वत जरूरत हो गई है, लेकिन फिर भी वही हमें जिलाए हुए है।
मंगलेश डबरालः तो हम इसे कैसे बिना अतीत राग बनाए देखें... इस बारे में बताओ।
वीरेन डंगवालः उस समय हम अपने यथार्थ के निरंतर साथ चल रहे थे। हम और हमारी भाषा भी। आज यथार्थ थोड़ा आगे चला गया और हम पीछे छूट गए हैं। हमारे साथ अगर वे चीजें स्वप्न या स्मृति के तौर पर मौजूद हैं तो भी वे प्रेरणा नहीं दे रही हैं। हम अदनेपन से घिर गए हैं। साधारण क्षुद्रताओं ने हमें पकड़ लिया है। इसकी वजह से जो उस स्वप्न या अतीत का योगदान हमारे जीवन में हो सकता था, जो हमें उस यथार्थ के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बनाता, जीवन और रचनाओं को स्पंदित करता, हमारे भीतर चिंगारी पैदा करता-मुझे लगता है उसका हमारे भीतर अभाव है।
मंगलेश डबरालः लेकिन हम और हमारी पीढ़ी की कविता ने जो स्वप्न देखा, जिसे हम सामूहिक स्वप्न कह सकते हैं, क्या उस सपने के सच होने की उम्मीद बची रहती है ?
वीरेन डंगवालः उस उम्मीद के अलावा कोई चारा भी नहीं है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं उसके अलावा। मैं तो भरसक कोशिश करता हंू लात खाकर भी उसे बचाए रखने की।
मुश्किल है। यह समय इतना अस्पष्ट है कि डर लगता है। मान लिया कि इस समय इतने उत्कट संघर्ष भी चल रहे हैं, जो उस स्वप्न को आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे पूरी तरह से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लोगों की पीड़ा बढ़ी है, संघर्ष भी बढ़े हैं लेकिन विचारधारात्मक विभ्रम सा बना हुआ है। जो लोग इसका निदान निकालने की कोशिश की बात करते हैं वे भी उस दिशा में जाते दिखाई नहीं देते।
मंगलेश डबरालः हमारे दौर की कविताओं में खासकर तुम्हारे संग्रह इसी दुनिया में इस स्वप्न की अनगूंजें स्पष्ट सुनाई देती हैं, छोटी-बड़ी कविताओं में, जैसे समोसा, गाय आदि। क्या यह स्वप्न आज की कविताओं मंे दिखाई देता है।
वीरेन डंगवालः यह स्वप्न हमारे लिए तो मुख्य संचालक बना हुआ है। उसके बिना तो कुछ सोचा नहीं जा सकता। अपनी कविताओं पर बात करना मुझे पसंद नहीं है लेकिन समाज की बात करें तो मेरे दूसरे कविता संग्रह के समय परिस्थितियां बदल रही थीं, वैश्विक परिस्थितियां बदल रही थीं। गैट आ रहा था, लाटरी का पूरा तंत्र आ रहा था, खासकर गरीबों के जीवन को अपने गिरफ्त में लेता हुआ और ठीक उसी समय इस पूरे बदलाव से ध्यान रचने के लिए, इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए, धोखा रचने के लिए बाबरी मस्जिद का ध्वंस रचा जा रहा था। बहुत बड़े अवरोधक उपकरण के तौर पर सांप्रदायिकता को स्थापित किया जा रहा था।
मंगलेश डबरालः बाबरी मस्जिद तो हमारे पूरे भारतीय समाज की बहुत बड़ी दुर्घटना है....
वीरेन डंगवालः नहीं यह केवल दुर्घटना नहीं, एक इतना भयानक संयत्र था जिसने पूरे भारतीय समाज को चरमरा दिया। वह आज भी खड़े होने की स्थिति में नहीं है।
मंगलेश डबरालः बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद गुजरात की हिंसा पर तो हिंदी में खूब कविताएं लिखी गईं। शायद किसी और भाषा में इतनी कविताएं नहीं आई हों...
वीरेन डंगवालः नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, हो सकता है लिखी गई हों। लेकिन हां, हिंदी में खूब अच्छी लिखी गईं, जैसे तुम्हारी गुजरात के मृतक का बयान।
मंगलेश डबरालः खैर, हम जिस भयानक यथार्थ में रह रहे हैं, उसकी सच्चाई जानते हैं। लेकिन कवियों से उम्मीद की जाती थी कि वे उसका प्रतिसंसार रचेंगे। इस भयानक यथार्थ को लांघकर एक दूसरे संसार, जो संभव संसार है, की ओर इशारा करेंगे। क्या हम कवि लोग उस संसार की ओर इशारा नहीं कर पा रहे हैं ? यह संसार बहुत तेजी से बदल रहा है, क्या हम इस संसार के शिकार हैं ?
वीरेन डंगवालः काफी हद तक। हम उसके शिकार हैं, उससे उल्लसित भी हैं। हम इनका मुकाबला करने, इन्हें जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए कविता का इतना असर नहीं है। अरे कविता का कम से कम कुछ तो असर समाज पर दिखाई देना चाहिए न साहब। आखिर इतनी महान भाषा, इतना महान इसका इतिहास, इतनी महान रचनाओं की थाती, सैकड़ों-हजारों सालों की परंपरा से भरी हुई और उस कविता का मौजूदा समाज, समय पर कुछ असर न हो। इसकी वजह सामाजिक विकास में जरूर खोजी जा सकती है लेकिन इसका मतलब है कि कविता ने कहीं कुछ छोड़ दिया और इस वजह से लोगों ने कविता को। इसके कारण कविता में मौजूदी हैं।
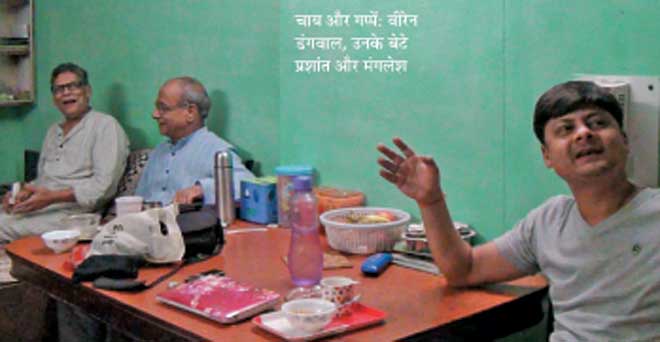
मंगलेश डबरालः इसकी क्या वजह हो सकती है ? क्या हमने विचारधारा छोड़ दी है और यथार्थ के आगे घुटने टेक दिए हैं। मसलन, मैंने ये बातें पढ़ीं कि मोबाइल ने दुनिया बदल दी....।
वीरेन डंगवालः फेसबुक ने बदल दी, लैपटॉप ने बदल दी...।
मंगलेश डबरालः क्या वाकई बदली है या यह आभास पैदा किया कि बदल दी है ?
वीरेन डंगवालः बदली है, इसमें नकारने वाली बात नहीं है। लेकिन अंततः बात यह है कि उसने आमूल परिवर्तन नहीं किया।
मंगलेश डबरालः तो क्या हमने विचारधारा छोड़ दी है ? यहां विचारधारा से मेरा आशय सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा से नहीं हैं।
वीरेन डंगवालः हां, ये तो जरूर हुआ है। मनुष्य का क्षरण तो जरूर हुआ है।
मंगलेश डबरालः पिछले दिनों मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि नवारुणा भट्टाचार्य ने कहा, बैक टू आईडीयोलॉजी, विचारधारा की तरफ वापसी। दिक्कत यह है कि विचारधारा की मार्क्सवाद से जोड़कर देखा जाता है, विश्व की बात नहीं सोची जाती। यह विचारधारा मार्क्सवाद हो सकती है, समाजवाद हो सकती है, बौद्ध दर्शन हो सकती है।
वीरेन डंगवालः (ठहाके लगाते हुए) हां, यह बड़ा विचित्र हिसाब हो गया है। कल एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं घनघोर कम्युनिस्टों से बहुत परेशान हंू। तो मैंने कहा कि कहां मिलते हैं ये घनघोर कम्युनिस्ट। उसने जवाब दिया, फेसबुक मंे दिखाई देते हैं।
नीलाभ मिश्रः वह जिन लोगों को फेसबुक पर देख रहा है, वे तो कम्युनिस्ट भी नहीं हैं।
मंगलेश डबरालः कहना चाहिए था कि वह तो सिर्फ फेशियल है।
वीरेन डंगवालः अरे, मैं तो घनचक्कर खा गया।
मंगलेश डबरालः दरअसल हो यह रहा है कि विचारधारा के अभाव में लिखा खूब जा रहा है। बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हर महीने कहा जाता है कि इसमें क्रांति हो गई है।
वीरेन डंगवालः बिल्कुल, प्रभूत मात्रा में। ऐसा लगता है कि जैसे प्रोडक्शन हाउस चल रहा है। कोई जीवन दर्शन नहीं नहीं नजर आता। मनुष्यता का कोई स्वप्न नहीं दिखाई देता।
भाषाः इस स्थिति का रिश्ता का कितना इस बात से जोड़ते हैं कि जब आपकी पीढ़ी लिख रही थी 70 के दशक में, तब बड़ा आंदोलन और उसके मूल्य आपको गढ़ रहे थे ? ऐसा आंदोलन आज के दौर में नहीं दिखाई देता।
वीरेन डंगवालः बिल्कुल सही। इस आंदोलन के वाहक बनने का हम सकून ले रहे थे और यह आपको रचने के लिए एक आत्मिक ताप दे रहा था। तो आंदोलनों के अभाव से दिक्कत तो होती ही है। लेकिन इसके अलावा कवि केा अपने उपकरण भी तो बनाने और तलाशने पड़ते हैं। यह थोड़े ही कहा जा सकता है कि हमारे समय में आंदोलन था इसलिए हमने बड़ी कविता लिखी और आज वह आंदोलन नहीं है तो नहीं लिखी जा रही। इस समस्या का समाधान तो हमें ही करना चाहिए कि आखिर कविता का असर क्यों नहीं हैं। ये तो कवि सम्मेलन में भड़ैती करते हैं उनका इतना असर है और आप जो बुनियादी बात करना चाहते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, आपका कोई असर नहीं हैं। सिर्फ कवि ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और कोई तो न निकालेगा यार। सवाल यह है कि क्या यह किसी के जेहन में है भी।
भाषाः युवा रचनाकारों की एक बड़ी दुनिया फेसबुक हो गई है।
मंगलेश डबरालः लेकिन वह अपना संकट साथ लेकर चल रहे हैं।
वीरेन डंगवालः लगता ऐसा है कि वे संकट को एन्जॉय कर रहे हैं। फेसबुक कविता उनकी त्वरित प्रतिक्रिया है जो जल्द ही बिला जाती है।
मंगलेश डबरालः ऐसा लगता है, इस समय की जितनी शक्तियों सरंचनाएं हैं वे सब कविता की विरोधी हैं, रचना विरोधी हैं।
वीरेन डंगवालः यह सही है कि शक्ति संरचनाएं रचना की विरोधी हैं, वे एक सपाट जगत चाहती हैं। लेकिन कविता को तो ऐसी परिस्थितियांे से भिड़ना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है। यह कविता का काम है। यह संकट हमारा तो है ही लेकिन हमारे बाद का ज्यादा है। दिक्कत यह है कि जैसे ही हम कहेंगे तो यह पीढी को कहेगी कि आप बूढ़े कवि हैं और आप नई पीढ़ी को गाली दे रहे हैं।
मंगलेश डबरालः यह कहा भी जाना चाहिए। हम भी अपने दौर में यही कहते थे।
वीरेन डंगवालः यह बात कल भी कुछ हद तक सही थी, आज और ज्यादा सही है। आज लोलुप बूढ़ों का युग है। इतने लोलुप बुड्ढे शायद भारतीय इतिहास में कभी एक साथ नहीं पैदा हुए, जितने अभी हैं।
मंगलेश डबरालः इसके कई उदाहरण हाल ही में भी देखने को मिले हैं। फिलहाल कविता का समाज से जो फासला बढ़ा है उसके लिए कहा जा रहा है कि कविता को बदलना होगा, उसे छंद की ओर जाना होगा।
वीरेन डंगवालः यह तो सिर्फ स्ट्रक्चरल मांग है। ऐसा हर समय हुआ है। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, बनिस्वबत हम उसका ईमानदारी से निर्वाह कर पाएं। शमशेर ने दो रास्ते आपके सामने रखे हैं। और तो और, मुक्तिबोध ने रखे हैं। नागार्जुन ने पूरा संसार रखा है। हम लोगों ने कहीं प्रयोगशीलता को अंगीकार नहीं किया। हम यह समझ रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन असल में हम दूर जा रहे थे। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता मिसाल है।
मंगलेश डबरालः अंधेरे में कविता को 50 साल हो गए हैं। सत्तर के दशक में गैर-कांग्रेसवाद के दौर में नक्सलवाद के उभार के साथ अंधेरे में एक बार फिर प्रासंगिक हो गई थी।
वीरेन डंगवालः इस कविता की जो सिंसियरिटी है, जो ताप है, जो सच्चाई है, उसे अंगीकार किए बिना आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि यह छंद आदि का सवाल नहीं है। यह कविता के सामने की चुनौती है। सवाल यह है कि हम किसके लिए कविता लिख रहे हैं।
नीलाभः तकनीक की बात पहले भी चली थी। तकनीकी बदलाव हर दौर में चले हैं और वे नए नैतिक सवाल खड़े करते हैं। 19वीं सदी में औद्यौगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड में डिकेंस जैसे रचनाकार इससे रूबरू हुए। लेकिन अब का रचनाकार क्या नई तकनीक से एंगेज कर रहा है।
मंगलेश डबरालः मेरा आप से सवाल है कि क्या यह जो नई तकनीक आई है उसने एक नई संस्कृति, नई भाषा को जन्म दिया है।
नीलाभः वही मैं कह रहा हंू कि इस नई तकनीक से भिड़ने-जुझने के बाद नए रचनाकार को पता चलेगा कि उसका भाषा या रचना पर क्या असर होगा। अभी तो वह उसमें बह रहा है। पत्रकारिता कभी-कभार इस सवाल से जूझती दिखती हैं। नई किस्म के शोषण हैं जिन्हें आज का हिंदी साहित्यकार नहंी समझ रहा है।
वीरेन डंगवालः यही समस्या है। इस चुनौती से भिड़ना कवि-रचनाकार को ही है।
मंगलेश डबरालः दिक्कत है कि आज हिंदी पट्टी में जो संकट है, जो निजीकरण की मार है, आदिवासियों पर मार है, उन पर कोई बड़ी कविता-कहानी नहीं दिखाई देती। हिंदी आदिवासियों पर ऐसी कहानी नजर नहीं आती। आदिवासियों से बड़ी संभावना है, स्त्रियों से, दलितों से बहुत संभावनाएं हैं।
वीरेन डंगवालः दलित और स्त्री समाज से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत आस है। हालांकि अभी हिंदी में उतनी बड़ी रचना आई नहीं हैं। आदिवासी समाज में भी बहुत बेचैनी है। अभी छोटी-मोटी चिंगारियां है।
भाषाः लेकिन हिंदी का जो मठाधीश हैं, वह इन तीनों (दलित-आदिवासी-स्त्री) की दावेदारी को नहीं स्वीकार कर रहा।
वीरेन डंगवालः वह करेगा भी नहीं। सामंतवाद का पूरे समाज पर बहुत असर है, हिंदी साहित्य में भी है।
मंगलेश डबरालः ये जो हिंदी के मठाधीश हैं, जमींदार हैं, जो सब पर कब्जा करना चाहते हैं। खासकर ये आलोचक, इनका बहुत दबदबा है। यह बड़ी त्रासदी है हिंदी में आलोचना का बहुत दबदबा है।
वीरेन डंगवालः दबदबा किस बात का, आलोचना दिशा कहां दे रही है ? आलोचना का मामला बहुत चौपट है।